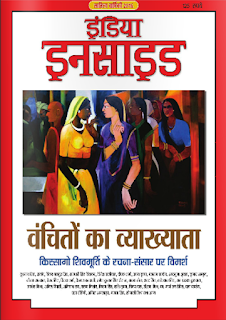--शिवमूर्ति
गांव की औरतों ने दांतों तले उंगली दबाई।
अचरज तो इस बात का है कि गांव की उन बूढ़ियों, सयानियों को भी कानों-कान भनक नहीं लगी जो अपने को तीसमार खां समझती हैं। जो मानती हैं कि गांव की किसी बहू-बेटी की सात पर्दे में छिपा कर की गयी ‘हरक्कत’ भी उनकी नजरों से बच नहीं सकती। वे अब भी अन्दाजा नहीं लगा पा रहीं हैं कि इस साॅड़नी ने किस छैल-छबीले को भेंड़ा बनाया और भेंड़ा बनाया तो छिपाया कहां? झटके में हुई ‘राह चलन्तू’ कमाई तो यह हो नहीं सकती। चार छः दिन का इत्मीनानी संग साथ चाहिए।
सबसे पहले चतुरा अइया की नजर पड़ी। नयी पीढ़ी की उन कुछ बहू-बेटियों को छोड़कर जिनके घर में पक्के संडास बन गये हैं, गांव की औरतें अब भी दिशा मैदान के लिए सुबह-शाम बाबा के पोखरे वाले जंगल में जातीं हैं। जिन घरों में संडास बन चुके हैं उन घरों की बूढ़ियां और चिरानी-पुरानी हो चुकी बहुएं भी जंगल जाना ज्यादा पसंद करती हैं। उनकी यह आदत मरने के साथ ही जायेगी। पानी-बूंदी के मौसम में मजबूरन घर में जाना पड़ा तो नाक, मुंह पर कपड़ा लपेटकर अंदर घुसती हैं।
जंगल जाना सिर्फ जंगल जाना नहीं होता। जो सुख झुंड में ‘बतकूचन’ से मिलता है वह घर में कैद रह जाने से कैसे मिलेगा? एक की बात खतम नहीं होती कि दूसरी की शुरू हो जाती है। घर वापसी हो जाती है और बात खत्म नहीं होती है। तब चलते-चलते पूरा झुंड रूक जाता है।
उस दिन वापस लौटते-लौटते उजास फैल गयी थी। पुरवा के झोंके से पल-भर के लिए कुच्ची का आंचल उड़ा कि चतुरा अइया की नजर उसके पेट पर पड़ी। इतना चिकनाया पेट। पांच महीने का उभार। उनकी आंखों के कोए फैल गये। अभी तक सबकी आंखों में धूल झोंकती रही यह बछेड़ी। लेकिन एकदम मुंहामुंही कहें कैसे? पद में वे कुच्ची की अजिया सास यानी सास की भी सास लगतीं हैं।... लेकिन इतनी बड़ी बात पेट में दबा कर रखें भी तो कब तक? अफारा हो जायेगा।
वे सारे दिन बेचैन रहीं। बाई उभर आयी। सांस उखड़ने लगी। किसी तरह राम-राम करके दिन काटा। शाम को मिलते ही उसे घेरा- ‘बाय गोला का रोग कहां से ले आयी रे बहुरिया?
अंदर तक हिल गयी कुच्ची। हाथ पैर के रोयें परपरा कर खडे़ हो गये। चतुरा अइया जैसी छछन्दी दूसरी कौन है गांव में? बहुत कुछ सुन रखा है उसने। पांच-छः बच्चों की महतारी होने तक जिधर से निकलती थीं, पानी में आग लगाती चलती थीं। जिसके मर्द से हंसकर बोल लेतीं उसकी ‘जनाना’ को जूड़ी चढ़ जाती थी। कांपती आवाज को काबू में करती हुई वह मिमियायी -बाय गोला का रोग सात दुश्मन को लगे अइया।
-फिर यह कोंछ में क्या छिपा रखा है? अइया ने उसकी नाभि में उंगली धंसाते हुए पूछा- मुझे तो पांच-छः महीने का लगता है।
-तुहूं गजब बाटू अइया। जब देने वाला ही चला गया तो ‘बाय गोला’ क्या मैं ‘परूआ’ पा जाऊंगी?
बगल चलने वाली पड़ोसन ने टहोका मारा- ‘गोला’ देने वालों की कौन कमी है इस गांव में। जरा सी नजर फंसी नहीं कि ले ‘गोला’।
तब तक कुच्ची संभल चुकी थी। छिपाने से कितने दिन छिपेगा? जवाब तो देना ही पडे़गा, लेकिन इतनी जल्दी देना पडे़गा, यह नहीं सोचा था।
-जिसको आना है वह तो अब आकर रहेगा अइया। छिपाने से लौट थोड़े जायेगा।
-न आने के भी हजार रस्ते हैं बहू। तेरे आदमी को मरे दो साल से ज्यादा हो गये होंगे। आने वाला आ गया तो किसका नाम धरेगी?
-किसी का नाम धरना जरूरी है क्या अम्मा? अकेले मेरा नाम काफी नहीं है?
चतुरा अइया कुच्ची के आगे आ खड़ी हुईं। उसकी दोनों बाहों को पकड़ कर झिंझोड़ते हुए फुसफुसाईं -कैसे बोल रही है रे? किसी ने भूत प्रेत तो नही कर दिया? तेरे जेठ बनवरिया को खबर लगी तो पीस कर पी जायेगा।
-जेठ से क्या मतलब अइया? मैं उनकी कमाई खाती हूं क्या? उनका चूल्हा अलग, मेरा अलग।
ऐसे करम और ऐसा जवाब। सब सन्न रह गयीं।
0
ससुर तो पहले ही कम बोलते थे। इकलौते जवान बेटे की मौत ने उन्हें एकदम गूंगा कर दिया। श्राद्ध का सारा कर्मकांड उन्होंने सिर झुकाए-झुकाए निपटाया। घुटा सिर, बिना दाढ़ी-मूंछ वाला चेहरा। अंदर को धंसी आंखे। उनको लगता रहा होगा कि बेटा कमाने-धमाने लगा। अब उन्हें गृहस्थी के झंझटों से मुक्ति मिल जायेगी। हाईस्कूल में दो बार फेल होने के बाद हनुमान चचेरे भाई बनवारी के साथ बोरिंग के काम में लग गया था। इलाके में धरती का पानी तेजी से नीचे खिसक रहा था, जिससे पट्टा पुल्ली वाले पुराने ट्यूबवेल पानी छोड़ने लगे थे। हर साल एक-दो ट्यूबवेल पानी छोड़ते थे। अब बिना डेढ़ दो सौ फीट गहरी बोरिंग किए, बिना सबमर्सिबल मोटर डाले पानी नहीं मिलने वाला था। दोनों भाइयों ने सही समय पर इस काम में हाथ सधाया। हजार पांच सौ रुपये रोज की कमाई करने लगे। मोटर और पाइप की खरीद पर डीलर से, मिलनेवाला कमीशन अलग। इस साल खुद अपने चक में बोरिंग कराने का इरादा किए था हनुमान कि वज्रपात हो गया।
तेरही के दूसरे दिन जब सारे मेहमान चले गये तो कुच्ची के बाप ने उसे एक किनारे बुलाकर मद्धिम आवाज में समझाया -तुम्हारा दाना-पानी अब इस घर से रूठ गया बिटिया। अब यहां की मोह-माया छोड़ो। कुछ खा-पी लो और चलने की तैयारी करो। यहां की चीजें, गहना गीठी, सास को सौंप कर चलना है।
पैर के नाखून से नम फर्श की मिट्टी कुरेदते सिर झुकाए उसने सुना, फिर अंदर जाकर अपनी कोठरी में घुस गई। खडे़ नहीं रहा गया। एक कोने में जमीन पर बैठ गई।
यहां की चीजें। क्या हैं यहां की चीजें? अभी तक यहां और वहां की चीजों को अलगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज पड़ गयी। उसे परम्परा से पता था कि अब यह घर उसका नहीं रह जायेगा। जिस खूंटे से बांधने के लिए उसे लाया गया था, जब वही नहीं रह गया तो...। उसकी आंखे झरने लगीं। ससुराल से मिले गहने-पायल बिछुआ, झुमका और अंगूठी तो उसने उतार लिया लेकिन नाक की कील उतारते हुए उसके हाथ कांपने लगे। कील के अंदर के पेंच ने घूमने से इंकार कर दिया। कल तक ये चीजें उसकी थीं। आज पराई हो गईं।
दो चप्पले थीं। एक गौने में मिली थी, एक अभी दो महीने पहले ‘वे’ लाये थे। क्या दोनों छोड़नी पड़ेगी? नगे पांव जाना पडे़गा?
सास कोठरी में घुसीं तो वह कील की पेंच खोलने में ही परेशान थी। उसने सास से मदद ली। सूनी नाक को उंगलियों से छूते हुए उसे अजीब लगा।
सास ने उसे अंकवार में भरते हुए कहा- चाहती तो हूं कि तुम्हें कभी न जाने दूं लेकिन किस अख्तियार से रोकूं? जाओ, तुम्हे इससे अच्छा घर वर मिले। हमसे अच्छे परानी मिलें। कोस दो कोस पर रहना तो कभी-कभार हमारी खबर भी लेती रहना।
गले लग कर दोनों कुछ देर तक सिसकती रहीं।
अचानक उसे याद आया कि अभी जानवरों को पानी नहीं पिलाया। बिना पिलाये चली गयी तो कहो दिनभर प्यासे ही रह जायें। वह बाल्टी लेकर बाहर आयी और हैंडपम्प से भर कर उन्हें पानी पिलाने लगी। कुए से पानी भरने की मेहनत से बचाने के लिए हनुमान ने पिछले साल यह हैंडपम्प लगवा दिया था।
नीले वेलवेट की एक छोटी सी थैली में वह अपने गहने रखती थी। इसमें सोने के टाप्स और जंजीर थी। इनको ‘उन्होंने’ दो महीने पहले खरीद कर दिया था। अभी सास को इनकी जानकारी नहीं थी।
हर महीने दूसरे महीने मोटर साइकिल पर बैठाकर वे उसे पिक्चर दिखाने शहर ले जाते थे। पिक्चर दिखाने और गोलगप्पे खिलाने। उसे गोलगप्पे का खट्टा पानी बहुत पसंद था।
वह कराहते हुए कहती- पेट में बहुत दरद हो रहा है अम्मा।
सास घबरा जातीं। ‘उनसे’ कहती- ले जा, किसी डाक्टर को दिखा दे।
लौटने पर पूछतीं- क्या बताया डाक्टर ने? कुछ उम्मीद है?
वह मुस्करा कर इंकार में सिर हिला हेती। कभी-कभी ब्लाउज से निकाल कर कैल्सियम या क्रोसीन की गोलियों की स्ट्रिप दिखा देती। पेट दर्द महीने दो महीने के लिए बंद हो जाता।
टाप्स और जंजीर भी लौटा दे कि साथ लेती चले? वह कुछ देर तक दुविधा में रही फिर तय किया- क्या फायदा? जब देने वाला ही चला गया।... वह जब भी इन्हें पहनेगी, ‘वे’ आकर सामने खड़े हो जायेंगे।
सास के हाथ में पकड़ाने से पहले उसने थैली का मुंह खोल कर गिना दिया- आपके दिए पांचो थान, साथ में ए टाप और जंजीर। इन्हें वे दो महीना पहले लाये थे। सहेज लीजिए।
सास ने बिना देखे थैली का मुंह बन्द करके कमर में खोंस लिया।
कुच्ची ने बक्से का ताला खोलकर लाल रूमाल में लिपटा एक छोटा पैकेट निकाला और सास के हाथों में पकड़ाते हुए बताया- इसमें सात हजार रूपये हैं। उन्होंने हमें रखने के लिए दिया था।
पैकेट लेकर सास ने फिर उसी बक्से में डाला और जमीन पर पड़ा ताला बक्से में लगाकर चाभी अपने आंचल की टोंक में बांध लिया।
सास बाहर निकली तो वह फिर अपना सामान सहेजने लगी। अपना क्या था? सब तो यहीं का था। वह खुद भी यहीं की हो चुकी थी। आज फिर मायके की हो रही थी। बल्कि अब कहीं की नहीं रह गयी थी। किनारी वाला एक झोला और प्लास्टिक की डोलची ही उसके मायके की थी। दो साड़ी, दो ब्लाउज, पेटीकोट, एक छोटा शीशा, एक कंघी, सिंदूर की छोटी डिब्बी, क्लिप का पैकेट और सूती शाल जो बिदायी के समय उसकी मामी ने दिया था। इन्हें रखने के लिए डोलची और झोला पर्याप्त थे। फ्रेम में मढ़ा पति के साथ तीन महीने पहले खिंचाया हुआ एक फोटो भी आले से झांक रहा था। इसे वह अपनी चीज मान सकती थी कि नहीं? जो भी हो, उसे भी उसने संभाल कर झोले में डाल लिया।
विदायी की बात जान कर आस-पास की औरतें भी आ गईं। एक लड़की ने उसकी डोलची और झोला उठा लिया। जेठानी उसे अंकवार में लेकर बाहर निकलने में मदद करने लगी। दो साल पहले घूंघट निकाले, गर्दन झुकाये, चूड़ियां खनकाते धीमें कदमों से चलते हुए उसने इस ड्योढ़ी में प्रवेश किया था। तांबे के पुराने बडे़ पैसे के बराबर बुन्दा लगाये, पान खाये, महावर से एड़ी रंगे, चुनरी ओढे़, हंसती हुई सास ने परिछन करने के बाद बडे़ दुलार से उसे डोले से उतारा था। पलास के ताजे नरम पत्तलों पर एक-एक पैर रखवाते हुए अंकवार में समेटकर ड्योढ़ी के अंदर ‘परवेश’ कराया था। एक-एक पत्तल बिछाने के एवज में नाउन ने नेग में एक-एक रूपये लिये थे। ग्यारह कदम के ग्यारह रूपये।काॅपते कदमों से चलती हुई वह बाहर आई। एक तरफ ससुर चारपायी पर बैठे थे। सिर का पल्लू थोड़ा आगे खींचकर उसने ससुर के पैर पकड़ लिए- खता कसूर माफ करना बाबू।
बूढ़ऊ फफक पड़े- बेटे को तो भगवान ले गये समधी। उन पर कोई जोर नहीं चला बहू को आप लिये जा रहे हैं। अब हमारे दिन किसके सहारे कटेंगे?
-वापस ले जाने के लिए तो भेजे नहीं थे समधी, लेकिन... कुच्ची के बाप का गला रूंध गया। वे अंगोछे से आंसू पोंछने लगे।
लड़की ने झोला और डोलची साईकिल के हैंडिल में दोनोें तरफ टांग दिया। जेठानी को भेंटेने के बाद कुच्ची ने सास के पैर छुए फिर औरतों के समूह से गले मिलने, पैर छूने लगी।
लौटी तो बाप ने पूछा -दे दिया सब?
उसने घूंघट तनिक उठाते हुए स्वीकार में सिर हिलाया।
बाप ने ऊँची आवाज में बताया- आप का दिया हुआ गहना-गीठी सास को सौप कर जा रही है मेरी बेटी। उसे इसी समय सहेज लीजिए समधी जी ताकि बाद में कोई तकरार न पैदा हो।
इतनी भीड़ देख कर बाहर बंधी भैंस खूंटे के चारों तरफ पगहे को पेरते हुए चोकरने लगी। यह भैंस भी गौने में उसके साथ मायके से आयी थी। उसके ‘आदमी’ को गवहीं खाने के नेग में दिया था उसके बप्पा ने। तो क्या उसके साथ भैंस को भी लौटना होगा?
वह धीमे कदमों से भैंस के पास गयी और उसके गले लग गयी। किसी की नजर उसके नंगे पैरों पर पड़ गयी। एक लड़की दौड़ कर अंदर गयी और चप्पल की जोड़ी लाकर उसे पहनाने लगी।
सास को अचानक दाॅती लग गयी। औरतों ने उन्हें गिरने से बचाया और जमीन पर लिटा दिया। उनके मुंह मे सीपी से पानी डालने की कोशिश होने लगी। मंुह पर छींटे मारे जाने लगे। औरतों के बीच फुसफुसाहट तेज हो गयी।
चतुरा अइया ने आगे बढ़कर उसके बाप से कहा- अभी बूढे़-बूढ़ी बहुत सदमें में हैं समधी। खुद अपने खाने की सुध नहीं है और खूंटे से चार-चार जानवर बंधे हैं। ये बिना चारा-पानी के मर जायेंगे। जाना तो एक दिन है ही लेकिन आज का जाना ठीक नहीं लग रहा है। महीने खांड़ में जब ये दोनों परानी कुछ संभल जाते तब ले जाते तो न अखरता।
बाप ने बारी-बारी सबके चेहरे देखे। फिर बेटी का मुंह जोहा। कुच्ची ने स्वीकृति में सिर हिलाया- ठीक है।
-हम एकाध महीने में आकर लिवा चलेंगे बिटिया।’ और साइकिल के हैंडिल में टंगी डोलची झोला उतारकर बेटी के हाथ में पकड़ा दिया।
0
हनुमान की लाश चिता पर रखने के साथ ही किसी चोर दरवाजे से बनवारी के मन में यह बात आयी थी कि अब हनुमान की खेती-बारी, घर-दुआर पर उसी का हक है। खून के रिस्ते में सबसे नजदीक वही ठहरता है। जगेसर, रमेसर दो सगे भाई। जगेसर से वह और रमेसर से हनुमान। उसे आज से ही काका-काकी का विश्वास हासिल करना होगा। पूरे चार बीघे की खेती है। चार बीघे का लालच कम नहीं होता। जमीन की कीमत पिछले पांच-छः साल में किस तरह आसमान पर चढ़ी है इसे क्या किसी को बताने की जरूरत है। यह तो कहो कि अभी काकी जिंदा हैं। न होतीं तो कौन रात के अंधेरे में अपनी औरत को काका का पैर दबाने के लिए भेज देता, कोई ठिकाना है। कौन कब बूढे़ को रातो-रात बोलेरो में बैठाकर ले उडे़। तहसील ले जाकर खुद को वारिस दर्ज करा ले या घर-बार, खेती-बारी की रजिस्ट्री करा ले, कोई ठिकाना है। जालिया लोगों के गिरोह मोटर साइकिल पर इन दिनो गांव-गांव घूम रहे हैं। किसकी खतौनी लगाकर दस-पांच लाख का लोन ले उड़े कोई ठिकाना है। बूढ़े, अशक्त, नावल्द या विधवा, तो उनके लिए नरम चारा है। पकड़ में भी आ गये, मुकदमे बाजी भी हो गयी तो उन्हें चिन्ता नहीं। मुकदमें का फैसला होने के पहले वे बूढ़े, विधवाएं बैकुण्ठ धाम चले जायेंगे। इसलिए न सिर्फ काका-काकी के खाने-पीने का बढ़िया इन्तजाम करना है बल्कि उनकी चैकीदारी भी करना है। कौन उनके घर आ जा रहा है, इस पर नजर रखनी होगी। उसने अपनी सुलछनी को अच्छी तरह समझा दिया है कि सुबह-शाम जाकर हालचाल लेती रहे। क्रिया-कर्म का खर्च-वर्च भले काका ने किया लेकिन दौड़-धूप का सारा काम उसी ने संभाला। यह औरत पता नहीं क्यो अब अपना रास्ता नहीं लेती, वरना वह काका-काकी को अपने चैके में ही खिलाने लगता। बाप तो बिदा कराने आया ही था। गांव की औरतें राह का रोड़ा बन गयीं। काकी को भी उसी समय दांती लगनी थी। बेटा मरा तो नहीं लगी दांती और पतोह जाने लगी तो दांती लग गयी। उसने सुलछनी को भी सहेज दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस औरत के लिए दूसरा घर-वर खोजने में अपने भाइयों को लगा दे।
इस औरत के जाते ही वह सबसे पहले काका को तहसील ले जाकर खतौनी में अपनी वरासत दर्ज करायेगा। फिर दोनों को लेकर उधर से ही चारों धाम की यात्रा पर निकल जायेगा। इस साल हनुमान दोनों लोगों को भेजने ही वाला था। कहंूगा हनुमान नहीं है तो क्या? मैं कोई गैर हूं। मैं भी तो बेटा ही हूं। सिर्फ खर्चा नहीं दूंगा साथ-साथ चलूंगा भी। सगे बेटे से बढ़ कर सेवा करूंगा।
कहते हैं बदरीनाथ का रास्ता इतना बीहड़ है कि कब कौन किस खड्ड में समा गया कुछ पता नहीं चल सकता। सीधे पतालपुरी पहंुचता है गिरने वाला। पहले के जमाने में तो जाने वाला अपना अच्छत, चावल, छीट परोर जाता था, यानी घर परिवार से अंतिम बिदा लेकर। लौट आये तो ठीक, नहीं तो जै सियाराम। रोते-पीटते लौटकर दोनों का किरिया-करम कायदे से निपटा देना होगा बस।
सहसा एक ख्याल ने उसके बदन में झुरझुरी पैदा कर दी। कहीं इस औरत की कोंख में हनुमान का अंश न ठहर गया हो? तब? आखिर दो महीने हो गये, यह जाती क्यों नहीं? इसके बाप ने लौटकर खबर नहीं ली। बिना इसके गये तो कोई ‘इस्कीम’ आगे बढ़ नहीं सकती।
वह सोचता है कि इतनी गुप्त स्कीम बनाने के पहले गांव के एकाध पिचाली लोगों का मन मुंह भी ले ले। कहीं फंसने-फसाने का खतरा हो तो उसकी काट भी खोज ली जाए। तीन-चार दिन पहले बलई बाबा बुलाने आये थे। सुलछनी बता रही थी कि उनकी ट्यूबेल ने पानी पकड़ना बंद कर दिया है। वह टाल गया था। सोच रहा था कि एकाध चक्कर और लगा लें तब जाय।
बलई बाबा खा पीकर रात के अंधेरे में दुआर से थोड़ा हटकर पाकड़ के पेड़ के नीचे मूंज की चारपायी पर बिना कुछ बिछाये लेटे हैं। नंगे बदन। पसीने से लथपथ। धोती को ऊपर तक खींच कर लंगोट की शक्ल दे दिया है। बाध पर पीठ रगड़-रगड़कर खुजला रहे हैं। हाथ का बना बेना डुला कर मच्छर भगा रहे हैं।
-बाबा पाय लागी।
-बनवारी उनका पैर छूने के साथ-साथ पैर दबाने भी लगता है।
-कौन? बनवारी। खुश रहो बेटवा। इतनी रात में?
-आप गये थे न मुझे खोजते हुये घर तक?
-हां-हां बेटवा। बोरिंग पानी छोड़ रही है। घंटे भर भी चलना मुश्किल।
-कल आकर देख लेते हैं।
-लेकिन छोड़ काहे रही है?
पाइप में लीकेज होगा या पानी का लेबल नीचे चला गया होगा। एक लेंथ पाइप लाकर डालना पडे़गा।
-कितने की आयेगी एक लेंथ? पैसा अभी लेते जाना।
-पैसा कहीं भागा जा रहा है बाबा! पहले ठीक कर दें फिर ले लेंगे।
-बहुत अच्छा किया जो तुमने यह काम सीख लिया। घर का आदमी घर का ही होता है। नहीं तो किसके पास दौड़कर जाते। और बताओ?
-और क्या बतायें बाबा। भगवान बड़ी विपत्ति में डाल गये। लछिमन जैसा भाई साथ छोड़ कर चला गया। सचमुच हनुमान की तरह आज्ञाकारी था। जहां लगा दो, जुट जाता था। उसी के बल पर मैंने बोरिंग का काम इतना फैला लिया था। समझिए दाहिना हाथ टूट गया। अब काका-काकी का बोझा भी मेरी खोपड़ी पर आ गया।
-तुम्हारी खोपड़ी पर क्यों? अभी तो रमेसर दोनों प्राणी खुद टाॅठ हैं।
-रखवाली तो करनी होगी बाबा। पता नहीं कब कौन किधर को भरमाने लगे, बहलाने-फुसलाने लगे। प्रापर्टी का मामला बहुत खतरनाक होता है, वारिस कमजोर दिखा तो जमीन फोड़ कर दस दावेदार पैदा हो जाते हैं। बुढ़ापे में बुद्धी भी बहुत आगे-पीछे चलने लगती है।
-तो साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नजर अभी से रमेसर की जगह-जमीन पर लग गयी है। कहने को तो कह दिया लेकिन उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि ज्यादा कड़ी बात कह दी। सबेरे उससे ट्यूबवेल बनवाना है। ऐसे में ऐसी कड़ी बात सर्वथा नीति विरूद्ध है।
-जगह-जमीन का लालच मुझे नहीं है बाबा। काका जब तक जिंदा है, जोते-बोंये। लेकिन उसके बाद तो मेरा हक बनता ही है। मैं यह तो न होने दूंगा कि कोई गैर उसके नजदीक
फटके। मेरे भी तीन-तीन बेटे हैं।
-तो गैर कहां से आ जायेगा? अभी तो हनुमान की बेवा ही मौजूद है।
-वहीं तो! अब उसका यहां क्या काम? दो महीने से खूंटा गाड़कर बैठी है। जवान, जहान बिना बाल-बच्चे वाली। उसे तो खुद ही अपना रास्ता पकड़ लेना चाहिए था। अब क्या मारकर निकाला जाये तब जायेगी?
-अरे भाई मार कर कैसे निकालोगे? ब्याह कर आयी है। कहने के साथ बलई बाबा ने अपनी जीभ काटी - यही आदत नहीं गयी उनकी। चाहे जितनी कड़वी हो, सही बात मुंह से निकल कर रहती है। जीभ यह भी नहीं सोचती कि किस आदमी से क्या गरज अटकी है। वे बहकी बात को संभालने की कोशिश करते हैं।
-अगर इतनी दूर की सोच रहे हो तो तुम्हीं क्यों नहीं रख लेते?
-मैं... बनवारी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया।
-और क्या। लम्बी चैड़ी है, कमासुत है, हंसलोल और जवान है।
-लेकिन वह तो मेरी भयहू लगेगी बाबा। भयहू को तो छू भी नहीं सकते। हनुमान मुझसे दस साल छोटा था। गोसाई जी बहुत पहले मना कर गये हैं- अनुज बधू भगिनी सुत नारी...। पाप पडे़गा।
-पाप तो तब पडे़गा जब कुदृष्टि से बिलोकोगे। उसे राजी कर लो। उसका मन जीत लो। सौ बात की एक बात, पट जाय तो सब जायज है।
बनवारी का हाथ बाबा के पैरों पर तेज-तेज चलने लगता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद फिर कहता है- मजाक तो नहीं कर रहे हैं बाबा? ऐसा हो सकता है?
-क्यों नहीं? उसे मर्द चाहिए, मर्द मिल जायेगा। तुम्हें परापर्टी चाहिए, परापर्टी मिल जायेगी। रमेसर दोनों परानी को रोटी चाहिए, उनकी रोटी पक्की हो जाएगी। सबका उखड़ा कूल्ह बैठ जाएगा। लेकिन...
-लेकिन क्या बाबा?
-कहते हैं दो औरतों के बीच पड़ा मर्द वैसे ही जलता है जैसे देशी भठ्ठे की ईंट। धुंआ निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। सुलछनी तुम्हारा जीना हराम कर देगी।
बनवारी कहीं खो जाता है। देर तक खोया रहता है। फिर उठते हुए कहता है- चलता हूं बाबा। ट्यूबेल कल शाम तक पानी देने लगेगी। परनाम।
नई और मन माफिक राह पाकर बनवारी का दिमाग और तेज चलने लगा है। इस इलाके में जमीन का रेट पांच-छः हजार का विस्वा चल रहा है। चार बीघा माने पांच-छः लाख। सुलछनी इतनी बुद्धू तो है नहीं जो हाथ आती परापर्टी को लात मारे। और मारेगी तो रहेगी कहां? अपनी जनाना का मुंह बन्द करना कौन मुश्किल काम है। रोज सुबह-शाम चार डंडा पडे़गा तो दस दिन में बोलती बंद हो जायेगी।
कुच्ची को उसने कभी भर नजर नहीं देखा। ऐसे तो रोज ही काम पर निकलते समय हनुमान को लेने उसके दरवाजे पर जाता था। मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही वह खाने के डिब्वे का झोला हनुमान को पकड़ाने के लिए घूंघट काढे़ निकलती थी। उसकी जवान देंह की महक हवा के झोंके के साथ उसकी सांसों में भी समाती थी। हवा के झोंके से कभी घूंघट हिलता तो लाल होंठों के बीच उजली हंसी की झलक भी मिल जाती थी। एकाध बार आंखों की मछलियां घूंघट के पीछे कौंधी भी थीं। ...और आवाज कितनी मीठी है। बोलती है तो लगता है गा रही है। वह कल्पना की आंखों से देखने लगा- कितनी मोटी-मोटी जंघायें। उसकी आंखों को सबसे ज्यादा पकड़ती हैं, उसकी भरी-भरी छातियां। उनका कदम-कदम पर हिलना, दलकना। बांधकर नहीं रखती। सुलछनी तो एकदम सीक सलाई है। उसका सब कुछ बहुत छोटा-छोटा है। उसके दाहिने पंजे में चुनचुनाहट होने लगी। सालभर पहले बाजार में एक गीत बजता था- गोरिया कै जोबना खजाना, गोरी दिलदार कब होए?
कैसे कोई दिलदार बनाता है?
आडे़ ओटे, अंधेरे उजाले में घात लगाकर ‘पटक’ तो कभी भी सकता है, लेकिन पटाना। पटकना जितना आसान, पटाना उतना ही मुश्किल। पटाने की विद्या वह आज तक नहीं सीख पाया... और आज देखो उसी विद्या की जरूरत पड़ गयी।
0
उस दिन दोपहर में पता चला कि कोआॅपरेटिव के गोदाम पर यूरिया बंट रही है। यूरिया की इतनी किल्लत रहती है कि आते ही खरीदारों की लाइन लग जाती है। गोदाम खुलते ही ढ़ाई-तीन घंटे में सारा स्टाक खतम। पिछड़ गये तो गये। रवी की फसल के लिए पन्द्रह-बीस दिन बाद जरूरत पड़ने वाली थी। बुढ़ऊ यूरिया लेने चले गये तो जानवरों को चराने के लिए उसे जाना पड़ा। शाम को जानवरों को चरा कर लौट रही थी तो देखा, खोर के बगल वाले खेत में जेठ धान के आखिरी बोझ के पास खडे़ हैं। अब तक तो जेठानी भी साथ-साथ ढो रही थी लेकिन लगता है आग-अदहन के लिए वह घर चली गयी। इन्तजार कर रहे होंगे कि कोई उधर से गुजरे तो उसे बोझ उठाने के लिए आवाज दें। वह पास पहुंची तो उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया- जरा उठा दे रे छोटकी।
वह न हां कह सकी न नहीं। सारी दुनिया को पता है कि छोटे भाई की पत्नी को छूने का पद नहीं पहुंचता बडे़ भाई का। बनवारी के दुबारा बुलाने पर वह खेत की मेड़ तक पहुंच कर बोली- हम कैसे उठा दें? छू नहीं जायेगा?
-छू कैसे जायेगा? बीच में तो बोझ रहेगा।
वह दुविधा में पड़ गयी।
पीठ पर पति की छाया रहती तब भी एक बात थी। बेवा औरत को ज्यादा ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। पता नहीं किस बात का क्या मतलब निकाल लिया जाय।
बनवारी ने मजबूरी बतायी- कोई और दिखायी पड़ता तो मैं खुद ही तुझे न बुलाता।.....
बात तो सही है। अगर वह बिना उठाये चली जाय तब भी ठीक नही लगता। अंधेरा हो रहा है। अब इधर से कौन गुजरने वाला है? ए पता नहीं कब तक किसी के इन्तजार में यहीं खड़े रह जाएं।
उसके गाय बैल आगे बढे़ जा रहे थे। कहीं किसी की फसल न चैपट करने लगें। वह जल्दी-जल्दी पास पहुंची। बोझ उठा कर बनवारी के सिर पर रखवाया और जैसे ही मुड़ने को हुई कि बनवारी ने दाहिने पंजे से उसकी बायी छाती दबोच ली।
उसने चिहुक कर उसके हाथ को झटकना चाहा लेकिन पकड़ इतनी सधी हुई थी कि मुक्त होने के लिए उसे जमीन पर बैठ जाना पड़ा। माख से उसकी आंखें भरभरा गयीं। इतना पाप पाले हुए हैं ए उसके लिए अपने मन में। संभली तो उठते हुए इतना ही बोल पायी- यह काम ठीक नहीं किया बड़कऊ।
-सब मन के मानने की चीज है, रे। बोझ को सिर पर साधते हुए मुड़कर बोला बनवारी- एक दूसरे के काम आने से जिंदगी हलुक (हल्की) होकर कटती है।
रूलाई के आवेग में उसे कुछ सुनायी नहीं पड़ा। बड़ी बेरहमी से पकड़ा था। जान निकल गयी। वह कुछ देर वहीं खड़ी की खड़ी रह गयी।
बनवारी की इस घटियारी के बारे में सास को बताए या नहीं? अगर किसी ने देख लिया हो और बाद में सास को बताए तो वे यही समझेंगी कि जरूर यह दोनांे का सधा बधा मामला होगा वरना बहू जेठ का बोझ उठाने क्यों जाती?
बड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद देर रात गये वह अपनी चारपायी से उठकर सास की चारपायी पर आयी और उनके पैर दबाने लगी।
-इतनी सेवा मत करो बहू। तुम्हारे जाने के बाद बहुत रोना पडे़गा।
बहू सिसकने लगी तो लगा कि वह कुछ कहना चाहती है। सास उठकर बैठ गयीं। पूरी बात सुन कर वे बड़ी देर तक चुप रह गयीं फिर उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए बोलीं- जमाना कितना खराब आ गया बिटिया। दिन गिरने पर अपनों की आंख का पानी भी मर जाता है। जब घर में ही डसने के लिए घात लगाने वाले पैदा हो गये तो न अब मेेरा रोकना ठीक रहेगा न तुम्हारा रूकना। हमारी जैसी बीतनी होगी बीतेगी। हम तो पके आम है । पता नहीं कब चू पड़ें। अभी तुमने जिंदगी में देखा ही क्या है। खेलने खाने की उमर में ही तो सब बिगड़ गया। मन को समझा लिया है कि हमारा तुम्हारा नाता बस इतने ही दिन का था। हम अपने रिस्ते के बंधन से तुम्हें उरिन (मुक्त) कर रहे हैं। मैं कल खुद ही तुम्हारे बप्पा को आने का संदेश भेजवाती हूं।
वह चुपचाप सिसकती रही। सास उसका सिर सहलाती रहीं। फिर बोली- बनवारी की ‘घटियारी’ को पानी की तरह पी जाना। बदनामी साथ लेकर जाना ठीक नहीं।
संदेश तो गया लेकिन इसके पहले कि उसके बप्पा आते, एक नयी विपत्ति आ गयी। मेंड से फिसल कर सास के जांघ की हड्डी टूट गयी। दूध देकर आ रही थीं। मेंड पसीजी हुई थी। फिसल गयीं। बनवारी की मदद से टेम्पो में लादकर ससुर अस्पताल ले गये।
टेम्पो ने तो सबेरे आठ बजे ही जिला अस्पताल के गेट पर उतार दिया लेकिन दोपहर तक बूढ़ी की भर्ती ही न हो सकी। पर्ची कटवाने के बाद बनवारी इसके उसके पास दौड़ता रहा। कभी कहा गया कि बेड खाली नहीं है। कभी कहा गया कि पहले एक्सरे कराकर दिखाओ। फ्रैक्चर होगा तभी भर्ती ली जायेगी। बूढ़ी बरामदे के एक कोने में लेटी कराहती रही। चूहे जैसी मूंछ वाला नर्सिंग होम का एक दलाल अलग पीछे पड़ा था। वह रमेसर को समझाने में लगा था कि बिना टेंट ढीली किए कुछ नहीं होने वाला। अगर हड्डी टूटी होगी और आपरेशन करना पडे़गा तो सरकारी डाक्टर भी बिना दस हजार एडवांस लिये हाथ नहीं लगायेगा। राड पडे़गी तो उसके लिये भी चैदह-पंद्रह हजार गिनना पडे़गा। तब हमारे नर्सिंग होम में अमरीकन डाक्टर से आपरेशन क्यों नहीं कराते? यहां तो अगर इनफेक्सन हो गया, मतलब जहर फैल गया तो सीधे पैर ही काट देंगे।
बुढ़ऊ सिर पर हाथ रख कर बैठ गये।
अचानक कुच्ची को धरमराज वकील की याद आई। गांव के पद से देवर लगता है। यहीं कचेहरी में होगा। बनवारी ने धरमराज को फोन किया। थोड़ी देर में धरमराज काला कोट पहने तीन साथी वकीलों के साथ दो मोटर साइकिल पर धड़धड़ाता हुआ आया। जो सामने पड़ गया उसी को घेर कर हड़काया- हमें पता है कि क्यों टरका रहे हो। सीधे-सीधे कटोरा ही क्यों नहीं थाम लेते? तनखाह किस बात की मिलती है?
दो तीन जगह हड़कम्प मचाने के बाद बुढ़िया चार बजे बेड तक पहुंची। नीचे से ऊपर तक का सारा स्टाफ मन ही मन उन्हें कोस रहा था। अब तक तो पत्रकार ही नाक में दम किये हुये थे। अब काले कोट वाले भी पहुंचने लगे।
जाते-जाते धरमराज ड्यूटी के डाक्टर को हड़काता गया- पाकेट से खर्च करके दवा खरीदने वाले मरीज नहीं हैं हम। जो दवा स्टोर में न हो उसकी लोकल परचेज करके दीजिए। स्टोर में पहुंचने के पहले तो बिक जाती है। रहेगी कैसे?
एक्सरे हुआ तो पता चला कि फ्रैक्चर है। आपरेशन होगा। पन्द्रह-बीस दिन अस्पताल में और दो-ढाई महीना घर में विस्तर पर लेटे रहना पडे़गा।
सही कहा था नर्सिंग होम के दलाल ने। पैसा न पाने के चलते डाक्टर तीन दिन तक आपरेशन टालता रहा। सबेरे कहता कि कल करेंगे। कल आता तो फिर कल पर टाल देता। देर होने से मवाद पड़ जाने का डर था। वार्डब्वाय और नर्स पहले दिन से ही डरा रहे थे कि जमराज से झगड़ा करके पार नहीं पाओगे तुम लोग, देहाती भुच्च। एक इंच भी पैर छोटा हो गया तो जिन्दगी भर भचकते हुये चलेगी बुढ़िया। देवर से कहो कि अपना रूआब कचेहरी में ही दिखाये। इस बार आ गया तो हाथ पैर तुड़ा कर इसी वार्ड में भर्ती होना पडे़गा।
सारे मरीज पैसा दे रहे थे। तय हुआ कि देने में ही भलाई है। आपरेशन के पहले शाम को दस हजार गिनने पडे़। राड भी उसी दुकान से खरीदना पड़ा जहां से डाक्टर ने कहा था।
ससुर और पतोहू के बीच ड्यूटी का बंटवारा हो गया। दिन में तो नर्स हैं, दायी हैं, जरूरत पड़ी तो बुलाने पर आ जातीं हैं लेकिन रात में दाइयां और नर्सें भी इधर-उधर झपकी लेने लगती हैं। बुलाने पर नहीं सुनती इसलिए औरत मरीज के पास औरत तीमारदार का रहना जरूरी हो जाता है। खास कर जब मरीज हिलडुल पाने की स्थिति में न हो। कपड़े बदलने के लिए या नीचे पैन लगाने के लिए।
वह जानवरों का चारा-पानी करके, खाना बनाकर, दूध दुह कर, अपना और सास का दोनों जून का खाना लेकर शाम को बाजार से टेम्पो पकड़ती है। आधे घंटे में शहर। फिर टेम्पो अड्डे से पैदल अस्पताल। तब ससुर घर लौटते हैं। सबेरे जानवरों को चारा देकर, शाम का बना खाना खाकर नौ-दस बजे तक वापस अस्पताल पहुंचते हैं, तब वह लौटती है।
उसकी सास के बगल वाले बेड पर एक बारह-तेरह साल का लड़का है पेड़ से गिरकर एक बांह और एक पैर तुड़वाकर आया है। उसका बाप महीने भर का राशन रखकर चला गया। गया तो फिर लौट कर नहीं आया। लड़के की मां एक जून रोटी सेकती हैै, दो दिन खाती है। दाल, सब्जी कुछ नहीं। बस, चटनी रोटी। गजब की ‘बोलका‘ है। सोते जागते उठते बैठते या तो कुछ बताती रहती है या कुछ पूछती रहती है।
कुच्ची को नर्सों की सफेद वर्दी बहुत अच्छी लगती है। दूध की तरह सफेद। एक भी दाग धब्बा नहीं। कितना साबुन खर्च होता होगा इनको धुलने में। ए लड़कियां एक भी गहना नहीं पहनतीं, नाक की कील के अलावा। चू़़ड़ी, बिन्दी कुछ नहीं। कान तक सूना।
‘कड़क‘ नर्स बस एक ही है, बड़ी नर्स। ऊंट की तरह लम्बी और पिपिहिरी की तरह पतली आवाज वाली। डाटने डपटने का बहाना खोजती रहती है। सास उससे बहुत घबराती है। उसकी आवाज सुनते ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करती हैं। लेकिन वह आते ही सीने पर थप-थप मार कर कहती है- पैर सीधा रखो। करवट नहीं लेने का। फिर सुर्ती खाया क्या? मुंह खोलो।
अपने सामने नीचे रखी बाल्टी में सुर्ती उगलवाती है फिर कुच्ची को डाँटती है- मना किया था न। फिर क्यों दिया सुर्ती? डिस्चार्ज करके भगा देंगे। गन्दी सब।
बिना सुर्ती खाये रह नहीं सकती बुढ़िया। पेट फूल जाता है। ‘कड़क’ के जाते ही कहती है- अब घर ले चल, आज ही ले चल। यहां एक दिन भी नहीं रहना। कितनी बदबू है चारो ओर। मेरी गृहस्थी बिगड़ी जा रही है।
गृहस्थी तो सचमुच बिगड़ी जा रही है। तीनो प्राणी अस्पताल से नत्थी हो गये हैं। जानवरों का चारा पानी मुश्किल से हो पाता है। लगता था खेत परती रह जायेंगे। कोई अधिया पर बोने के लिए तैयार नहीं हुआ। तेरह मूठी के जवान बैल खूंटे पर बंधे-बंधे खा रहे हैं। जोते कौन? आखिर एक दिन किराये का ट्रैक्टर मंगाकर किसी तरह बीज डाला गया। रोटोवेटर से दो घंटे की जुताई के दो हजार रूपये लग गये। फरूही करना, (क्यारी बनाना) अभी बाकी ही है।
धान तो कट गया था लेकिन उसकी मंड़ाई बाकी थी, तभी अस्पताल की दौड़ शुरू हुई। अब आये दिन आसमान में बादल के टुकडे़ तैरते नजर आते हैं। पानी बरस गया तो खलिहान में ही सारा धान जम जायेगा। ऐसे में सास की चिन्ता गलत नहीं है। लेकिन डाक्टर जाने दें तब न।
अस्पताल आने पर तो लगता है सारी दुनिया ही बीमार है। हर जगह मरीजों का रेला। इमरजेंसी वार्ड का एक नम्बर बेड अंदर घुसते ही ठीक सामने पड़ता है। सबेरे की शिफ्ट वाली अधेड़़ दायी इसे सबसे पहले ‘रेडी‘ करती है। उस दिन एक लड़का आकर उस पर बैठ गया तो उसने फौरन उठाया- उठो-उठो। इसकी बुकिंग आने ही वाली है।
- आपको आने के पहले ही पता चल गया?
- हां बेटा, रोज आती हैं। बिना नागा। कोई ना कोई कहीं न कहीं से चल पड़ी होगी। उसके पास एक मिंट का समय नहीं होगा। शाम तक तो रवानगी भी हो जाती है, ‘डिस्चार्ज‘।
तब तक सचमुच अठारह - बीस साल की एक लम्बी तगड़ी सांवली लड़की को पकडे़ तीन चार लोग लाते हैं। वह दर्द से छटपटा रही है और ओक-ओक करके ‘कै‘ करने की कोशिश कर रही है। बेड पर लिटाने के साथ, हाथ पैर दबा कर उसकी उछलती देंह को काबू में किया जाता है। वह बार-बार उठ कर भागने की कोशिश कर रही है। लगता है पेट में आग लगी है। मुंह से झाग निकल रहा है। डाक्टर, नर्स और दाइयों के झुंड ने बेड को घेर लिया है। नाक के रास्ते पेट में प्लास्टिक की नली डाली जा रही है। नाक पर टेप लगा कर सेट किया जा रहा है। हाथ में इंजेक्शन के लिए ‘वीगो‘ लगाया जा रहा है। हाथ बांधो... पैर बांधो। छोटे पम्प से पेट की सफाई शुरू हो गयी। पेट में दवा पहुंचाई गयी। इंजेक्शन लग गया। हाथ से फिसलती जिंदगी को बचाने के लिए युद्ध स्तर का प्रयास।
डाक्टर नर्स जा चुके हैं। लड़की अब रोने लगी है। ऊपर झुकी दायी के गले में हाथ डालने की कोशिश करते हुए अस्फुट स्वर में बुदबुदाती है- बचाई लेव अम्मा... हमार बिटिया क मुंह देखाइ देव...
-धीरज धरौ बिटिया, धीरज धरौ। माया दायी उसके आंसू पोछती हैं फिर मुंह फेर कर बुदबुदाती हैं- घंटा, दुइ घंटा मा मुक्ती मिल जाये।
इस बेड का नाम ही है- ‘प्वाइजन बेड‘। जहर खाकर आने वाली औरतों के लिए रिजर्व। रोज इसी समय कोई न कोई आती हैं, बिना नागा। सिर्फ औरतें। आदमी एक भी नहीं। सब बीस-पचीस साल की उम्र वाली। ज्यादातर ‘सल्फास‘ खाकर। गांव देहात के घरों में वही सहज उपलब्ध है।
शाम को या रात में झगड़ा होता होगा। मार पड़ती होगी। आधी रात में खाकर छटपटाने लगती होंगी। लेकिन इतनी रात में कहां सवारी खोजें? सबेरे लेकर चलते हैं। तब तक जहर असर कर चुका होता है।
लड़की धीरे-धीरे शिथिल पड़ रही है। उवलती हुई आंखे पथराने लगी हैं।
शाम होते-होते खेल खतम। चमकता हुआ शरीर मिट्टी हो गया। पलकें दबाकर अधखुली आंखे बंद की गयीं। मरने का रूक्का बना। सफेद चादर से ढकी, स्टेªचर पर लद कर चीर घर की ओर चल पड़ी। सात-आठ बजते-बजते बेड खाली। चादर बदलो तकिया बदलो। अगले मेहमान के स्वागत की तैयारी।
कौन थी? क्यो खाया जहर?
हर दिन की अलग कहानी। अवैध गर्भ। पति द्वारा पिटाई। दहेज प्रताड़ना। तीसरी बेटी पैदा कर देना।
बेड नं. 7 बर्न बेड है। यह भी सबेरे-सबेरे अपना चादर तकिया बदल कर तैयार हो जाता है। इस पर आने वाली औरतों में ज्यादातर नवव्याहताएं होती हैं। किसी की गोद में साल भर की बच्ची, किसी की गोद में छः महीने की। वह बेड भी शायद ही कभी खाली रहता हो। जहर खाने वालियों की मुक्ति तो उसी दिन हो जाती है लेकिन जलने वालियां चार-पांच दिन तक पिहकने के बाद मरती हैं। कभी-कभी पूरा शरीर संक्रमित होने में हफ्ते दस दिन लग जाते हैं। कितनी बहू बेटियां हैं इस देश में कि रोज जलने और जहर खाने के बाद भी खत्म होने को नहीं आ रही हैं?
सबेरे घर वापसी से पहले अब कुच्ची इमरजेंसी के 1 नंबर और 7 नम्बर बेड का एक चक्कर जरूर लगाती हैं। लौट कर सास को आॅखों देखा हाल बताती है। फिर पूरे दिन उदास रहती है। दुनिया को जितना नजदीक से देखती है उतना ही दुखी होती है।
उस दिन वापस घर पहुंची तो देखा बैलों के खूंटे सूने पडे़ थे। गाय और भैंस रह रहकर रंभा रहीं थीं। शायद पगहा तुड़ा कर आस-पास चरने चले गये हों। वह अगवाडे़-पिछवाड़े देख आयी। तब तक सुलछनी आती दिखी। किसी के न रहने पर वह इधर का एकाध चक्कर लगा जाती है। उससे पूछा।
-बिक गये।
-बिक गये?
-हां। पैकवार दो दिन से आ रहा था। आज सौदा पट गया। सबेरे ही तो हांककर ले गया।
वह चुप रह गयी। बेचने के पहले ससुर ने कोई चर्चा तक नहीं की। हो सकता है सास से सलाह की हो। जाते हुए दोनों को देख भी न पायी। थके कदमों से चले गये होंगे। गाय और भैंस उन्हीं की याद में रंभा रहीं हैं।
पता चला कि सास को भी नहीं मालूम। उनसे भी कोई राय सलाह नहीं की। बेचने के बाद सारे दिन उनके पास बैठे रहे लेकिन तब भी नहीं बताया। अगले दिन सास ने पूछा तो बोले- अब कौन उन्हेें खिलाता और कौन जोतता? मेरे वश का तो है नहीं। बेकार बांध कर खिलाने का क्या मतलब?
-कभी चर्चा भी नहीं किए। पूछे भी नहीं।
-किससे पूछते? तुमसे? जो लंगड़ी होकर यहां पड़ी हो। कि बहू से? जो आज गयी कि कल।
-कितने में फेंके?
-सोलह हजार में।
-बीस हजार में तो दो साल पहले बेटा खरीद कर लाया था। तब चार दांत के थे। अब पचीस हजार से कम के न थे।
-मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है हनुमान की अम्मा। अब न कुछ पूछो, न बताओ।
शाम को वह पहुंची तो बूढ़ी उसके गले में बांह डालकर रोने लगी।
-सब बिगड़ गया बिटिया। उस एक के जाते ही सब बिगड़ गया। भगवान तेरे पेट में एक बिरवा रोप दिए होते तो हम जी जाते। तब मैं थोड़े तुझे कहीं जाने देती। उसी के सहारे हम सब जिंदगी काट देते।
सास को खिलाने और दवा देने के बाद वह फर्श पर बिछे अपने बिस्तर पर लेटी तो फिर उसकी आंखों में हनुमान का चेहरा नाचने लगा। गुलाबी मसूढ़ो वाला हंसता हुआ चेहरा। मुराही (शरारत) से चमकती आंखों वाला। वे दिन में उसे कुच्चो रानी और रात में कंचनजंघा कहते थे। कहीं से आते तो कोठरी के एकान्त में पहले उसके स्तनों को दबोचते फिर पूछते- यह बायां वाला दाहिने से छोटा क्यों है? इसे भी महीने भर में दाहिने के बराबर कर देना है। कभी कहते -मां बाप ने मेरा नाम हनुमान रखा है। मुझे बाल बरम्हचारी रहना था। तुमने आकर सब भरभंड कर दिया।
-मैं क्या तुम्हे बुलाने जाती हूं। कहीं से आते हो तो सीधे कोठरी में ही घुस आते हो। दिन में तो बरम्हचारी रहा करो।
वे भी इन्तजार कर रहे थे उस विरवे के अंखुआने का। उन्होंने तो नाम भी सोच लिया था- बालकिसन। उसके पेट को सहलाते हुए पूंछते- कब आयेगा रे मेरा बालकिसन? फिर पेट से कान सटा कर कहते- शायद आ गया। किलकारी की आवाज सुनायी पड़ रही है।
उमड़ते आंसुओं को आंचल से पोंछते हुए वह बुदबुदायी- हम तुम्हे तुम्हारा बालकिसन नहीं दे सके राजा।
कल से ही उनकी छवि मन में बसी है। कल शाम बितानू आया था। हनुमान का हेल्पर। पता चला कि अम्मा अस्पताल में भर्ती हैं तो देखने चला आया। कह रहा था कि बडे़ मिस्त्री (बनवारी) की खोपड़ी में पैसे की गर्मी घुस गयी है। अब वह उनको और तेल नहीं लगायेगा। खुद अपना काम शुरू करेगा। उसने बताया कि बडे़ मिस्त्री के पास बोरिंग का जो सामान है उसकी खरीद में आधा पैसा हनुमान भैया का लगा है। अगर बंटवारा करके आधा सामान उसे दिला दिया जाय तो उसका काम चल निकले। वह महीने महीने किराया देता रहेगा।
-यह बात तो सीधे बाबू से कहो बितानू। मैं तो चार दिन की मेहमान हूं।
-अच्छा भाभी, जमीन वाला कागज बडे़ मिस्त्री ने भइया को दे दिया था कि नहीं?
-कौन सी जमीन?
-पिछले साल दोनों भाइयों ने बाजार में दुकान खोलने के लिए साझे में जमीन खरीदी थी। उसकी रजिस्ट्री का कागज बडे़ मिस्त्री के पास था। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि चार पांच महीना पहले उसी के लिए दोनों भाइयों में कुछ कहा सुनी हुई थी।
कुच्ची ने बितानू का स्टूल अम्मा के सिरहाने रखवाते हुए कहा- जरा अम्मा को बता दो यह बात।
बूढ़ी ने भी ऐसी किसी जमीन या कागज की जानकारी से इंकार कर दिया। फिर कहा- बितानू बेटवा, तुम यह बात हमारे बुढ़ऊ के कान में जरूर डाल देना।
एक और शंका पैदा कर दी बितानू ने- जैसे पिचाली हैं बडे़ मिस्त्री, हो सकता है रजिस्ट्री में हनुमान भइया का नाम ही न डलवाये हों।
सास बहू उसका मुंह देखने लगीं।
-ऐसा न होता तो बडे़ मिस्त्री कागज देने में आनाकानी क्यों करते?
-सही बात! दोनों के मुंह से एक साथ निकला।
-इसलिए काका से कहिए कि रजिस्ट्री आफिस जाकर पता लगायें। अगर लिखते समय ही धोखा हो गया है तब तो अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन अगर कागज में दोनों भाइयों का नाम है तो अपना हिस्सा नपवा कर फौरन बाउन्डरी करवा लें। अगर बडे़ मिस्त्री ने मकान बनवाकर पूरी जमीन घेर ली तो ताजिंदगी कब्जा नहीं मिलेगा।
दोनों औरतों के सिर एक साथ सहमति में हिले। फिर बूढ़ी बोली - इसका पता तुम्ही लगा सकते हो बाबू। बुढ़ऊ के वश का नहीं है।
-एक बात मेेरी समझ में नहीं आती काकी। बडे़ मिस्त्री हनुमान भइया को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले गये? घर क्यों ले आये। अगर वहीं से लेकर अस्पताल भागे होते तो हो सकता है भइया की जान बच जाती। वही जहरीली दारू दो लेबर भी पिये थे। उन्हें लोग सीधे मेडिकल कालेज ले गये और उनकी जान बच गयी।
-दारू तो वे कभी पीते नहीं थे।
-एक दो बार पिये थे।
-दारू कहाँ मिली?
-मधुबन के जंगली सिंह ने नयी बोरिंग करायी थी। उसी दिन बिजली का कनेक्सन मिला था। उसी का जश्न था। बडे़ मिस्त्री एक खराब मोटर चेक करने चले गये थे। उनके लौटने में देर होने लगी तो ए लोग पीने लगे। जब तक बडे़ मिस्त्री लौटे तब तक इन लोगों की हालत खराब होने लगी तो बडे़ मिस्त्री पीने से बच गये।
तब से कुच्ची को लग रहा है कि जेठ ने जानबूझ कर खुद को जहरीली दारू पीने से बचा लिया और उनको अस्पताल पहुंचाने में देर कर दी। जमीन और दारू के बीच में कुछ ‘कनेकसन’ जरूर है।
सारी दुनिया के मर्द कहते हैं कि औरत के पेट में बात नहीं पचती। तुमने भी मुझे विश्वास लायक नहीं समझा राजा।
0
टूटे हाथों वाला लड़का डिस्चार्ज हो गया। लेकिन जाने के पहले उसकी मां ने कुच्ची को एकान्त में ले जाकर बहुत खाते-पीते घर के एक विधुर लड़के के बारे में बताया-अब इस बुढ़िया का पैर दबाने से क्या मिलने वाला है? अपने बाप को मेरे पास भेजना।
उसी ने सारी नर्सों, दाइयों और बार्ड ब्वाय तक को बता दिया है कि कुच्ची का आदमी मर गया है और वह जल्दी ही उसके लिए दूसरे मरद का इंतजाम कर रही है।
एक नर्स है कुट्टी। लम्बी, पतली, सांवली। लंगड़ी हिन्दी बोलने वाली। उसको देख कर लम्बी मुस्कान बिखेरती है। कहती है- मेरा तेरा एक नाम- कुच्ची और कुट्टी। तो दोनों सिस्टर-सिस्टर हुआ।
एक दिन मुस्कराकर पूछा- दूसरी शादी कब बनाएंगा?
कुच्ची भी मुस्करायी- जब तुम बनायेगा।
-ना बाबा। हम तो कब्भी नहीं बनाएंगा।
-क्यों?
-हमको जलने से बहुत डर लगता। दारू पीकर आयेंगा और केरासन डालकर जला देगा।
लेकिन बाद में पता चला कि इसके तो एक बेटा भी है। सात-आठ साल का। एक दिन बस्ता टांगे स्कूल से अस्पताल आ गया था।
कुच्ची ने पूछा- तुम्हारे तो बच्चा है।
-बच्चा बनाया, मगर शादी नहीं बनाया।
-तो बच्चा कैसे बनाया?
-बच्चा एक फ्रंेड से ‘गिफ्ट‘ लिया। उसके साथ महीने भर सोया और बच्चा मिल गया। फ्रंेड़ बोला- शादी बनाएगा? हम बोला- नहीं। हसबैंड बनते ही ‘लभर‘ डेमन बन जाता। डेमन समझती?
-मरद की जरूरत तो पड़ती है न। कुच्ची मुस्करायी।
-जरूरत पड़ने पर मरद मिल सकता। जरूरत पड़ने पर बच्चा मिल सकता। सैंडिल खटखटाकर जाती हुई कुट्टी मुड़कर मुस्कराते हुए बोली- मरद नहीं, हसबैंड खतरनाक होता।
अगले दिन, फिर अगले दिन कुट्टी ने पता नहीं क्या-क्या बताया। क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। एक हीरोइन ने एक खिलाड़ी से ‘गिफ्ट‘ लिया। एक लेडी डाक्टर ने बीज बैंक से ‘गिफ्ट‘ लिया। बाहर के मुल्कों में तो जाने कबसे ‘गिफ्ट‘ का लेन-देन चल रहा है।
गिफ्ट? माने भेंट। माने चीन्ह, माने निशानी। मुंदरी और रूमाल का गिफ्ट तो सुना था उसने। अब यह बच्चे का गिफ्ट भी चलन में आ गया?
0
उस दिन शाम को कुच्ची ने जानवरों की सरिया में मच्छरों को भगाने के लिए भूसे के ढेर में नीम की पत्तियां मिलाकर धुंआ सुलगाया। भैंस लगाया। दूध उबलने के लिए आंगन में गांेइठे की आंच पर रखा और बगल में मचिया पर बैठकर सब्जी काटने जा रही थी कि किवाड़ खुलने की आहट आयी। देखा तो बनवारी सीधे उसी पर नजर गड़ाये आधे आंगन तक आ गया था। वह सिर से पैर तक जलभुन गयी। न खांसना न खखारना। खांस खखार कर घर के अंदर आने का मर्दों का कायदा रहा है ताकि औरतें अपना कपड़ा लत्ता सही कर लें। पता नहीं कौन किस हालत में है। पहने ओढे़ है कि उघार है। पता तो है इनको कि मैं घर में अकेली हूं। वह गुस्से से कांपने लगी। घूंघट नहीं किया। सीधे मुंह उठा कर देखा। अंदर ही अंदर सावधान हो गयी।
-जरा आग देना रे छोटकी। बीड़ी जलाना है।
वह उठकर खड़ी हो गयी।
-अकेली औरत के आंगन तक, चोर की तरह घुस आये। बाहर सरिया में उतनी आग सुलग रही है, वह नहीं दिखायी पड़ी।
ऐसी शुरुआत की उम्मीद नही थी बनवारी को। उसने मुस्कराने की कोेशिश की- उससे ज्यादा आग तो मेरे दिल में जल रही है छोटका। तुमको दिखायी पडे़ तब न।
-मुझे जो दिखायी पड़ रहा है उससे परलै (प्रलय) आ जायेगी। खैर इसी में है कि मेरे रास्ते से हट जाओ।
हंसिए वाला हाथ हवा में लहराते हुए उसने ललकारा- बाप की तरह लगते हो और राल चुआते शरम नहीं आती?
-पहले मेरी बात तो सुनो कुच्चन। मुझे दुश्मन क्यो समझती हो? मैं दोनों को रख लूंगा। इस घर में तुम राज करो। उस घर में सुलछनी। कहीं जानें की जरूरत क्या है?
-कान खोल कर सुन लो। हमारी राहे जुदा हैं और जुदा रहेंगीं। फिर कभी मेरी राह काटने की कोशिश किए तो अपने और तुम्हारे खून की धार एक कर दूंगी।
अब? क्या-क्या कहने की सोच कर आया था। सोचा था, कहेगी- मुझे पता है कैसे रखोगे। आधी रात में जेठानी को घसपिटने से पीटते हो तो उसका अल्लाना सारा गांव सुनता है।
वह कहता- कसम ले लो जो तुम्हें फूल की पंखुरी से भी मारूं। रानी बना कर करेजे में रखूंगा। तब हो सकता है मुस्करा देती। लेकिन यहां तो शुरूआत ही बिगड़ गयी।
अपने पचास साला हेल्पर नसीर को वह औरतों के मामले में उस्ताद मानता है। कई दिन से उस्ताद के साथ सोच विचार चल रहा था। आगे पीछे की सारी संभावना सोच कर उस्ताद ने डायलाग तैयार कराये थे। कहा था- वह औरत ही क्या जो सीधे-सीधे हां कर दें। औरत की ना में ही हां छिपा रहता है। उसे पहचानने की नजर चाहिए। लेकिन उसे तो कहीं से भी हां के लच्छन नजर नहीं आते। उस्ताद ने कहा था वह मर्द ही क्या जो ना सुन कर पीछे हट जाय। हिम्मत और हिकमत से टेढ़ा काम भी बन जाता है। अकेले में मिल गयी और नहीं मानती तो आगे बढ़ कर गिरा देना। हो सकता है, दिखाने के लिए थोड़ी देर हाथ पैर झटके लेकिन अंत में चुप हो जायेगी। और अगर चीखी चिल्लाई भी तो तुम्हारा क्या। वही बदनाम होगी और धीरे-धीरे टूट जायेगी। मंुह काला कर दो तो कहीं जाने लायक रहेगी ही नहीं।
आज सबेरे से ही वह तैयारी में था। काम पर नहीं गया। बाजार जाकर फकीरे की सैलून में दाढ़ी बाल बनवाया। मूंछे छंटायीं, उनमें पके बाल नोचवाये। नहाया-धोया, तेल लगाया। कुर्ता धोती पहना। जूता-मोजा डाटा। सुलछनी को चरी काटने भेज कर निश्चिंत हो गया। पता था कि काका अस्पताल में हैं। वह घर पर अकेली है। मान जाती तो लोय लग जाती। इससे जो बेटे पैदा होते वे जवान होने पर हरियाणा नशल के सांड़ों की तरह दिखते। चार-पांच भी हो जाते तो सारे गांव को पानी पिला देते। जिधर से हंकड़ते हुए निकलते लोग राह छोड़ कर हट जाते। सुलछनी के पेट से तो मरकट जैसे पैदा हुए हैं तीनों। एक लट्ठ पड़ जाय तो पोंक मारें।
कुच्ची की आंखों में उतरा खून देखकर उसे प्यार मोहब्बत के सारे बोल भूल गये। हंसुए की धार के आगे कोई हिकमत नहीं सूझ रही है। लेकिन औरत के आगे से मैदान छोड़ कर हटना... वह फिर हिम्मत जुटाता है। सूखे होंठ चाट कर दहाड़ने की कोशिश करता है- तो तू भी कान खोल कर सुन ले। इस गांव में एक ही शर्त पर रह सकती है। मेरी जांघों के नीचे बिछना कबूल करके। वरना भागना पडे़गा। सीधे नहीं तो टेढे़।
-मैं किस घाट लगूंगी यह तो ऊपर वाला ही जाने। जिंदा रहूंगी या कहीं बह बिला जाऊँगी, क्या पता। लेकिन इस जनम में तेरी जांघ के नीचे नहीं बिछूंगी, यह बात तू गांठ बांध ले। दगाबाज! हत्यारा कहीं का!
बनवारी एक एक कदम पिछड़ते, फुफकारते हुए किवाड़ के पास तक गया फिर झटके से सीधा हुआ। ऐं। यह कौन? लाले लोहार की बहू। कब से किवाड़ से सटी खड़ी है?
वह रूका नहीं। उस पर उड़ती सी नजर डालकर गली में गायब हो गया।
0
पन्द्रह दिन में ही डाक्टरों ने तुम्हे अपने पैरो पर खड़ा कर दिया? बूढ़ी से मिलने आयी पड़ासे की औरतें अचरज करती हैं ।
-डाक्टरों ने नहीं, मेरी इस बहू ने। बूढ़ी पास खड़ी कुच्ची की कलाई पकड़ते हुए कहती है - सगी बेटी भी पेशाब पाखाना साफ करते हुए एक बार घिनायेगी लेकिन यह तो बेटी से भी बढ़कर निकली। इसी की सेवा से उठ कर खड़े हुए हैं।
कुच्ची ने बताया - लोहे की छड़ डालकर नट बोल्ट से कस दिया, और ऊपर से माँस चमड़ा ढक कर सिल दिया।
-अरे गजब! उन्हे यकीन नहीं होता।
-यह जो लोहे का गोला है, इसे वाकर कहते हैं। इसके सहारे धीरे-धीरे चल सकती हैं। बस टूटे हुए पैर पर महीने भर जोर नही डालना है। तीन चार महीने में हड्डी पूरी तरह जुड़ जायेगी। इस बीच दिशा मैदान के लिए उठते बैठते समय किसी का सहारा लेना पड़ेगा, बस।
-राम करें, तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। बूढ़ियाँ असीसती हैं।
बूढ़ी कुच्ची का हाथ पकड़े पकड़े कहती है - लगता है पिछले जनम में यह मेरी बेटी थी।
कुच्ची का बाप आया और सारी बात जान समझ कर लौट गया। जैसे इतने दिन बीते वैसे चार महीना और सही।
बनवारी ने सुलछनी को बूढ़े बूढ़ी का दिल जीतने के काम में लगा दिया। दिल जीतना और सास बहू के बीच शंका और झगड़े का बीज बोना। जितनी जल्दी शंका का पेड़ फल देगा उतनी जल्दी यह औरत यहाँ से दफा होगी। वह खुद भी सुबह शाम हाजिरी लगाने की कोशिश करेगा।
बुढऊ का दिल जीतने के लिए ज्यादा उद्यम करने की जरुरत नहीं है। नहाते समय पहुँच कर हैंड पम्प चला देने या गीली धोती धोकर फैला देने भर से खुश हो जाने वाले जीव हैं बुढऊ। बूढ़ी को सिर में तेल लगाकर कंघी करके और जुँआ निकाल कर खुश कर देगी। सास को खुश करने का सबसे कारगर हथियार है बहू के काम में मीन मेख निकालना। सुबह शाम दिशा मैदान लेकर चली जाये तो अकेले में चाहे जितना कान भरे।
सुलछनी की सेवा देख कर तीनो प्राणी खुश भी हैं और हैरान भी। इसका मतलब दिल की बुरी नहीं है सुलछनी। लेकिन बनवारी के स्वभाव में आयी नरमी और अपनापन जरूर अचरज में डालता है। सिर्फ कुच्ची को बनवारी का सामने पड़ना बर्दाश्त नहीं होता। वह सामने से हट जाती है।
एक जल्दबाजी को लेकर बनवारी पछता रहा है। जब बूढ़ी अस्पताल में थी तो उसने साझी आबादी की जमीन का दो तिहाई घेर कर अपनी सरिया की नींव डाल दी जबकि कायदे से उसका हक आधी जमीन पर ही बनता है। नींव डाली तो डाली, उसका एक मोहार (द्वार) भी काका की तरफ खोल दिया। अब यह तो कोई भी समझ सकता है कि जिस दिन वह इस मोहार के सामने चार खूँटे गाड़ देगा, लगभग सारी जमीन उसके कब्जे में आ जायेगी। यह काम करने का सही समय अभी नहीं आया था, पर चूक हो गयी। भगवान करे इस चालाकी पर काका की नजर न पड़े।
काका की तो नहीं लेकिन काकी की नजर इस पर अस्पताल से लौटते ही पड़ गयी। पहले उसने कुच्ची की खबर ली। कुच्ची ने दुहाई दी कि हिस्सेदारी का मामला उसकी समझ में नही आया। तब बूढ़ी ने बुढ़ऊ को जाकर काम रोकवाने के लिए कहा लेकिन बुढ़ऊ की टोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। उल्टे बूढ़ी को ही समझाने लगे - उसकी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। वह तो अब गिरने से रहीं। वह झगड़ालू आदमी है। अपने दिन खराब चल रहे हैं। हमेशा के लिए बिगाड़ हो जायेगा।
-जब नींव खोद रहा था तब आपकी आँखें फूट गयी थी?-मुझे मौका कहाँ मिला पिछवाडे़ जाकर देखने का? सारा दिन तो अस्पताल में बीत जाता था। और अब हमारे आगे पीछे कौन है? किसके लिए टंटा किया जाये?
-इतनी जल्दी मरे भी नहीं जा रहे हैं। अभी से धनुहा-बान रखने से कैसे बीतेगी?
लेकिन बुढ़ऊ उधर झाँकने नहीं गये।
एक दिन कुच्ची को एक किनारे ले जाकर सुलछनी बोली - तेरे लिए एक लड़का ढूँढा है। एक दम गभरू जवान। मेरे जीजा का छोटा भाई है। तू देखते ही मोहित हो जायेगी।
कुच्ची उसका मुँह ताकने लगी।
-मेरे घर आकर बैठा है। बम्बई कमाता है। चल दिखा लाऊँ।
-दीदी, उनको पहले बप्पा के पास भेजो। जो करेंगे बप्पा ही करेंगे।
-अरे, उसके साथ सोना तुझे है कि बप्पा को। पहले तुझे तो पसन्द आये। फिर उसको गुदगुदाते हुए हँसी - अच्छा तू बाल्टी लेकर हैंडपम्प तक आ जा। वह तो देख ले अपनी महारानी को।
फिर उसका हाथ पकड़ कर बाहर खींचते हुए समझाया - सोने जैसी जवानी को अकेले गला कर राँगा करने में कौन सी अकलमंदी है?
एक दिन शाम को बितानू आया। सुलछनी के रहने तक इधर उधर की बाते करता रहा। उसके जाने के बाद बताया - कालिका बनिया की जमीन खरीदी गयी है। कालिका ने बताया कि लिखाते समय दोनो भाई मौजूद थे। दोनो भाइयों की दसखत हुई है।
सुन कर तीनो प्राणी देर तक ऊभ-चूभ होते रहे।
-बनवारी को कागज देना होता तो हनुमान के जिंदा रहते दे देता। कागज पाने का और कोई रास्ता नहीं है?
-है क्यो नहीं? रजिस्ट्री आफिस जाना पड़ेगा। कालिका से रजिस्ट्री की तारीख पता करके काका के नाम से नकल की दरखास्त लगानी पड़ेगी। थोड़ा टैम लगेगा। थोड़ा खर्चा लगेगा।
-तो वही करो। जो भी खर्चा लगेगा देंगे। बूढ़ी बोली।
- ठीक है। बितानू उठते हुए बोला - और बोरिंग के सामान का क्या सोचा काका? दिला देते तो मेरा काम भी शुरु हो जाता।
-मैं दिलाऊँगी बितानू बेटवा। मुझे ठीक हो जाने दो। ए तो बनवरिया के सामने पड़ते ही गूँगे हो जाते हैं।
बितानू के आने की खबर पाकर चैंक गया बनवारी। पता नहीं क्या लगाई बुझायी कर गया होगा। उसका रास्ता बंद करना होगा।
सुलछनी को पता है कि बुढ़ऊ को महुए का ठोंकवा और पना-बड़ा बहुत पसंद है। ठोंकवा तो कई दिन पहले बना कर खिला गयी थी। आज पना-बड़ा बना कर लायी है।
बूढ़ी कहती है - क्यों परेशान होती है?
-इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं आपकी बहू नहीं हूँ?
-वह तो ठीक है लेकिन अभी तो तेरी देवरानी है ही पकाने खिलाने के लिए। जब नहीं रहेगी और मेरा जाँगर घट जायेगा तो तेरे सिवा दूसरा कौन है खिलाने वाला?
सुलछनी के जाने के बाद कुच्ची कहती है - अम्मा, मेरा मन नहीं करता कि इसके हाथ का बना खाना खाऊँ। इन दोनो के मन में चोर है। क्या पता किसी दिन जहर ही खिला दें।
-हो सकता है। बुढ़ऊ बोले - बनवरिया कुछ भी कर सकता है। लाओ, कुतवा को खिला कर देखते हैं। अभी पता चल जायेगा।
-पागल हो गये हो क्या? बूढ़ी डाट लगाती है- कुतवा बेचारे की जान लेने की क्या जरुरत है? अँधेरा हो गया है। ले जाओ घूरे में गड्ढा खोद कर गाड़ दो।
कई दिन बाद, बूढ़ी के सिर में तेल लगाते हुए सुलछनी ने गोली दागा - एक बात बताना चाहती हूँ अम्मा। फिर सोचती हूँ बताऊँ कि न बताऊँ?
-बता न। क्या बात है?
घर के आदमी की शिकायत भी तो नहीं करते बनता।
-बुझौवल क्यों बुझाती है? साफ साफ बोल न।
-तीन चार दिन हुए, साँझ के झुटपुटे में मैने देवरानी और बितानू को बैलों की सरिया से मुस्कुराते हुए आगे पीछे निकलते देखा था।
-क्या कह रही है?
-हाँ अम्मा। आप की कसम। एक बार तो मुझे भी अपनी आँख पर यकीन नही हुआ। लेकिन इतना अँधेरा भी नहीं था कि पहचान न पाऊँ।
बूढ़ी ने मौन साध लिया।
-मेरी मानो तो इस आग के गोले को जितनी जल्दी हो सके, दफा करो। मैं तो हूँ ही सेवा टहल के लिए। मुझे परायी क्यों समझती हो?
-हूँ। एक लम्बी हुँकारी।
-पता नहीं देवरानी को उस नटुल्ले में मिल क्या रहा है? इतना सुन्दर लड़का मैने दिखाया था...
-तूने दिखाया था? कब?
-कई दिन हुए।
-कहाँ?
-यहीं घर पर। मेरे जीजा का भाई है। मैने तो कहा कि अम्मा को भी दिखा दे। आपको बताया भी नही?... यही कपट-खेला मुझे अच्छा नहीं लगता।
बूढ़ी से कुछ कहते नहीं बना।
बितानू की सूचना से तीनो प्राणियों के मन की खदबदाहट बढ़ गयी। बूढ़ी के बहुत दबाव डालने पर एक दिन बुढ़ऊ ने जमीन की चर्चा छेड़ी।
-कैसी जमीन? बनवारी बौखला गया।
-जिसे कालिका बनिया से दोनो भाई साझे में खरीदे हो।
-साझे में? कौन कहता है? मैने खरीदा है, तनहा।
-कागज में तो हनुमान की भी दसखत है।
-दसखत तो है लेकिन खरीदार के तौर पर नहीं। गवाह के तौर पर। फिर पूछा-किसने पढ़ाई ए पट्टी? बितनुआ ने तो नहीं? काला नाग है। ऐसी जगह डसेगा कि पानी भी नहीं मिलेगा।
-वह अपना बोरिंग का काम शुरु करना...
-हाँ हाँ, खूब कराओ बोरिंग। होंठ ऐठ गये बनवारी के - बढ़िया से कर देगा। इसीलिए रोज घर में घुसाये रहते हो?
लाख चाहने के बावजूद बनवारी अपनी तल्खी दबा नहीं सका। उसे यह भी लग गया कि प्यार मुहब्बत का दिखावा आगे काम नहीं आने वाला। सुलछनी का भी मानना है कि बूढ़ी के पेट से कोई बात निकाल पाना महा मुश्किल। कुछ पूछते ही गूंगी बन जाती है बुढ़िया।
-अच्छा ऐसा कर, अब जिस दिन वहाँ बितनुआ आये, उसे बहाने से घर के अंदर बुला। फिर आवाज देकर कुच्ची को भी बुला ले और बितनुआ की कमर पकड़ कर लटकते हुए चिल्लाना शुरु कर दे कि हरामजादे मेरा ही घर मिला तुझे घटियारी करने के लिए। घसीट सके तो चप्पल से पीटते चिल्लाते हुए उसे घर से बाहर घसीट ला। तब तक दस पाँच लोग इकट्ठे हो जायेंगे। उन्हें बता कि तूने देवरानी के संग उसे बदमाशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तू इतना कर दे तो आगे मै देख लूँगा। एक ही झटके में दोनो ‘खेत’ हो जायेंगे।
-झूठ बोलना पड़ेगा?
-झूठ सच क्या होता है? चार बीघे के लिए तो आदमी दिन दहाड़े सगे बाप को काट देता है।
लेकिन सुलछनी का इंतजार लम्बा होता जा रहा है। बितानू इधर दिखायी ही नहीं पड़ा।
बनवारी की निराशा बढ़ती जा रही है। लगता नहीं कि यह औरत यहां से जायेगी। इसका बाप भी पता नहीं कहां मर गया। वह इतना बेचैन हो गया है कि उसका हेल्पर नसीर उसे ब्लड प्रेशर जांच कराने की सलाह देने लगा है।
0
वह पिछवाड़े से ईधन लेकर लौटी तो देखा उसकी नाद पर बनवारी की भैस और पंड़िया बंधी थीं। यहाँ क्यो बांध गये? उसका मन किया तुरंत जाकर दोनो जानवरों को भगा दें, लेकिन गम खा गयी। जब सास ससुर मौजूद है तो उसका आगे बढ़कर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्या पता बूढे बूढ़ी को ही यह अच्छा न लगे।
मुश्किल से दस दिन हुए होंगे जब बनवारी ने साझे महुए की एक मोटी डाल काट ली थी। दोनो घरों के बीच महुए का वही एक पेड़ था जिससे हर साल डेढ़-दो मन महुआ मिल जाता था। भला कोई ऐसा फलदार पेड़ काटता है? वह भी बिना राय सलाह के। बूढ़ी ने बुढ़ऊ को ओरहन लेकर जाने के लिए कहा तो वे टाल मटोल करने लगे। बोले-मुँहफट आदमी है। कभी कभी पी भी लेता है। क्या पता क्या बोल दे? अपनी इज्जत अपने हाथ। झगड़ा बढ़ाने से कटी हुई डाल जुड़ तो जायेगी नहीं।
लेकिन कुच्ची का कहना था कि बात एक डाल की नहीं, अपने हक हिस्से के लिए खड़े होने की है। वह एक एक चीज हड़पता जा रहा है। टोंका नहीं गया तो मनबढ़ होता चला जायेगा। आम की पूरी बाग साझे में है। किसी दिन चुपके से बेंच देगा तो क्या होगा?
बुढ़ऊ नही गये तो बूढ़ी ने सुलछनी को बुलवाया। वह एक ही मिठबोलनी। बोली-गलती हो गयी अम्मा। नयी सरिया के लिए ‘धन्न’ की जरुरत थी। कोई और पेड़ था नहीं, इसलिए काट लिए। पूछा नहीं यही गलती कर दिए। पूछते तो क्या बुढ़ऊ मना कर देते? उनको भी अपनी गलती समझ में आ गयी है इसीलिए उस दिन के बाद आप लोगों के सामने पड़ने से बच रहे हैं।
चुप हो गयी बूढ़ी। गलती मान लिया तो अब क्या बोले?
लेकिन अब यह काँड। उसने आकर बूढ़ी को बताया। बुढऊ बाजार गये थें। लौटे तो बूढ़े-बूढ़ी में बहस होने लगी।
बुढ़ऊ उल्टे बनवारी की तरफदारी करने लगे- अपने बैलों की जगह तो खाली ही पड़ी है। जब तक उसकी सरिया पर छप्पर नहीं पड़ जाता तब तक मेरी सरिया में बाँध ले तो क्या हर्ज है?
-बाँधने से पहले आपसे पूछा?
-पूछा नहीं, यही तो बेजह किया।
-इसलिए नहीं पूछा कि उसे किसी का डर नहीं रह गया है? उसके मन में लालच का भूत समा गया है। जबरिया कब्जियाना चाहता है। धौंस से। अभी नहीं बोले तो एक दिन घर से निकाल देगा। आपके मुँह में जीभ नहीं है? इसी दम चलकर सरिया खाली करवाइये। हम दोनो भी पीछे पीछे आ रहे हैं।
बुढ़ऊ का मन नहीं था जाने का, लेकिन गये तो बात बढ़ती चली गयी।
-तुझे किसी का डर भय नहीं रह गया रे? क्या समझ कर मेरी सरिया कब्जियाने चला है।
-तुम बहरे तो थे ही, अन्धे भी हो गये क्या काका? देख नहीं रहे हो कि हमारी पुरानी सरिया किस हाल में है। एक भी फूस उस पर बचा है? नयी पर अभी छाजन नहीं पड़ी। हमारे जानवर माघ की इस ठंड में रात भर काँपते हैं। खाली पड़ी सरिया में बाँध दिया तो क्या गुनाह कर दिया?
-बाँधने से पहले पूछना नहीं चाहिए?
-इसमें पूछने की क्या बात है? किसी गैर के खूँटे पर बाँध दिए हैं क्या? हनुमान के बाद अब मेरा तेरा का क्या सवाल रह गया?
-क्यों हनुमान के साथ हम भी मर गये क्या? तुम्हारा रवैया हम शुरु से देख रहे हैं। पहले मोटरसाइकिल दबा के बैठ गये फिर आबादी की जमीन घेर ली। फिर महुए की डाल काट ली। अब सरिया कब्जिया रहे हो। कल को घर में घुस आओगे। क्या मतलब है इसका?
-अरे काका, जब खूँटा ही बूड़ गया तो आपके जीने मरने से कितना फरक पड़ जायेगा? जी लो दस पाँच साल, जब तक मन न भरे। उसके बाद तो सब मेरा ही है। कि नया खूँटा गाड़ने का इरादा है?
-तुम इतना अगाही सोच रहे हो बनवारी?
-अगाही मैं नहीं तुम सोच रहे हो काका। और समझते हो कि किसी को कुछ पता नही है। तुम्हारे मन में क्या पक रहा है यह मुझे ही नहीं, सारे गाॅव को पता है। नहीं तो किसके लिए तड़-तड़ पतोहू घर में बैठा कर पोस रहे हो? पड़ोसियों के लिए? लेकिन ईमान से बताना, उस नीलगाय जैसी औरत में तुम्हारा कुछ ओधता भी है? (असर भी करता है?)
दीवार की ओट लिए खड़ी कुच्ची के कान में मानो पिघला शीशा पड़ गया।
-अरे बेशरम। बुढ़ऊ चिल्लाये - लाज शरम सब घोल कर पी गया क्या रे?
लाज शरम की सोचते तो घर में ही डाका डालते। गाँव के बच्चे बच्चे को पता है। किसका किसका मुँह बंद करोगे? बेटा तो कुछ उखाड़ नहीं पाया। अब बाप चला है बाझिन से बेटा पैदा करने।
बाझिन! बाझिन। कुच्ची के कान में गोले दगे।
-लेकिन कान खोल कर सुन लो। ससुर पतोह छिनारा करोगे तो सारा गाॅव चुपचाप देखता नहीं रहेगा। मूँड़ मुड़ा कर मुँह में कालिख पोत कर, गदहे पर बैठा कर सारे इलाके में घुमाया जायेगा।
गुस्से में रमेसर की देंह से चिनगारी निकलने लगी। वे थोड़ी दूर पड़ा एक डंडा लेकर किचकिचाते हुए उसे मारने दौड़े। बनवारी ने डंडा छीन कर दूर फेंका और बुढ़ऊ को पटक कर लगा मुँह पर ताबड़तोड़ मुक्का जमाने। बुढ़ऊ चिल्लाये - मार डाला। बचाओ।
कुच्ची दौड़ते हुए पहुँची तो बनवारी बुढ़ऊ की छाती पर बैठा उनका गला दबा रहा था। बुढ़ऊ गों-गों करते छटपटा रहे थे। कुच्ची ने बगल से बनवारी के बायें कंधे पर एक लात हुमचा। बनवारी उलट गया। लेकिन उलटते उलटते उसके हाथ में कुच्ची की साड़ी आ गयी। उसने अपना सारा जोर साड़ी खींचने में लगा दिया। साड़ी सरसरा कर खुलने लगी। आधी साड़ी कुच्ची के हाथ में आधी बनवारी के। तब तक क्या करते हो, क्या करते हो, कहते हुए दोनो के बीच सुलछनी कूदी। उसने बनवारी के हाथ से साड़ी छीन कर कुच्ची के ऊपर फेका और बनवारी की बाँह पकड़कर घर की ओर घसीटने लगी।
सुलछनी की पकड़ से छूटना कितना मुश्किल? आधे झटके में छूट जाता। लेकिन वह खूद छुटना नहीं चाहता। एक ही लात खाकर वह दहल गया है। एक बार कुच्ची के भाई ने बताया था कि प्राइमरी स्कूल में यह लड़को से कुस्ती लड़ जाती थी। बिलकुल सही बताया था। इसलिए मुड़ मुड़ कर गाली देते हुए वह सुलछनी की गिरफ्त में चलता चला गया।
आसपास के लोग पहुँचने लगे तो कुच्ची साड़ी लपेटते हुए वहा से हट गयी। लोगों ने रमेसर को खड़ा किया। वे धूल धूसरित थे। मुँह से खून थूक रहे थे। उनके आगे वाले तीन दांत टूट गये थे। दो ऊपर के, एक नीचे का।
कुच्ची साड़ी ठीक करके लौटी और रमेसर को सहारा देते हुए घर की ओर ले चली। बुढ़ऊ ओसारे में पड़ी चारपायी पर भहरा पड़े। मेला लग गया। कुच्ची लोटे में गरम पानी लायी। बुढ़ऊ को बैठा कर कुल्ला कराया गया। कुच्ची ने अँगौछा गीला करके उनके चेहरे और देह की धूल माटी पोंछी फिर लेटा कर रजाई ओढ़ा दी गयी। वे आँख बंद करके कराहने लगे। लोग बनवारी की ज्यादती के लिए बुरा भला कहने लगे। पाटी पकड़ कर जमीन पर पैर फैलाये बैठी बुढ़िया लोगों की सहानुभूति पाकर रोने लगी। थोड़ी देर रोती फिर आँखो देखा हाल सुनाती-कितनी बेदर्दी से घूँसे मार रहा था। छाती पर चढ़ कर हुमच रहा था। भतीजा नही दुश्मन है। बहू न पहुँच जाती तो मार ही डालता।
अचानक कुच्ची को इस महाभारत की जड़ याद आयी। उसने नाद में बँधी बनवारी की भैंस और पंड़िया के पगहे खोले और दो दो डंडे मार कर सिंवार की ओर खदेड़ दिया।
लोग एक एक करके लौटने लगे। बुढ़ऊ का दर्द बढ़ गया। पीठ में धुस्स चोट लगी थी और कुहनियाँ छिल गयी थीं। कुच्ची कटोरी में हल्दी तेल गरम करके लायी और सास बहू रजाई के अंदर हाथ डाल कर बुढ़ऊ की मालिस करने लगी।
आधी रात होने को आयी। चारो तरफ सन्नाटा छा गया। बुढ़ऊ की कराह बन्द हो गयी। तब बूढ़ी ने बहू से कहा - जाकर चूल्हे पर चावल दाल चढ़ा दे।
बूढ़ी देर तक पाटी पर सिर टेक कर आँख मूँदे बैठी रही। बुढ़ऊ की देह में हलचल हुई तो कहा - तुम्हारी थाली यहीं भेजवा देती हूँ।
-तुम लोग खाओ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है।
-तुम नहीं खाओगे तो सभी उपवास करेंगे। आज का दिन उपवास करने का नहीं है।
-अब मै बहू को उसके मायके पहुँचा कर ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। उससे कहो सबेरे तैयार हो जाय। सारे झगड़े की जड़ खत्म हो जाय।
-क्या बकते हो? बूढ़ी गुस्से से फुफकारी - झगड़े की जड़ बहू है कि तुम्हारा वह कसाई भतीजा, जिसके मुँह में लगाम नहीं है। जो हमारी खेती बारी और घर दुवार पर ही नहीं बहू पर भी दाँत गड़ाये बैठा है। बहू तो इस घर में ब्याह कर आयी है। उसी का तो सब कुछ है। अभी उसे पहुँचा दोगे तो मुझे पकड़ कर जंगल तुम ले चलोगे? रोटी तुम सेकोगे? मेरे ठीक होने के बाद वह अपनी मरजी से जाना चाहेगी तो शौक से बेटी की तरह विदा करेंगे और रहना चाहेगी तो घर की मालकिन बना कर रखेंगें। उसे कौन निकाल सकता है? ऐसी बात मुंह से निकाली कैसे? कहां का गुस्सा कहां उतार रहेे हो? चीलर के डर से कोई कथरी फेंक देता है? उठो, हाथ मुंह धोओ।
बुढ़ऊ थोड़ी देर तक चुप रहे फिर बोले - खा नहीं पायेंगे। दाँतों में बहुत दर्द है। लगता है मुँह सूज रहा है।
-अच्छा धीरे धीरे एक गिलास ठंडा दूध पी लो। भेजवाती हूँ।
बुढ़ऊ के दूध पीने के बाद कुच्ची सास की थाली लेकर उनकी कोठरी में गयी तो बूढ़ी ने हाथ पकड़कर उसे भी बैठा लिया- आ, इसी में दोनों जनी खा लेते हैं।
खा कर दोनों एक ही चारपायी पर लेट गयीं। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। बहू थोड़ी देर तक सास से कुछ फुसफुसाती रही फिर उठी और दरवाजा खोल कर बाहर आ गयी। मंड़हे में ससुर रजाई ओढे़ बैठे थे। उनकी बीड़ी की लौ रह-रह कर तेज हो जाती थी।
-बाबू, उठिए।
-क्या हुआ?
-अंदर चलिए। आपकी चारपायी आज से दरवाजे के अंदर बिछाएंगे। जेठ के सिर पर लालच का भूत सवार है। आपका यहां खुले में अकेले सोना खतरे से खाली नहीं है।
ससुर ने उठने में आलस दिखाया तो बहू ने उनका हाथ पकड़ लिया -उठिए।
बुढ़ऊ को अंदर सुलाकर कुच्ची ने किवाड़ की कुंडी लगायी फिर अपनी कोठरी में जाने के बजाय सास की कोठरी में चली गयी। रजाई में घुस कर वह बूढ़ी के गले में बांह डालकर लेट गयी।
बूढ़ी हिचकियाँ लेते हुए बड़बड़ा रही थी- हम बूढे़-बूढ़ी कितने दिन के मेहमान हैं? हमारे बाद तो सब उसी का होना है। फिर भी उसको सबर नहीं है।
-वह आपके मरने का इंतजार नहीं करेगा अम्मा। मारने का इन्तजाम कर देगा। मैं ही हूं, उसके रास्ते का कांटा। मेरे जाते ही वह आप लोगों को लील लेगा।
बूढ़ी अंदर तक कांप गई। लेकिन प्रकट में कहा -लील लेगा, तो लील ले। जैसी भगवान की मरजी।
-लेकिन मैं उसे लीलने दूंगी तब न। सिंघी मछली बन कर उसके गले में अटक जाऊँगी। उसकी आँत में हाथ डाल कर अपनी जमीन निकालूँगी। अब मैं आप लोगों को छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाली। जैसे आप लोग ‘उनके’ मां बाप थे वैसे ही मेरे हैं। उस की आवाज क्रमशः ऊँची होती गयी- खबर करवा दीजिये मेरे बाप को कि अब कुचिया की जिन्दगी अपने सास ससुर की सेवा में कटेगी। करे जितनी बदनामी करना चाहे यह पापी।
-बूढ़ी ने बहू को खींचकर कलेजे से लगा लिया।
-तू नहीं जाना चाहेगी तो कोई तुझे जबरदस्ती थोडे़ भेज देगा बिटिया। हम जब तक जियेंगे तुझे पान के पत्ते की तरह फेरेंगे।.... लेकिन जवान देह का भी एक धरम होता है। ये दिन अकेले काटने से नहीं कटते।
सारे फल खाते हैं, अम्मा। एक फल नहीं खायेंगे तो क्या नहीं निभेगा?
कोठरी में सन्नाटा छा गया।
0
गांव की औरतों के बीच बस एक ही चर्चा- यह गर्भ वह लायी कहां से?
-मुझे तो लगता है, घर में ही खेला हुआ है। अपने बुढ़ऊ को जगाया होगा। एक बूढ़ी अनुमान लगाती है।
-बुढ़ऊ में अब क्या बचा होगा अइया? साठ पार कर गये हैं। एक बहू की शंका।
-साठ माने कुछ नहीं। बूढ़ी का प्रतिवाद- किसी दिन अपने बुढ़ऊ को आजमा कर देख तो पता चल जायेगा। मर्द-बर्द और घोड़े कभी बूढे़ नहीं होते। खोराकी मिलती रहे तो चाहे आखिरी दिन तक जोतो। हमारे मिठ्ठू के बप्पा को देख रही हो। हनुमान के बाप से साल दो साल बडे़ ही ठहरेंगे। लेकिन जहां महीना बीस दिन गुजरा कि लगते हैं काॅखने कराहने। क्या, तो कमर चिलक गयी है। क्या, तो नार उखड़ गया है। क्या, तो कपार दुख रहा है। दोपहर से ही छछन्द फैलाना शुरू करते हैं। घर की बहुएं जान जाती हंै। कि अम्मा के लिए बुलौवा आ गया। गरम तेल की कटोरी लेकर रात में बुढ़ऊ की मॅड़ई में जाना पडे़गा। सब मुंह में आंचल का टोंक दबाकर हंसती हैं। मजाक करती हैं- ए अम्मा! आप की गौने वाली साड़ी निकाल देते हैं। वही पहन कर जाइयेगा।
आम धारणा के अनुसार ‘बुढ़ऊ’ का मतलब सत्तर-अस्सी वर्ष का आदमी होता होगा लेकिन इस इलाके में इसका मतलब सचमुच इतना बूढ़ा हो, यह जरूरी नहीं। बेटे का गौना आते ही बहू से वार्ता करते हुए सास अपने पति को ‘बुढ़ऊ’ कहने लगती है, चाहे ‘बुढ़ऊ’ अभी पचास भी न पार किए हों। इसी कड़ी में वह खुद ‘बूढ़ी बूढ़ा’ ‘अइया’ या ‘अम्मा’ हो जाती है। लेकिन कहने से क्या। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सास बहू की जचगी एक साथ पड़ जाती है।
-मैं बहुओं से मुंह छिपाती फिरती हूं। लेकिन जाना तो पड़ता ही है। न जाऊं तो अगले दिन कोई न कोई बहाना निकाल कर वे घर भर को गरियाना शुरू कर देंगे। घर को उनके कोप से बचाने के लिए जाना पड़ता है।
-अच्छा! अपनी खुशी से नहीं जाती?
बूढ़ी के होंठों पर रोकते-रोकते भी क्षीण मुस्कान उभर आती है।
कुच्ची के गर्भ को लेकर औरतों में दो मत है। एक की राय में अगर उसे यही करना था तो इससे अच्छा था दूसरा खसम कर लेती। रमेसर भगत के मुंह पर कालिख पोतने की क्या जरूरत थी?
-यह तो होना ही था। जोड़ा तोप तान कर चलने लगी तभी मैंने कहा था कि जल्दी ही यह ‘बज्जर’ किसी न किसी पर गिरेगा।
‘बज्जर’ तो गिरा। सवाल है कि कौन है वह तकदीर का धनी जिस पर गिरा?
उनके बीच एक-एक नाम पेश होता है और खारिज हो जाता है।
किसी किसी ने अपने पति से जवाब तलबी कर डाली - कहीं तुम्हारा तो नहीं है? तुम्हारा सारा चाल चरित्तर मुझे पता है।
कुछ का कहना है कि रांड़ तो अपना रँडापा काट ले लेकिन शोहदों छिनरों के मारे काटने पाये तब न। औरत जात कब तक जान बचायेगी।
-घर में, पर्दे में रहना हो तो बच भी जाय। खेती-बारी के काम में टैम कुटैम निकलना ही पडे़गा।
-जो पर्दे में रहती हैं, वही कहां बच पाती हैं। एक बहू कहती है- मेरे मायके में एक बड़ी बखरी की बहू गौने के बाद ही विधवा हो गयी। दूसरा विवाह उसके यहां होता नहीं था। विधवा होने के चैथे-पांचवे महीने खबर फैली की बहू तप करने बैठ गयी है। एकान्त तप। अब सूरज की किरण भी उसे न देख पायेगी। बहुत बड़ा घर था। बहुत बड़ा हाता। फुलवारी। कभी बाहर नहीं निकली। कभी किसी के सामने नहीं पड़ी। दिशा मैदान का इन्तजाम भी हाते के अंदर कर दिया गया। घोर तपस्या। ताकि अगले जनम में विधवा का दुर्भाग्य न झेलना पड़े। चैदह साल तपस्या किया। एक दिन खबर फैली कि तपस्या में बैठे-बैठे ही उसका स्वर्गवास हो गया। वहीं हाते में उसे समाधि दे दी गयी। कई साल बाद गांव का वह घर बेच कर अगली पीढ़ी ने पक्की सड़क के किनारे घर बनवा लिया। गांव के जिस पड़ोसी ने उस घर को खरीदा उसने उसे गिरा कर पक्का घर बनवाना शुरू किया। नीव खोदी जाने लगी तो तपस्या वाली कोठरी के फर्श के नीचे से सात नन्हें-नन्हें बच्चों के कंकाल निकले। चौदह साल की तपस्या का फल। सात बच्चे।
बूढ़ी कहती है- यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहां क्या नहीं होता? सब अपनी गरज और दशा से निपटने रास्ता खोज लेते हैं। बगल के गांव के मथुरा का नाम तो तुम सबने सुना होगा। पांच छः साल पहले ही तो मरे हैं। जब मैं व्याह कर पहली बार इस गांव में आयी तो औरतों के बीच मथुरा को लेकर बहुत हंसी मजाक चलता था। चालीस पचास साल तो हो ही गये होंगे। उस जमाने में जिस औरत को गौने के तीन चार साल तक बच्चा नहीं होता था। उसके घर में चिन्ता व्याप जाती थी। डाक्टरी का जमाना तो था नहीं। ओझायी-बैदायी और टोना-टोटका शुरू हो जाता था। पदी हदी औरतें मजाक करने लगती थीं कि लगता है अब इसको मथुरा की चैरी पर ले जाना पड़ेगा। मथुरा ओझायी करते थे। भूत-प्रेत झाड़ते थे। भूत ग्रस्त औरतें दूर-दूर से आकर उनकी चैरी पर अभुवाती रहती थीं। लेकिन असली शोहरत इस बात की थी कि उनका हथियार बहुत बड़ा और अमोघ है। उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। पोते का मुंह देखने को आतुर सासें या ऐसी माताएं जिनकी बेटी बाॅझ का ताना सुनते-सुनते आत्महत्या करने की सोचने लगती थी या जिसका पति दूसरी शादी करने की सोचने लगता था, मथुरा की शरण में आती थीं। ज्यादातर दूर के मामले, ताकि पहचान छिपी रहे। खासकर ऐसे घरों के मामले जहां औरतों की चलती थी। एकाध ऐसे मामले भी जहां कोई संतान का मुंह देखने के लिए बुढ़ापे में शादी करता था लेकिन संतान का इन्तजार लम्बा होता जाता था।
-इलाहाबाद मे पढ़ने वाले गांव के लड़कों ने मथुरा का नाम ‘महालिंगम’ रख दिया था। बहुत दिनों तक कोई इसका मतलब ही नहीं समझ पाया।
-क्या होता है इसका मतलब अइया?
-इसका मतलब, अपने भतार से पूछना। फिर कहती हैं- जाने कितने खानदानों को मथुरा ने निरवंस होने से बचाया। कितनी औरतों का घर उजड़ने से बचाया। फरक इतना है कि उन औरतों के सिर पर उनके मरदों की छाॅव थी, कुच्ची के सिर पर किसी मरद की छाॅव नहीं है।
-किसी का तो होगा? जिसका होगा वही छाॅव करेगा।
-पेट देखने से तो लगता है कि पूस में होगा। इस हिसाब से चैत का है। चैत में कटिया बिनिया के चलते घर के बाहर आना जाना बढ़ जाता है। मनई मजूर से वास्ता पड़ता है।
-कौन ऐसा मनई मजूर है जिसका आना जाना ज्यादा रहा हो?
-छोड़िए अम्मा। यह बताइये कि आप को भी कभी मौका मिला मथुरा के पास जाने का? एक तेजतर्रार बहू सवाल दागती है।
टोली में खिलखिलाहट गूंजने लगती है।
बूढ़ी मुस्कराती है- कहाॅ रे! मेरी पहिलौठी बिटिया तो साल भर के अंदर ही पेट में आ गयी थी।
0
कुच्ची की सास के पास तो इस ‘आग’ की खबर पहुंच गयी लेकिन सुलछनी के पास पहुँचने से औरतें अभी तक बचाए हुए हैं। सबको पता है कि कुच्ची बनवारी की आंख की किरकिरी है। खबर पाते ही वह अगिया बैताल हो जायेगा।
कुच्ची की सास की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह बहू से कुछ पूछे। दो साल में बहू ने घर-गृहस्थी का काम पूरी तरह संभाल लिया है। खेती बारी, बाजार हाट, लेना देना, धरना उठाना, सब कुछ। बनवारी आये दिन कोई न कोई टंटा खड़ा करता है और बहू उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। बूढे़ बूढ़ी का दाना-पानी और गाय भैंस का चारा चोकर ‘टैम- पर। रमेसर अपने मन से जो करना चाहे करें वरना सुबह शाम चैराहे जाकर चाह पिये। सास से कहती- बुढ़ऊ को बहुत संभाल कर रखना होगा अम्मा। इन्हीं की छाॅव में हम गाॅव में टिके रह पायेंगे। अपनी सेवा देखकर रमेसर की आंखों में पानी आ जाता। बहू की चढं़ती की देंह उनसे भर आंख देखी नहीं जाती। नजर हटा लेते। रान्ह परोस की औरतें सिहातीं- अब किस आस में यह बावली हुई जा रही है?
बहू को आगे रखने में ही सास को भी भलाई दिखती थी। तभी तो यहां उसका मन लगेगा। वह न रूकी होती तो वे दोनों प्राणी चार छः साल से ज्यादा के मेहमान न होते। कहो, रात बिरात बनवरिया ही गला दबाकर पार लगा देता।
लेकिन इस खबर से वे बेचैन हो गयीं। उन्हें याद पड़ता है, लगभग डेढ़ साल होने वाले हैं, पिछली से पिछली होली के दिन बहू ने उनसे यह बात कही थी। उस दिन खलिहान के बंटवारे को लेकर बनवारी से झगड़ा हुआ था। बहू लपककर आगे न आ जाती तो बनवारी के डंडे का वार बुढ़ऊ का सिर फोड़ देता। बनवारी के हाथ से डंडा छीनने से पहले बहू ने उसके तीन वार अपनी हथेली पर रोपे थे। दाहिने हाथ की दो उँगलियों के बीच का माँस फट गया था। टाँके लगवाने पड़े थे।
उस रात उनके आँचल से मुँह ढक कर लेटी बहू ने कहा था - मैने अपने मन को बहुत रोका अम्मा, नही ंतो उसी डंडे से जेठ की पीठ लाल कर देती।
अपने यहाँ कोई भिड़ने वाला नहीं है बिटिया इसीलिए बाघ बना हुआ है।
थोड़ी देर तक बिसूरने के बाद रंज डूबी आवाज में कहा था बहू ने - ए अम्मा! मन करता है एक, दो बेटे पैदा कर डालूं जो बडे़ होकर इसके ‘उसमें’ डंडा डाले।
बूढ़ी चोट खायी बहू के मन के उबाल को समझ रही थी। शान्त स्वर में समझाया था- यही काम तो औरत नहीं कर सकती बिटिया।
-औरत ही तो कर सकती है अम्मा। मर्द थोडे़ कर सकता है।
-ऐसा मत कर डालना मेरी बच्ची। गाँव रहने नहीं देगा। बनवरिया जीने नहीं देगा।
-अभी कहाँ जीने दे रहा है अम्मा। इसीलिए तो जरूरी है।
-जरूरी तो बहुत है बिटिया लेकिन क्या कर सकते हैं। हमारा ‘टैम’ निकल गया।
-मेरा टैम निकल गया अम्मा। अभी तुम्हारा नहीं निकला। तुम्हीं पैदा करो।
बूढ़ी करूणा, दुःख और शर्म के मिले-जुले भावों में डूब गयी थी। आँचल हटाकर बहू का गाल चूम लिया था। गाल पर आंसुओं का खारा स्वाद था।
लेकिन इसने तो सचमुच कर डाला। खाने पीने के बाद रात में वे जाकर बहू के बगल में लेटती हैं। आसमान में बादल गरज रहे हैं। थोड़ी देर तक उसका पेट सहलाने के बाद फुस फुसाती है- इसमें कुछ है क्या रे?
-हां अम्मा।
-बिजली कड़कती है। क्षणभर के प्रकाश में वह देखती है, उतान लेटी बहू की आंखे बंद हैं। बूढ़ी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिसलता हुआ हाथ रूक जाता है।
-क्या जवाब देंगे रे?
-जवाब कौन मांगेगा अम्मा?
-अरे, गांव देश। टोला परोस।
-गांव देश हमारी हर्ज गर्ज, आफत विपत में आज तक कभी आया है कि जवाब मांगने ही आयेगा?
लम्बी चुप्पी। बाहर छकछका कर पानी बरसने लगा है। लगता है बहू सो गयी। बूढ़ी से लेटा नहीं जाता। बरसात शायद धीमी हुई है। वह अंधरे में दबे पांव दरवाजे में सोये बुढ़ऊ की चारपायी तक आती है। खर्राटा ले रहे बुढ़ऊ को पाटी पर बैठकर हिलाती है- सुनते हो।
-कौन?
-बहू तो पेट से है।
-ऐं! वे चैक कर बैठ जाते हैं।
-हां। चार पांच महीने से कम का न होगा। सारे गांव में खबर है।
-किसका है?
-पता नहीं।
-तूने पूछा नहीं?
-सोचा, पहले तुम्ही से पूंछ लूं।
-मैं क्या बताऊंगा। रात दिन तो साथ में तू रहती है। तुझे तो पता होगा कि कौन आता जाता था।
-घर में भला कौन आयेगा?
-तब?
-तब क्या! बूढ़ी बगल में लेटने की जगह बनाते हुए पूछती है- कहीं तुम्हारा ही तो नहीं है?
-पागल हो गयी है क्या? बहू के साथ मेरा नाम जोड़ते शर्म नहीं आती।
-जरा मेरी ओर मुंह करके बोलिए। बूढ़ी ने बुढ़ऊ का मुंह अपनी ओर घुमाते हुए कहा- तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अभी इतने बूढे़ भी नहीं हुए कि...
-चुप कर। बचने की राह खोज। ले जाकर कहीं गिरवा दे।
-वह गिरवायेगी नहीं।
-क्यों?... पूछा?
-क्या पूछंू। मैं जानती हूं।
बूढ़ी ने खलिहान के झगड़े वाली रात में कही हुई बहू की बात बतायी फिर जोड़ा- इसके अलावा, पांच महीने का बच्चा अगर जायेगा तो मां को साथ लेकर जायेगा।
-क्या?
-और क्या। इतना खून खच्चर होगा।
-तो दोनों जांय। गरह कटे।
भोर में जब सास अपनी चारपायी पर लौटी तो वहां बहू आड़ी तिरछी लेटी हुई मिली।
-क्या कहा बुढ़ऊ ने अम्मा?
-बुढ़ऊ क्या कहेंगे?
-बिगड़ तो नहीं रहे थे?
-बिगड़ कर क्या कर लेंगे? जो बिगड़ना था बिगड़ चुका।
-बिगड़ा नहीं अम्मा। बना है।
थोड़ी देर तक चुप्पी, फिर बूढ़ी बहू का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लेकर पूछती है- जिसका है उसके साथ निकल तो नहीं जायेगी?
0
लगी तो पहले भी थी गांव में ऐसी आग। एक नहीं कई बार। लेकिन उन्हें समय रहते बुझा दिया जाता था। यह तो डंके की चोट पर कह रही है कि पैदा करूंगी।
बनवारी खुश है। इस बार ऐसा पेंच फंसा है कि या तो रमेसर इस कुलच्छनी को घर से निकालेंगे या सारा गांव मिल कर उसके साथ रमेशर दोनों परानी को गांव से बाहर भगाएगा। कौन चाहेगा कि इसके चलते सारे गांव की बदनामी हो। इस औरत को कौन जानता है। बदनामी तो गांव की होगी।
दोनों घरों के बीच में बोलचाल, आवाजाही बंद है। सुलछनी और कुच्ची ने एक दूसरे को अपने दुआर पर न आने की कसम दे रखी है। सयाने कहते हैं कि उसे रमेशर से बिगाड़ नहीं करना चाहिए था। काका-काकी कहकर बूढ़े-बुढ़िया के पैर छूता रहता और कुच्ची के खिलाफ दोनों के कान भरता रहता तो सब कुछ हासिल हो जाता। सब कुछ माने सबकुछ। लेकिन चूक हो गयी। इस बार वह अकल से काम लेगा। खुद सामने नहीं आयेगा। पूरे गांव को मुकाबले में खड़ा कर देगा।
0
शायद बनवरी ने कुच्ची के मायके तक खबर पहुंचा दी। उसका छोटा भाई मिलने आया है। रमेसर कहीं निकले है। कुच्ची की सास ओसारे में चारपायी पर दरी बिछा कर उसे बैठाती है। एक कटोरे में दही गुड़ और लोटे में पानी लाकर देती है। फिर भीतर जाकर चूल्हे में रोटी सेंकती बहू को खबर करती है। कुच्ची फूला हुआ पेट लेकर सामने आने में सकुचा रही है। किंवाड़ की आड़ से हालचाल पूछती है।
-बहुत दिनों बाद खबर लेने आये भइया। माई से कहना मेरी जान सूली पर टंगी है। उनसे मिलने को मन बहुत हुड़कता है।
-भाई आंख नहीं मिलाता। शून्य में देखते हुये कहता है- माई ने कहलाया है कि कुचिया अब मायके लौटने की न सोचे। वह मेरे लेखे मर गयी।
-वह सिहर जाती है।
-माई ने कहलाया है कि बड़की भाभी ने?
-दोनो ने।
-और बप्पा ने क्या कहलाया है?
-बप्पा को कुछ पता नहीं है।
-और तुम क्या कहते हो?
भाई, जिसको उसने गोद में खेलाया है, चुप रह जाता है।
-तुम भी अपने मन की बात कह दो दीपू।
भाई खड़ा हो जाता है।
-पानी तो पी लो बबुआ। सास कहती है।
-माई ने मेरे घर का पानी पीने से भी मना किया है... क्या?
भाई सिर झुका कर बाहर निकल जाता है।
वह किंवाड़ की आड़ से बाहर आते हुए कहती है- जाकर माई से कहना, मैं उनके घर की ओर मुंह करके रोऊंगी भी नहीं।
0
जहां जो मिलता है बनवारी उससे कुच्ची की करतूत का बखान शुरू कर देता है। जो लोग नौकरी करने, वकालत मुंशियाना करने या राजगीरी दिहाड़ी कमाने शहर जाते हैं उनके पास कहाँ फुरसत है बात सुनने की। जो सुनते हैं वे भी हंस देते हैं- हमसे क्या मतलब?
-एतराज हो तो रमेशर दोनों परानी को हो। तुम्हे इतनी बेचैनी क्यों है?
-बोरिंग का काम मंदा पड़ गया क्या मिस्त्री, जो दूसरे के फटे में टांग फंसाने निकल पडे़?
-आदमी अपनी बहू बेटी संभाल ले यही बहुत है। पूरे गांव को संभालने का ठेका कौन ले सकता है?
उसी में कोई चढ़ा देता - जब इतना ही दिल पर ले लिया था तो गाॅव भर में रांड़ रोवन करने की क्या जरुरत थी? एक रात बाहर से जंजीर चढ़ाकर फूँक दिया होता। घर के अंदर ही सब स्वाहा हो जाते और कोई जान भी न पाता।
कुछ लोग मजा लेते हैं- नाक तो सचमुच कट गयी तुम्हारे खानदान की बनवारी। इससे तो अच्छा था कि तुम्ही कुछ कर गुजरे होते।
हां, बूढे़ पुरानों की नजर में जरूर यह गम्भीर मामला है- इसने तो पूरे गाॅव की बहू बेटियों के बिगड़ने का रास्ता खोल दिया। वे पूरी बात रस लेकर सुनते हैं, पूछताछ करते हैं, बच्चे के बाप का अनुमान लगाते हैं और पंचायत में पहुंचने का वादा करते हैं।
वैसे ‘विलेज बैरिस्टर’ तो इस गांव में नहीं हैं जो लोगों को मुकदमे में फंसाते हैं और थाना तहसील, ब्लाक या अस्पताल की दलाली करते हैं लेकिन तीन-चार मातबर ऐसे हैं जिनकी आंख, कान से आज तक गांव देखता सुनता रहा है। उनमे भी धन्नू उर्फ धनई बाबा माने धनराज मिसिर और बलई बाबा माने बलराज पांडे खास हैं। उस साल बलई बाबा के सबमर्सिबल ने पानी छोड़ दिया था तो नयी बोरिंग का काम रोक कर उसने एक लेंथ पाइप अपने पैसे से खरीद कर डाला था। लेकिन ‘लेबर चार्ज’ की कौन कहे, अभी तक पाइप का दाम भी नहीं दिया। उसने मन ही मन तय किया था कि फिर अंटकेगी तो बताऊंगा।... लेकिन अब वह सारा घाटा-उधारी भुला देगा। पांडे बाबा को सारे वेद पुरान जबानी याद हैं। जिसकी ओर खडे़ हो गये उसकी विजय पक्की। उन्हें किसी भी कीमत पर अपने पाल्हे में रखना है। कोशिश तो वह धन्नू बाबा को भी पटाने की करेगा। धन्नू बाबा बिना पढे़ लिखे बडे़-बड़े वकीलों के कान काटते हैं। मुश्किल यह है कि ए दोनों बाभन कभी एक पाल्हेे में नहीं खडे़ हो सकते। एक तीर घाट रहेगा तो दूसरा मीर घाट।
हल्ला है कि बनवारी ने बलई बाबा को पटा लिया। पूछने पर तम्बाकू से काले दांतो को निपोर कर हंसता है- राम नेवाज मुंशी कहते थे कि जो चमडे़ के जूते से न माने उसे चांदी के जूते से मनाओ। चांदी के जूते से तो बडे़-बडे़ जज वालिस्टर मुठ्ठी में आ जाते हैं। बलई किस खेते की मूली हैं। फिर जीभ को दांत से काट कर पलटता है- सवाल यह है कि मुझे यह सब करने की जरूरत क्या है? जिसको जरूरत हो वह पटाये।
- सुनते हैं तुमने बचन दिया है कि जब तक जिओगे, उनके ट्यूबवेल की मरम्मत फिरी में करते रहोगे।
- वह तो मैं अब भी करता हूं। गांव में किसी से कभी मुंह खोल कर पैसा मांगा? जिसने जो दे दिया बिना गिने पाकेट में डाल लेता हूं। फिर जाते-जाते कहता है- न अफवाह सुनो न अफवाह फैलाओ। गांव की इज्जत बचाओ।
बलई बाबा की सलाह से ही वह लछिमन चैधरी के घर के चक्कर लगा रहा है। लछिमन उसकी विरादरी के चैधरी हैं। सामने के गांव में उनका घर है। पंचायत का फैसला लागू करवाने में उनका दबदबा काम आयेगा।
अपने दुआर पर नीम के नीचे चैकी पर बैठे हथेली पर सुर्ती ठोंक रहे लछिमन चैधरी के आगे वह हाथ जोड़ कर कहता है- इस घोड़ी को गांव से भगाने का फैसला कर दो, चैधरी। मेरे खानदान की इज्जत बच जाय। मुर्रा पड़िया दरवाजे पर बांध जाऊंगा।
पुराने घाघ हैं लछिमन। जाने कितनों का बसा घर उजाड़ा और उजड़ा घर बसाया है। सुर्ती फांक कर मुंह बंद कर लेते हैं। आवाज तो निकलती है लेकिन कहीं और से। एक बार आगे पीछे सिर हिला देते हैं।
गांव की खुसर-फुसर से अनजान नहीं है कुच्ची। उसे लग रहा है कि उसने भारी जोखिम उठा लिया। कुट्टी नर्स के लिए शहर में रह कर ऐसा करना आसान था लेकिन उसके लिए गांव में रहकर...। यह लड़ाई उसे अकेले दम पर लड़ना है। घर के अंदर भी और बाहर भी। बुढ़ऊ मुंह दुब्बर हैं। गांव के मुकाबले खुलकर उसके साथ खड़े हों इसकी उम्मीद कम है। अम्मा जरूर मन से उसके साथ हैं लेकिन औरत जात, पचों के सामने कितना मुंह खोल पायेंगी।
शाम के धुंधलके में वह धन्नू बाबा के घर जाती है। दलान और ओसारे के बीच में एक छोटी खांची पलट कर उस पर लालटेन रखी गयी है जिसकी आधी रोशनी दालान में और आधी ओसारे में बने चूल्हे तक पहुंच रही है। बाबा दालान में ‘संध्या’ करने बैठे हैं। मिसराइन अइया ओसारे के चूल्हे में आग सुलगा रहीं हैं। कोई आल-औलाद न होने के चलते इस उमर में भी खुद ही चूल्हा फंूकना पड़ता है। वह पास जाकर पैलगी करती है। अइया घूमकर उसे भर नजर देखती हैं फिर पूछती हैं- कौन सा असिरबाद (आशीर्वाद) दें रे? कि पांच पसेरी का बेटवा हो? फिर पास आते हुए कहती हैं- तैं ई का करि डारे? (तूने यह क्या कर डाला?)
-अब तो करि डारे अम्मा। कहती हुई कुच्ची चूल्हे के पास जाती है और फंूक मार कर आग जला देती है। लपट से उसका चेहरा लाल-पीला होने लगता है।
कुच्ची जानती है कि बाबा उसे मानते हैं। जहां मिलते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं। बहुत पहले एक बार वह सास के साथ खेत से लौट रही थी तो रास्ते में मिल गये। वे जंगल से आम की एक हरी डाल घसीटते हुए आ रहे थे। डाल आंधी से टूट कर गिर गई थी। गांव की औरतों को राशन से ज्यादा चिन्ता जलावन की रहती है। डाल भारी थी। बाबा उसे खींचते-खींचते हांफ गये थे। लेकिन राह में छोड़ भी नहीं सकते थे। कोई उठा ले जाता। कुच्ची के सिर पर घास की खांची थी। खांची उसने सास के सिर पर रखा और डाल को एक झटके में उठा कर अपने कंधे पर रख लिया। लाकर सीधे बाबा के दुआर पर गिराया। पीछे-पीछे आते बाबा रास्ते भर उसे असीसते रहे। उसके बल और स्वभाव की तारीफ करते रहे।
एक बार कार्तिक एकादशी पूजने के लिए सास ने उसके हाथ से पांच गन्ने भेजवाये। किवाड़ खटखटाने पर बाबा ने आंगन से पूछा- कौन?
-मैं, कुच्ची!
बाबा बाहर आये और हंसते हुए पूछा- यह बता, कुच्ची तेरा बचपन का नाम है कि कुचवती होने के बाद पड़ा?
कुच्ची ने सुन रखा था कि बाबा जितने ज्ञानी हैं उतने ही मजाकिया। बारात जाते हैं तो ‘शास्त्रार्थ में ऐसी ‘कटबइठी’ पूछते हैं कि बडे़-बड़े पंडितों को जवाब नहीं सूझता। जरूर कोई गहरी बात पूछे रहे हैं। उसने हाथ जोड़ कर माथे से लगाते हुए कहा- हम आपकी ‘अंगरेजी’ नहीं समझे बाबा।
बाबा हंसे- जिस दिन समझ जायेगी मन से महारानी बन जायेगी।
महारानी तो अब वह क्या बनेगी, बस घर से बाहर न कर दी जाय। बाबा चाहेंगे तो उसके टिके रहने की राह निकाल देंगे।
कुच्ची इस गांव की शान है। शास्त्रों में लिखे पैमाने के अनुसार गढे़ गये हैं उसके अंग-प्रत्यंग। मोहिनी का अवतार। ऐसी लम्बी चैड़ी चिकनी चमकती जवान जनाना का शिकार कर लेना चाहता है लकड़बघ्घे जैसी खीस वाला यह बनवारी, जिसका मुंह दूर से बदबू करता है। इसको ‘बेज्जत’ करके तो सारा गांव ‘बेज्जत’ हो जायेगा। निःसंतान विधवा को देख कर बाबा को उतना ही दुःख होता है जितना सोलह आने मालियत वाले खेत को परती पड़ा देखकर होता है।
बाबा उसका मन टटोलते हैं - अगर तू अपने ससुर का नाम लगा दे तो सारी तकरार ही खतम हो जाय।
-लेकिन मै झूठ नहीं बोलना चाहती बाबा। सही बात यह है कि मुझे बच्चे की तलब लगी, जरुरत लगी और मैने कहीं से इंतजाम कर लिया। मैं अपनी बात पर ही कायम रहना चाहती हूँ।
-कोई बात नहीं। तू पहली औरत थोड़े है जो इस तरह मां बनी है। जब से यह दुनिया बनी है, ऐसे अनगिनत बच्चे पैदा होते रहे हैं। एक से बढ़कर एक प्रतापी, एक से बढ़कर एक महारथी। बाबा ने उसे कर्ण हनुमान, सीता, पांचो पोडवों आदि की पैदाइश के किस्से सुनाते हुए कहा कि तू पहली औरत है जो कह रही है कि अपनी जरूरत से पैदा कर रही हूं। ऐसा सोलह आने का सच कौन बोल पाया है आज तक?
वह तीन दिन बाबा के पास गयी और तीन लोक का ज्ञान लेकर लौटी। वह तो डरी हुई थी कि बाबा डाट कर भगा न दें।
बाबा से मिले सहारे से उसे सुघरा ठकुराइन के पास जाने की हिम्मत पड़ी। सुघरा एक बेटी को जन्म देकर विधवा हो गयीं। जेठ ने कहा- विधवा का विवाह तो इस खानदान में संभव नहीं लेकिन भाई मरा है, मैं तो अभी जिंदा हूं। तुम इस घर की मालकिन बनकर रहो। उन्होंने घर की चाभी सुघरा को सौंप दी और बाल मुंडवा दिए। बाल क्यों मुड़वा दिये? तो बोले- मेरा बड़ा बेटा जवान होने वाला है, इसलिये। सुघरा ने बेदाग निभाया। अपनी बेटी और जेठानी के बच्चों में कोई भेद नहीं किया। जेठानी का छोटा बेटा पप्पू तो पैदा होने के दिन से उन्हीं की गोद में पला। उन्हीं का दूध पीकर बड़ा हुआ। उसके मुंह लगाने से सुघरा के स्तनों में दूध उतर आया, जबकि उनकी बेटी तब चार साल की हो चुकी थी।
लेकिन जेठ के मरने के साल भर बाद वही पप्पू दबाव बनाने लगा कि अपने हिस्से का चक उसके नाम लिख दें। सुघरा ने लाख कहा कि तुम्हीं को तो मैंने बेटा माना है। तुम्हारा ही तो सब कुछ है। दूसरा कौन है लेने वाला? एक बेटी थी जिसका व्याह कर विदा किये चैदह साल बीत गये हैं। लेकिन पप्पू मानने को तैयार न था। लोगों ने उसे डराया होगा कि मोह में पड़ कर बेटी-दामाद को लिख देंगी तो तुम्हारी हैसियत आधी से घटकर चैथाई रह जायेगी। सुघरा ने भी साफ कह दिया कि जीते जी अपना हाथ नहीं कटा सकती। जो मेरा है वह मरने के दिन तक मेरा रहेगा।
पप्पू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जाति-बिरादरी के लोग बीच-बचाव करने आये तो साफ कह दिया- पिताजी की बात पिताजी के साथ गयी। पिताजी को इन्होंने क्या बूटी पिलाई कि मेरी मां के रहते उन्होंने इनको घर की चाभी सौंपी, इसे ए जाने या पिताजी जाने। घर में बचा क्या है धन्नि बडे़र के अलावा? सब तो चोरी छिपे बेटी-दामाद के घर जाता रहा। सबके समझाने-बुझाने के बावजूद उसने सुघरा को चक पर कब्जा नहीं दिया। गुजारे के लिए दो बीघा खेत और रहने के लिए दालान का एक हिस्सा देने को राजी हुआ। इसके बाद भी उन्हें तंग करने का कोई न कोई तरीका निकाल लेता। वे अपनी कोठरी बंद करके कहीं जातीं तो ताला तोड़ कर आटा, चावल गायब कर देता।
आखिर सुघरा मुकाबले के लिए खड़ी हुईं। खेत पर ससुर ने ही दोनों भाइयों का नाम चढ़वा दिया था। चकबन्दी में दोनों भाइयों के अलग-अलग चक कट गये थे। कब्जा भर लेना था। लेकिन यह भी आसान नहीं था। उन्हें लगता था कि पप्पू किसी रात गुस्से में आकर उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखायी। मदद के लिए बेटी दामाद को बुलाया। दो ढाई साल तक थाना कचेहरी का चक्कर लगातीं रहीं और चक पर कब्जा लेकर मानी। दो साल पहले तक गांव की परधान थीं। बातचीत में किसी को सेटती नहीं। खरी-खरी कहने के लिए बदनाम हैं।
सुधरा बोलीं- देख भाई, सास-ससुर की लाठी बन कर रहने के लिए दूसरा घर नहीं किया, इसे आज के जमाने में समझदारी का काम नहीं कहेंगे। हां, पीठ ठोंकने का काम जरूर है। अब गैर से गर्भ ले आयी। यह तो एकदम नया चलन है। लेकिन तू बुलाने आयी है, तो पंचायत में आऊंगी और जो सही लगेगा, बोलूंगी।
0
बनवारी ने दौड़ धूप कर आधे गांव को पंचायत में आने के लिए राजी कर लिया। अभी क्वार लगा ही है। धान की फसल पक रही है। जानवरों को चारा-पानी देने और दुधारूओं को सुबह-शाम दुहने के अलावा कोई काम नहीं। आधे घरों के खूंटे पर तो कोई जानवर ही नहीं। पंचायत के लिए इससे ज्यादा फुरसत का समय और कब मिलेगा? आठ दस दिन से पानी नहीं बरसा। जमीन सूखी चट्ट है। मिठौवा महुए के नीचे उगी हाथ-हाथ भर की घास पीली पड़ने लगी है। बैठने के लिए टाट जाजिम तक की दरकार नहीं। कुछ दूर तक मिठौवा की तीन जडे़ जमीन के ऊपर उठ कर तीन दिशाओं में जाकर अंदर धंसी हैं। बैठने के अलावा इन पर पीठ भी टिका सकते हैं। धन्नू बाबा और बलई बाबा के लिए बनवारी चारपायी लाया है। बीच में दस पन्द्रह हाथ की जगह छोड़ कर इसके पूरब बलई बाबा बैठे हैं और पश्चिम तरफ धन्नू बाबा। लछिमन चैधरी के लिए तखत का इन्तजाम है। वे उत्तर तरफ बैठे हैं। सुघरा ठकुराइन का नौकर उनके लिए खटोला लेकर आता है। वे महुए के तने के साथ खटोला सटाकर बैठती हैं- बलई और लछिमन चैधरी के बीच में। बनवारी, रमेशर उनकी बूढ़ी और कुच्ची, सुलछनी वगैहर दक्षिण तरफ बैठे हैं, उत्तर मुंह करके। आने वाले लोग इन्हीं लोगों के पीछे चारों तरफ बैठ रहे हैं। सबको बनवारी ने ही बुलाया है। रमेशर किसी को बुलाने नहीं गये। लछिमन चैधरी का संदेश मिला तो दोनों प्राणी पतोहू को लेकर हाजिर हो गये। रमेसर दोनों प्राणियों का चेहरा चूहेदानी में फंसे चूहे जैसा निरीह लग रहा है।
छिनारा की पंचायत तो गोपियों की रासलीला वाली कथा से भी ज्यादा ‘रसदार’ होती है। इसलिए घर का कामकाज जल्दी-जल्दी निबटाकर औरतों का झंुड उमड़ता चला आ रहा है। सास-बहू, बूढ़ी-जवान सभी। बेटियों और बहनों को छोड़कर। गोद में, साथ में बच्चे। उनके हाथ में दालभात या मैगी की कटोरी, बहुएं घूंघट में हैं तो क्या। बोलने की हिम्मत न सहीं, सुनने से कौन रोक लेगा? नये-नये जवान हो रहे लड़के भी शरमाते और एक दूसरे की आड़ में मुंह छिपाते चले आ रहे हैं।
औरतों, बच्चों का एक झुंड बनवारी के पीछे कुंए की जगत पर जमा है। गांवभर में यही अकेला कुंआ है जो जीवित है। पप्पू मौर्या ने इसके पेंदे में जमा गाद की सफाई कराकर, इसमें एक पम्पिंग सेट फिट कर दिया है। इसी से अपनी सब्जी की सिंचाई करते हैं। जगत के बगल में सीमेंट की एक छोटी टंकी बनाकर टोंटी लगा दी है। जबसे सरकारी प्राइमरी स्कूल के हैंडपम्प का हत्था चोरी हुआ, सारे बच्चे पानी पीने यहीं आते हैं। कुएं की जगत पर बनवारी ने अपने बडे़ बेटे मिठुआ को एक डलिया मंे बीस-पचीस भेली गुड़ लेकर बैठा दिया है। टंकी पर पानी पीने वाले को एक ढांेका गुड़ भी दिया जाय। छोटे बच्चे गुड़ की लालच में डलिया के गिर्द अपना घेरा कसते जा रहे हैं।
बलई पांडे कहते हैं- शुरू करिए। दिन लटक गया।
लछिमन चैधरी कहते हैं- सबको पता है कि यह पंचायत बनवारी मिस्त्री ने रमेसर भगत और उनकी पतोहू कुच्ची के खिलाफ बुलाई है। दोनों फरीक बचन दें कि पंचायत जो भी फैसला करेगी, मानेंगे।
-जरूर मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बनवारी तुरंत उठकर कहता है।
-तुम बोलो कुच्ची। बलई पांडे उंगली दिखाते हैं।
-पद मानेंगे, कुपद नहीं मानेंगे।
-तो क्या हम लोग कुपद करने आये हैं? बलई नाराजगी दिखाते हैं।
-बचन तो दे दिए बाबा कि पद मानेंगे। अगर पंच दूसरे फरीक का गुड़ खाकर कहने लगें कि कुच्ची की आंख फोड़ दो, कान काट लो तो कैसे मानेंगे?
-पंच इतने सस्ते हैं कि गुड़ पर बिक जायेंगे?
-कौन कितने सस्ते-महँगे बिकेगा यह तो बिकने वाला जाने, लेकिन हमें भी पंच की जबान चाहिए कि वे न्याय करेंगे अन्याय नहीं करेंगे।
-कौन तय करेगा कि न्याय हुआ या अन्याय? धनई मिसिर पूछते हैं।
-आप का दिल तय करेगा बाबा। मेरी दादी कहती थीं कि जीभ की लगाम दिल के हाथ में रहने दीजिए, कुपद नहीं होगा।
बलई पांडे कहते हैं- जो भी पंचायत में बोलेगा वह बनवारी का गुड़ नहीं खायेगा। अब तो ठीक है?
लेकिन लछिमन चैधरी को कुच्ची की बात में आती बगावत की बू अच्छी नहीं लगी। वह कहते हैं- जब यहां रमेशर भगत मौजूद हैं तो कुच्ची से पूछने का क्या मतलब? उसी की ‘कुचाल’ पर तो पंचायत बैठी है। जो भी सजा जुरमाना होना है उसी पर होना है और भुगतना है रमेशर को, तो रमेशर भगत बचन दें।
रमेशर अपनी जगह खडे़ होकर हाथ जोड़ते हैं- पंच तो भगवान बराबर है चैधरी साहेब। भगवान से बाहर कैसे चले जायेंगे? हम पंच का ‘मान’ रखेगे। पंच अपनी ‘लाज’ रखें। इसी में ‘सब समाया’ है।
-ठीक है। बलई बाबा कहते हैं- बनवारी, अब तुम अपनी उजुरदारी लगाओ।
बनवारी कंधे पर पड़ा तौलिया हाथ में लेकर खड़ा होता है। दोनों हाथ जोड़ता है। तौलिया माथे से लगाता है और भोली सूरत बना कर शुरू करता है- -पंचों, सबको पता है कि इस पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी। हनुमान मेरे लिए सगे भाई से बढ़ कर था। समझो, मेरा दहिना हाथ था। हनुमान की अकाल मौत से हम सबकी कमर टूट गयी। उसकी बेवा की अभी कोई उमर नहीं हैं हमारे ‘रिसी मुनी’ कह गये हैं कि जवानी अन्धी होती है। उस पर किसी का जोर नहीं चलता। इसलिए हम सभी चाहते थे कि वह दूसरा घर कर ले। काका-काकी को हम खुशी-खुशी संभालते, ताजिंदगी। लेकन इस औरत के मन में जाने क्या पक रहा था कि कही जाने को राजी न हुई। क्यों? तो सास-ससुर की सेवा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। कैसी सेवा की इसने, यह तो काका जाने लेकिन मेरे खानदान की नाक जरूर कटा दी। पता चला है कि इसे छः महीने का ‘पेट’ है। यह कहां मिला? किसका है? काका बतावें या यह बतावे। काका यह भी बतावे कि सारा पाप जगजाहिर हो जाने के बाद भी उसे अपने घर में क्यों रखे हैं? कब तक रखेंगे? किसके लिए रखेंगे? पंच बतावे कि ऐसा कलंकी मुंह देखने से गांव वालों को कब ‘मुक्ती’ मिलेगी?
बनवारी एक बार दायें-बायें देखता है फिर अपनी जगह बैठ जाता है। बलई पांडे, लछिमन चैधरी की ओर देखकर कहते हैं- शुरु करिए।
चैधरी इंकार में सिर हिलाते हैं- आप ही शुरु करिए महाराज।
बलई पांडे खखार कर शुरू करते हैं- सकल गांव को पता है कि हनुमान को मरे दो-सवा दो साल से ज्यादा हो गये। कुच्ची बताए कि क्या उसके पेट में बच्चा होने की बात सही है।
-हां महराज। कुच्ची हाथ जोड़ कर खड़ी होती है- सही है।
-यह बच्चा कहां से आया?
-मैंने दूसरे से बीज लिया, महराज।
-क्यों?
-कई कारन हैं महराज।
-बता। सारा गांव जानना चाहता है।
-मुझे जरूरत लगी महराज। मेरा आदमी तो एक बार मर कर फुरसत पा गया लेकिन मुझे बेसहारा समझ कर हर आदमी किसी न किसी बहाने मुझे रोज मार रहा था। मैं मरते मरते थक गयी तो जीने के लिए अपना सहारा पैदा कर रही हूं।
-तो तुझे दूसरी शादी करने से किसने रोका था?
-दूसरी शादी कर लेती तो मेरे सास-ससुर बेसहारा हो जाते बाबा। अपने सहारे के लिये इनको बेसहारा छोड़कर जाते नहीं बना। मेरा रिस्ता मेरे आदमी तक ही तो नहीं था।
-लेकिन तू हनुमान की व्याहता है। तेरी कोख पर सिर्फ हनुमान का हक बनता है।
-मरे हुए आदमी के काम तो यह कोख आ नहीं सकती बाबा। उनके मरने के बाद किसका हक बनता है?
-दूसरा मर्द करेगी तो उसका हक बनेगा।
-दूसरा मंैने किया नहीं, तो किसका बनेगा? मेरी कोख पर मेरा हक कब बनेगा?
तू हनुमान के घर का हक हकूक भी लेगी और हराम का बच्चा भी पैदा करेगी, ऐसा कैसे होगा?
-हक हकूक की बात तो मैंने कभी सोची नहीं बाबा। मैं तो सोचती हूं कि जो जिम्मेदारी मरने वाला मेरे ऊपर डाल गया उसे पूरा करूं। मेरी सास पोते का मुंह देखना चाहतीं थीं। मेरा आदमी बेटे का मुंह देखना चाहता था। उसने तो नाम भी सोच लिया था- बालकिसन। मैं खुद बेटी चाहती थी। नाम सोच रखा था- किसनकली। इस बात पर उनसे अक्सर तकरार होती थी कि पहले बालकिसन आवे या किसनकली। लेकिन किसी के आने के पहले ही वे चले गये। कुच्ची की आवाज भर्रा जाती है -अब मैं उनकी आखिरी चाहत पूरी कर रही हूं।
-वाह! दूसरे से बच्चा जनमा कर अपने आदमी की चाहत पूरी कर रही है।
-तो क्या करती बाबा। वे तो जन्माने के लिए अब सरग से लौटकर आने से रहे और अकेले मैं जनमा नहीं सकती थी।
-तो तूने हराम की औलाद से हनुमान का वंश चलाने की ठानी है। वाह।
-उनका चले न चले। मेरा तो चलेगा।
-अरे मूर्ख वंश मां से नहीं बाप की बूंद और नाम से चलता है।
-ऐसा क्यों है बाबा? पेट में तो नौ महीना सेती है महतारी। बाप तो बूंद देकर किनारे हो जाता है।
-इतनी दूर तैरने से पार नहीं पायेगी, लड़की। तू इस गांव की बहू है। तूने क्यों नहीं सोचा कि तेरे इस कदम से गांव की नाक कटती है।
-मेरी गोद भरने से, मुझे सहारा मिलने से गांव की नाक कैसे कट जायेगी बाबा? क्या मेरे भूखे सोने से गांव के पेट में कभी दर्द हुआ? जेठ की धमकी से डर कर जब हम तीनों प्रणी रात भर बारी-बारी घर के भीतर पहरेदारी करते हैं तो क्या गांव की नींद टूटती है? जब यह बहाने बनाकर मुझे और मेरे ससुर को गरियाता-धमकाता है तो क्या गांव उसे रोकने आता है? जब मेरी भूख पूरे गांव की भूख नहीं बनती। मेरा डर पूरे गांव का डर नहीं बनता, मेरा दुःख-दर्द पूरे गांव का दुःख-दर्द नहीं बनता तो मेरे किये हुये किसी काम से पूरे गांव की नाक कैसे कट जायेगी?
- अरे! यह तो वकील का बाप बन रही है। बलई बाबा को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। कोई और पंच मदद के लिए आगे क्यों नहीं आता? धीरे-धीरे आगे पीछे झूमते हुए वे नया ‘पैंट’ निकालते हैं- तू क्या समझती है कि यह बच्चा हनुमान का कानूनी वारिस हो जायेगा?
-पता नहीं बाबा। कानून तो मैंने पढ़ा नहीं।
-कानून पढ़ा बेपढ़ा नहीं देखता। बलई बाबा की आवाज में चिढ़ समा गयी है- शिकंजे में पाता है तो बडे़-बड़ों को मुर्गा बना देता है। चांपता है तो मुंह से फिचकुर निकल आता है।
सिहर जाती है कुच्ची। कितनी मिर्च खाकर आया है यह बुड्ढा?
-आपका मुंह बहुत बड़ा है बाबा। कुछ भी बोल सकते हैं।
-कुछ भी क्यों बोलूंगा? जो कानून में लिखा है वही बोल रहा हूं। यह नाजायज संतान है। इसे हनुमान की प्रापर्टी में धेला भी नहीं मिलेगा।
-न मिले महराज। हम बैपारी तो हैं नहीं कि घाटा-नफा जोड़ कर सौदा करें। फिर तनिक रूक कर पूछती है- कानून में चांपने की बात भी लिखी है महराज?
-अब तू मेरी जबान पकडे़गी? इतनी सरहंग हो गयी?
-मर्द की जबान पकड़ना औरत के वश में कहां है बाबा? लेकिन यह बता देते कि कानून लिखा कहां जाता है, लिखता कौन है, तो चलकर उसी से फरियाद करते कि हमारे बालकिसन जैसों के जीने खाने के लिए भी ‘दू अच्छर’ कानून लिख देते।
कुच्ची की मूर्खता पर ठठाकर हंसते हैं बाबा। देर तक हंसते रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें सचमुच इतनी हंसी आ रही है। बस, मौका पाकर वे अपने मन मे घुमड़ कर परेशान करने वाली गैस निकाल रहे हैं।
-अरे मूरख, कानून रोज-रोज थोड़े लिखा जाता है। विरासत का कानून हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले लिख गये हैं। हजार साल पहले तो याज्ञवल्क्य मुनी की पोथी की टिकायें लिखी गयीं- मिताक्षरा, दायभाग, एकाध और। उसी के सहारे पंडित जवाहर लाल ने पचास साठ साल पहले कानून पास करवाये- हिन्दू, विवाह कानून, विरासत का कानून, गोदनामे का कानून वगैरह...। हां रे। गोदनामे के नाम पर एक काम की बात सूझी। अगर तू दूसरे का बच्चा गोद ले ले तो उस बच्चे को हनुमान की विरासत भी मिल जायेगी और तुझे बुढ़ापे का सहारा भी मिल जायेगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। बनवारी के ही तीनों बेटों में से किसी को ले सकती है।
-वाह! क्या ‘पैंट’ निकाला बाबा ने। बनवारी सिर नीचे करके अपनी मूछें ऐंठता है- इसको कहते हैं बुद्धी।
थोड़ी देर तक चुप्पी छा जाती है। सिर्फ कुंए की जगत पर बैठी औरतों के झगड़ने और बच्चों के गुड़ के लिए रोने, लड़ने की आवाज आती है।
पंचो की नजर कुच्ची पर टिक गई है।
कुच्ची पूरी पंचायत पर नजर घुमाते हुये कहती है- लेकिन मैं तो पहले ही ले चुकी। गोद में नहीं सीधे कोंख में।
फिर बलई की ओर मुंह घुमा कर कहती है- और अपने तो गजब का कानून बताया बाबा। दूसरे का पैदा किया हुआ गोद ले लूं तो उसे सब कुछ मिल जायेगा और अपनी कोख से पैदा करूंगी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मेरी कोख से पैदा होगा उसका आधा चाहे जिसका हो लेकिन आधा खून तो मेरा होगा। गोद वाले बच्चे में तो मेरे खून की एक बूंद भी नहीं होगी। दोनों में से मेरा ज्यादा सगा कौन हुआ? वह सिर घुमाकर चारों तरफ देखती है- मुझे तो विश्वास नहीं होता कि पंडित जवाहर लाल ऐसा अन्धा कानून पास कराये होंगे। फोटू में तो बहुत ‘गऊ’ आदमी लगते हैं।
लोग हंसने लगते हैं।
-ए भाई, ए तो बालिस्टर का कान काट रही है। बलई बाबा झुंझला जाते हैं।
- अब इस गाॅव में कुच्ची का कानून चलेगा बाबा। पीछे से कोई कूट करता है।
-लग तो यही रहा है। बलई कहते हैं - तुलसी बाबा ने सही कहा है, युवती नारि नृपति वश नाहीं। किसी और को कुछ पूछना हो तो पूँछे।
अब पंचों में से किसी को बोलने की जल्दी नहीं दिखती। सब दूसरे को पहले सुनना चाहते हंै।
-यह भेली बूढे़ चैधरियों के दांत से फूटने वाली नहीं लगती। कोई ठिठोली करता है।
धन्नू बाबा लछिमन चैधरी को इशारा करते हैं। -बढ़िए।
लछिमन चैधरी इंकार में सिर हिला देते हैं- आप ही बढे़ महराज।
-अच्छा कुच्ची। धन्नू बाबा कहते हैं- पहले तो तू अपनी जगह बैठ जा। घंटे भर से खड़ी है। अब बैठे ही बैठे जवाब दे।
कुच्ची सूखी घास पर बैठ जाती है। दोनों हाथ पीठ पीछे जमीन पर टिकाने से राहत महसूस करती है। उसे प्यास लग गयी है।
-इसके बैठने के लिए भी कोई पीढ़ा, मचिया लाओ भाई... हां, तू कह रही थी कि तेरे गर्भ धारण करने के कई कारण हैं। एक तो बताया, बाकी?
-बाबा बरम्हा ने औरत को कोख किसलिए दिया है?
-तू ही बता।
-मेरे जानते तो इसलिए कि वे बरम्हा की बनाई दुनिया को आबाद करती रहे। औरतें जब से दुनिया में आयीं हैं, वे बरम्हा का काम ही कर रही हैं।
-फिर?
बैठकर बोलने से आवाज दूर तक नहीं जा रही है इसलिए पीछे बैठे लोग उठकर आगे आने लगे हैं।
-मेरा कहना है कि कोख देकर बरम्हा ने औरतों को फंसा दिया। अपनी बला उनके सिर डाल दी। अगर दुनिया की सारी औरतें अपनी कोख वापस कर दें तो क्या बरम्हा के वश का है कि वे अपनी दुनिया चला लें?
-पता नहीं, तू ही बता।
-पाड़े बाबा ने भी मेरे सवाल का जवाब टाल दिया और आप भी टाल रहे हैं।
-तू सिर्फ वह बता जो पूछा जा रहा है।
-मुझे भी तो कुछ पूछने की छूट मिलेगी।
-अभी नहीं। अभी मेरे सवाल का जवाब दे।
-मैं अपनी कोख का उद्धार करना चाहती थी। बचपन से सुनती रही हूं कि कोख का उद्धार तभी होता है जब कोख फले। अपने ‘जन्मे’ को दूध पिलाकर मैं मां के दूध से ‘उरिन’ होना चाहती थी।
-और कोई कारण?
-हां बाबा, मैं अपनी कोख पर लगा ‘बांझ’ का कलंक छुड़ाना चाहती थी। मेरे जेठ ने दो साल में जाने कितनी बार ‘बाझिन’ कहकर मेरे करेजे में बरछी भोंकी है।
अचानक बलई बाबा कुच्ची की ओर उंगली उठाकर पूछते हैं - बड़ा कलंक क्या है? कोख का बांझ रह जाना या कोख में हराम की औलाद पालना?
धन्नू बाबा रोकते हैं- बाद में, बाद में। पहले मेरी जिरह खतम हो जाने दीजिए।... और कोई कारण?
- हां बाबा मैं जानना चाहती थी कि बच्चा पैदा करने की पीर कैसी होती है? अपने जैसा दूसरा जीव पैदा करने का सुख कैसा होता है?
-पैदा करने का सुख? बनवारी चिल्ला पड़ता है- साफ क्यों नहीं कहती कि छिनारा का मजा लेना चाहती थी।
-छिनारा का मजा लेने के लिए तो तुम बहुत हाथ पांव मारे लेकिन अपना सा मुंह लेकर रह गये। इसी किलक के चलते तो इतना उत्पात मचाए हो। पंचो, इसने मुझे अरहर की मधु समझ लिया था कि जब चाहेगा उंगली डुबो कर चाट लेगा। जब दाल नहीं गली तो गांव से भगाने के लिए ‘ऊधमबांह’ जोत रहा है। यह समझता है कि गांव के लोग ‘बच्चा’ हैं। उन्हें गुड़ खिलाकर फुसला लेगा। पद में यह मेरा जेठ लगता है। कायदा है कि जेठ अपनी भयहु की परछायी भी बचा कर चलेगा। सीधे छूने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन ‘उनको’ मरे तीन महीने भी नहीं हुए थे कि इसने धोखे से मेरी ‘छाती’ पकड़ लिया। जब मेरी सास अस्पताल में थीं तो बुरी नीयत से मेरे सूने घर में घुस आया। बाल तो इसके आधे सफेद हो गये लेकिन दिल अभी तक काला है। मुझे पटाने के लिए महारानी बना कर रखने का लालच दे रहा था। पूछिए इस कपटी से, सच है कि झूठ? इसी पंचायत में इसका फैसला भी होना है।
-यह तो भारी जुर्म है। किसी औरत के सूने घर में बुरी नीयत से घुसना। इसमें तेा धारा 354 लग जायेगी। धन्नू बाबा चारों तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहते हैं- अब यह धारा भी गैर जमानती हो गयी है। सात साल की सजा।
-बाबा, यह एक नम्बर की ‘हरहट’ है। बनवारी चिल्ला कर कहता है- सरासर झूठ बोल रही है।
-मैं मौके का गवाह पेश कर दूंगी। मेरी गवाह इसी पंचायत में बैठी है।
-पहले जो मामला पेश है उसका तो हला भला होने दें। बलई बाबा कहते हैं।
-जब पंचायत बैठ गयी है तो दोनों फरीकों के मामले निबटा कर उठेगी। एक दिन में नहीं दो दिन में सही। धन्नू बाबा समाधान करते हैं- लेकिन तुम इसे छिनारा क्यों कहते हो बनवारी? छिनारा कहते हैं अपने आदमी और परिवार से छिपाकर दूसरे आदमी से लगने को। यह तो साफ कह रही है कि उसे बच्चे की जरूरत थी और उसका पति मर गया था।
-मर गया था तो सबर करती। बलई गरजते हैं- और अगर इतनी जवानी चर्रायी थी कि धरा-थामा नहीं रही थी तो दूसरा सांड़ जैसा भतार खोज लेती।
-ए महराज, जवानी तो आप की चर्रायी थी। वह भी पचास साल की उमर में। सुधरा ठकुराइन अचानक बलई बाबा की ओर तर्जनी उठा कर कहती हैं- ऐसी चर्रायी थी कि परायी औरत को फुसलाकर घर में बंद कर लिए और चंगुल से निकल भागी तो भोकार छोड़ कर रो रहे थे।
लोग ठठाकर हंस पडे़ हैं। औरतें मंुह में आंचल ठंूस कर हंस रहीं हैं। छोटे बच्चे भौचक होकर रोना बंद कर दिए हैं।
बलई बाबा का चेहरा फक पड़ जाता है।
क्या चरखा दांव मारा ठकुराइन ने। चित कर दिया।
0
बात पुरानी जरूर है लेकिन लोग भूले नहीं हैं। बलई बाबा की घरैतिन को गांव की बूढ़ी औरतें दयालु प्राणी के रूप में याद करती हैं। तब गांव के हर घर में दोनों जून चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती थी। वे भूखे-दूखे के दुःख में सहारा बन कर खड़ी होती थीं। लेकिन अच्छे आदमी की जरूरत तो ऊपर भी रहती है। जिस साल उन्होंने बेटी को व्याह कर विदा किया उसी साल तीन दिन के दिमागी बुखार में चल बसीं। तब बाबा के बेटे सनातन दस-ग्यारह वर्ष के थे। खुद बाबा अभी चालीस के अंदर थे। यह मानकर कि कोई न कोई बेटी वाला देर सबेर घेर कर फिर बलई बाबा का ब्याह कर देगा, भावी सौतेली मां के अत्याचार से बचाने के लिए सनातन के नाना-नानी उसे अपने साथ ले गये। बाबा की घरैतिन मां बाप की अकेली थी इसलिए बलई सनातन को ननिहाल भेजने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि नानी का धन, पानी का धन (दूध में) और बेईमानी का धन सबको नहीं फलता। वे अपने बेटे को ऐसे धन का वारिस बनने से बचाना चाहते थे लेकिन सास की जिद के आगे हार गये। एक बार गया तो सनातन ननिहाल का ही होकर रह गया। नाना-नानी ने ही उसका विवाह किया। बलई बाबा बराती बनकर गये और लौट आये। बाबा गोरे चिट्ठे लम्बे सुदर्शन थे। ज्यादातर केवल धोती पहनते थे। छाती पीठ पर सिर्फ जनेऊ। जिधर से निकलते औरतें काम छोड़कर किवांड की ओट से निहारने लगतीं। अच्छी खेती बारी थी लेकिन जाने क्यों कोई बेटी वाला फिर उनकी ड्योढ़ी नहीं चढ़ा। बाबा तनहा रह गये। स्वपाकी हो गये। नैका कहाइन की सास दिलराजी जब तक जिंदा थी उनका चैका बर्तन कर देतीं, चूल्हा जलाकर चावल दाल चढ़ा देतीं। सब्जी छौंक देतीं। आटा गूंथ देतीं। बाबा नहाकर बटुली-कड़ाही उतार लेते। दिलराजी बेल देती, बाबा सेंक लेते। बदले में बाबा ने कमाने खाने के लिए गोयड़ का एक बीघा खेत दे दिया था। बाबा ने दिलराजी से कई बार कहा कि अब तुम्हारी उमर हो गयी है। खुद खटने के बजाय अपनी बहू नैकी को भेज दिया करो लेकिन दिलराजी दिल की बड़ी कठोर निकलीं। नैकी को एक दिन के लिए भी अकेले नहीं भेजा। कभी लायीं भी तो साथ लेकर आयी, साथ लेकर लौट गयीं।
बाबा ने बहुत चाहा कि इलाके में मथुरा की तरह उनका नाम भी ‘महालिंगम‘ मशहूर हो जाय लेकिन नहीं हो सका। हां, शंकर के पुजारी और बाद में शंकर भगवान के अवतार के रूप में जरूर उनकी ख्याति तेजी से फैली। उन्होंने दरवाजे के सामने पाकड़ के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनवाया। बनारस से रेडीमेड जटाजूट, डमरू, चांदी का वक्र चन्द्रमा, प्लास्टिक का फनधारी कालानाग और मृगछाला लाये। लाले लोहार से ढाई गज लम्बा त्रिशूल बनवाया। भभूत पोत कर और लंगोट के ऊपर मृगछाला बांध कर डम डम डम डम डमरू बजाते हुए बाबा जब तांडव नृत्य करते तो लगता खुद शंकर भगवान कैलाश पर्वत से उतर आये हैं। शिवरात्रि के दिन उनका नृत्य देखने सारा इलाका उमड़ पड़ता। उनका नाम ही तांडव बाबा पड़ गया।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयः......
चकार चण्ड्ताँडवं तनोतुनः शिवः शिवम्
डमरू से इतनी स्पष्ट आवाज निकालते कि खुद शंकर भगवान भी न निकाल पाते होंगे। तांडव देखती स्त्रियों की आंखों से झरता प्रशंसा का भाव बाबा को तृप्ति से भर देता। उनका ‘मानुष तन किसी को तो संतुष्ट कर रहा है, वैसे न सही-ऐसे सही।
एक दिन शाम के झुटपुटे में बाबा दिशा मैदान से लौट रहे थे तो पगडंडी पर एक औरत तेजी से आती दिखी। पास पहुंच कर बाबा से पूंछा- मायापुर कितनी दूर पडे़गा?
बाबा ने ध्यान से देखा। उमर पैंतीस चालीस के बीच। रंग गेहुंआ। देखने में सीधी सादी। माया की मूरत मायापुर का पता पूछ रही थी।
बाबा को नारद मोह हो गया। बोले- दूर तो कोस भर से ज्यादा नहीं है लेकिन तीन चार दिन से उधर लकड़बग्घा निकला है। औरतों-बच्चों पर रोज हमला कर रहा है। इस समय अंधेरे में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। सामने मेरा घर है। रात रूक जाओ। सबेरे चली जाना।
औरत मान गयी। उसे क्या पता कि बाबा अपने घर में अकेले हैं। एक बार ड्योढ़ी के अंदर गयी तो कपाट बंद। लोग कहते हैं कि बाबा ने उसे अपने हाथ से छानकर देशी घी की पूड़ियां और घुइयां की सब्जी खिलायी थी। रात भर का साथ रहा। चैथे पहर बाबा ने प्रस्ताव रखा कि हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जातीं मेरे घर। बारह बीघे खेत हैं। बाग बगीचे। घरैतिन के गहने। रोटी पोने वाली के अलावा भगवान ने सब कुछ दिया है। सुख से रखेंगे। वह शायद मान भी गयी। लेकिन भोर में दिशा मैदान जाने की बात आयी तो बाबा ने सावधानी बरतना जरूरी समझा। कहते है कि औरत तभी तक अपनी है जबतक अपनी जांघ के नीचे है। तुलसी बाबा तो बहुत पहले ‘मानस’ मे सावधान कर गये हैं- निज प्रतिबिम्ब बरूक गहि जाई। जानि न जाय नारि गति भाई।
खंूटी पर डोरी का बंडल टंगा था। पहले लोग यात्रा पर पैदल निकलते थे तो लोटा, डोरी साथ लेकर निकलते थे। जहां प्यास लगी, कुंए से पानी निकालकर पी लिया। अब न कुंए रहे न पैदल चलने वाले। सालों से बेकार टंगी थी। प्यासे बाबा ने उसे उतारा। पानी भरा लोटा औरत के हाथ में पकड़ा कर जंगल ले गये। डोरी का फंदा उसके दाहिने पैर में फंसाकर बंडल का लपेटन खोलते हुए कहा- जाकर उस झाड़ी के पीछे बैठ जाओ। डोरी का दूसरा सिरा पकड़कर वे बीस गज दूर बैठकर इंतजार करने लगे।
उजाला होने लगा। वे डोरी को खींचकर देखते। डोरी तन जाती। इत्मीनान हो जाता। लेकिन इतनी देर तक कर क्या रही है? रात भर की जगी थी, सो तो नहीं गयी? हिचकते हुए जाकर झाड़ी के पीछे झांका। न कहीं लोटा न लोटे वाली। डोरी का फंदा झाड़ी की टहनी में फंसा था। बाबा आसमान से गिरे। पहर दिन चढ़े तक जंगल में ढूंढते रहे फिर रोते हुए वापस लौटे।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदंमुखच्छिदं...
गजच्छिदाँध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे
रावण कहता है कि शिवस्त्रोत का पाठ करने वाले को भगवान शंकर- रथ, गजेन्द्र और तुरंग के साथ-साथ समुखि व लक्ष्मी प्रदान करते हैं। ताण्डव बाबा को सुमुखि तो दिए लेकिन सिर्फ रातभर के लिए।
शाम को उस औरत का आदमी लाठी लेकर खोजता हुआ आया। पूछा? कौन है इस गांव में वह आदमी जो अपने घर का अकेला है। जिसके दरवाजे पर पाकड़ का पेड़ है। जिसके दाहिने पंजे में छः अंगुलियां हैं जिसने मेेरी औरत को फुसला कर घर में बंद कर लेना चाहा। जिसके डर से भागकर उसे रात भर जंगल में छिपना पड़ा। तब गांव वालों को बाबा के रोने का रहस्य समझ में आया। अच्छा हुआ कि बाबा दोपहर में गंगा स्नान के लिए निकल गये थे।
इस दुर्घटना के बाद प्रायश्चित स्वरूप बाबा नंगे पांव रहने लगे। मूंज की जनेऊ पहनने लगे। खुद को ‘कामारि’ बनाने पर तुल गये। ‘उसे’ भी मूंज के बन्धन में जकड़ दिया। बहुत दिनों तक बलई का जिक्र आते ही धन्नू बाबा मुस्कराते और तुलसी बाबा के दोहे को किंचित संशोधित करके सुर में सुनाते-
काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह की धारि’
तिन्ह मंह अति दारून दुखद मायापुर की नारि।
0
कुच्ची के बैठने के लिये मचिया आ गई है।
लाले लोहार की बहू पीने के लिये उसे पानी का गिलास देती है।
-परायी औरत को सूने घर में रातभर बंद रखने का फैसला भी लगे हाथ हो जाय। सुधरा कहती हैं।
-अरे छोड़िए ठकुराइन, पचीस साल पुरानी बातें। धन्नू बाबा मुस्करा कर कहते हैं- रात गयी बात गयी।
-कब तक छोडे़ रहेंगे बाबा? हाईकोट भी कहता है कि पुराने मामले पहले निबटायें जायें।
-पहले जो मामला पेश है वह तो निबटे। लछिमन चैधरी कहते हैं- एक ही दिन में क्या-क्या निबटायेगें?
-ठीक है। धन्नू बाबा लछिमन चैधरी से कहते हैं- अब आप बढ़ाइये।
लछिमन चैधरी सिर में अंगोछा लपेटते हुए कुच्ची की ओर देखते हैं।
-पंच जानना चाहते हैं कि यह बीज तू कहां से लायी?
धन्नू बोल पड़ते हैं - मंैने तो सुना है कि रमेसर चैधरी अयोध्या जी गये थे। वहां से खीर का प्रसाद लाये। उसी को खाने से इसे गर्भ ठहरा।
-खीर खाने से गर्भ ठहर जायेगा महराज? लछिमन चैधरी पूछते हैं।
-ठहर जायेगा नहीं, ठहर गया। एक नहींे चार-चार। नाम बताएं?
-वह त्रेता की बात थी महराज। यह कलजुग है।
-जो त्रेता में हो सकता है वह कलजुुग में क्यों नहीं हो सकता? त्रेता में तो खाने से ठहरा। द्वापर में तो सुमिरन करने भर से ठहर गया। इस रफ्तार से कलियुग में देख लेने भर से ठहर सकता है।
-हे भाई। पीछे से आवाज आती है- बहुत खुलकर कुच्ची का पक्ष ले रहे हैं बाबा। कहीं आड़े ओटे चखा तो नहीं दिया?
-अब बहत्तर साल की उमर में चखने लायक तो क्या रह गये होंगे। दूसरा मुस्कराता स्वर- हां चटा दिया हो तो बात दूसरी है।
-यह कौन बोला? लछिमन चैधरी डपटते हैं- पंचायत में मसखरी करने आये हो? मुर्गा बना कर पीठ पर दस ईट लाद दी जायेगी तो दिमाग दुरूस्त हो जायेगा।
-इसको नहीं, इसके बाप को मुर्गा बनाओ, जिसने ऐसी मुरही औलाद पैदा की।
लेकिन पता ही नहीं लग रहा कि बोलने वाला कौन है?
कुएं की जगत पर बैठी दुलहिनों के झुंड में खीर की बात सुन कर हंसी की लहर दौड़ गयी है। एक दुलहिन चतुरा अइया के कान में मुंह सटाकर पूछती है- खीर खाने से कि खीरा खाने से अइया?
फिर हंसी की लहर!
-तू क्या समझती है, सचमुच खीर खाने से पैदा हो गये?
-रमायन में तो यही लिखा है।
- लिखने पढ़ने से सच हो गया? सारा झूठ फरेब तो पढे़ लिखे लोग ही करते हैं।
-हे! धन्नू बाबा डपटते हैं- तुम लोगों ने उधर क्या गपड़चैंथ शुरू कर दी? शान्त रहो।
कुच्ची मचिया से उठने की कोशिश करती है लेकिन लोगों के मना करने पर फिर बैठ जाती है।
-खीर हलुआ खाने और सुमिरन करने से रानी महरानियों के पैदा होते होंगे पंचों। उनकी मदद करने तो देवता-पित्तर सब दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हमारे जैसों की मदद करने वाला तो कोई मानुख पुरुख ही होगा।
- पंच जानना चाहते हैं कि वह मददगार मानुख पुरुख कौन है?
-जो पुरुख मेरे मन में बस गया। जिसके जैसा बच्चा मैंने चाहा।
-तो तेरे मन में हनुमान के अलावा कोई पुरुख बसता था?
-हर औरत के मन में कोई न कोई पुरुख बसता है। कभी वह उसे पा जाती है कभी नहीं पाती। नहीं पाती तो जिसे पाती है उसी में रम जाती है। मेरे मन में पहले से नहीं बसा था लेकिन जरूरत पड़ी तो बसाना पड़ा।
-वाह! विधिहुं न नारि हृदय गति जानी। बलई बाबा हवा में प्रणाम करते हैं।
लछिमन चैधरी हंसने लगते हैं -तू तो पूरी पंडित है कुच्ची। पंचों को भी बता कि तेरे मन में बसने वाला वह पुरुख कौन है?
-यह गुप्त दान है बाबा। दान करने वाले ने इसी शर्त पर दिया है कि उसका नाम गुप्त रखा जायेगा।
-क्यों?
-क्योंकि नाम जाहिर कर देने से दान का पुण्य मर जायेगा। इसीलिए तो बडे़-बडे़ सेठ-महाजन गंगा जी में डुबकी लगाकर लाखों की मोहर, असर्फी दान करते हैं और बायें हाथ को पता नहीं चल पाता कि दाहिने ने कितना दान किया?
एक बार फिर चुप्पी।
-अरे लछिमन चैधरी का ही नाम लगा दे। कोई मनचला कूट करता है- इनसे पूरे गाॅव के लिए पूड़ी तरकारी का भोज लिया जायेगा।
लिहाड़ी लेने और ‘व्यंग’ बोलने में इस गाॅव के लोगों का जवाब नहीं। वे मौका मिलने पर फब्ती कसने से नहीं चूकते। कभी कभी आवाज बदलकर भी।
लछिमन चैधरी बनावटी गुस्सा दिखाते हैं- वाह भाई! मजा मारै गाजी मियां धक्का सहैं मुजावर।
सामूहिक हंसी।
-अच्छा यह बता, अपने यहां तो ‘मिलुअई’ लाने का भी चलन है। तुझे दूसरा घर नहीं करना था तो कोई ‘मिलुअई’ ही खोज लेती। बहुत लोग अकेले पडे़ जिंदगी काट रहे होंगे। वह तेरे काम भी आता और तेरी-खेती बारी भी संभालता।
-पहली बात तो यह कि हाथ-पैर चलते मेरे सास-ससुर ‘मिलुअई’ क्यों आने देते? आने भी देते तो ऐसा मिलुअई कहां से खोज कर लाती जो मन का भी होता और मिलकर भी चलता। सास-ससुर की सेवा के लिए तो मैंने दूसरे घर, वर का मोह त्यागा। वह उंगली पकड़ने के बाद पहुंचा पकड़ने लगता तो? सास-ससुर की छाती पर मूंग दलने लगता तो? या यह भी न करता, किसी रात गहना, गीठी लेकर भाग खड़ा होता तो? धन धरम दोनों चला जाता। ऐसे कितने मामले सुने गये हैं।
बात तो सोलह आने सही कह रही है। कई सिर सहमति में हिलते हैं।
-अब? और कोई कुछ पूछना-कहना चाहें। लछिमन चारो तरफ देखते हैं।ै
शाम उतरने लगी है। आग अदहन का समय हो गया है। मामला किसी सिरे चढ़ता नजर नहीं आता। अभी बच्चे भूख से रोना शुरू कर देंगे। चारा देना है। गाय-भैंस दुहना है। इक्का-दुक्का आदमी और दो-दो, चार-चार के झुंड में औरतें सिर झुका कर धीरे-धीरे खिसकने लगीं हैं।
लछिमन चैधरी को लग रहा है कि जितनी जल्दी फैसले तक पहंुचने की सोचा था वैसा होता नहीं दिखता। यह औरत रंच भर डरने या झुकने को तैयार नहीं। सबकी बोलती बंद कर दे रही है। इसको लपेटने के लिए नया फंदा तलाशना होगा। वे दायें-बायें देखकर कहते हैं- पंचो लगता है किसी नतीजे पर पहुंचने में अभी एक दो दिन लग जायेंगे। पांच छः घंटे में सब थक गये हैं। दिशा-मैदान का समय हो गया है। खाना-पीना भी करना है। धन्नू बाबा और बलई बाबा को संध्या आरती के लिए समय चाहिए। सुघरा ठकुराइन काली मंदिर में संझा की दिया-बाती करती हैं। अगर सबकी राय हो तो कल दोपहर तक के लिए पंचायत रोक दी जाय। कल दोपहर इसी जगह फिर बैठते हैं।
धन्नू बाबा कहते हैं- बात तो ठीक है लेकिन एक बार पंचायत टूटी तो फिर सबको जुटाना मेढ़क तौलने जैसा हो जायेगा। कोई ऊदपुर निकल जायेगा, कोई महमूदपुर। मेरी मानिए, पंचायत को रोकिए जरूर लेकिन तीन-चार घंटे के लिए। लोग अपने जरूरी काम निबटाकर दस बजे तक वापस आ जायंे। रात में जितनी भी देर हो जाय, हला भला करके ही उठा जाय।
यही तय होता है।
0
सबेरे पंचायत में जाते समय तीनों प्राणियों मुंह लटका हुआ था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन बहू का सवाल जवाब सुन कर रमेसर दोनों प्राणियों की अटकी हुई सांस इस समय सम पर चल रही थी। रमेसर लौटते ही जानवरों का चारा पानी करने में लग गये।
पंचायत के डर ने कुच्ची को कल से ही अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सबेरे किसी तरह उसने गले के नीचे एक रोटी उतारी थी। इस समय भी भूख गायब थी लेकिन सास ससुर तो उपवास नहीं कर सकते, इसलिए पिछवाड़े जाकर वह उपले और जलावन लायी। चूल्हा पोता और ताखे से माचिस लेने के लिए मुड़ी ही थी कि कराह कर बैठ गयी। बूढ़ी लपक कर आंगन से आयी और सहारा देकर उठाते हुए पूछा- क्या हुआ?
-लगा जैसे पेट के अंदर छुरी चल गयी अम्मा। दर्द की लकीर आरपार हो गयी।
कांपती टांगों से चारपायी की ओर बढ़ते हुए टूटती आवाज में कहा- चक्कर आ रहा है।
उसे चारपायी पर लेटा कर बूढ़ी पाटी पर बैठा कर हवा करने लगी। कुच्ची की आंखें मुंद गयीं। लगा नींद आ रही है। नींद या मूर्छा?
तब तक बजरंगी आ गया। पूछा - क्या हुआ?
-तुम कहां चले गये थे?
-मैं गोलगप्पे लेने गया था।
-मेरी जान सांसत में पड़ी है और तुुम्हें गोलगप्पे की सूझ रही है।
-सांसत में क्यों? लो गोलगप्पे खा लो। ठीक हो जाओगी।
जिस समय पपड़ियाए होंठो को तर करने के लिए बूढ़ी ने कुच्ची के मुंह से पानी भरी सीपी लगायी, ठीक उसी समय बजरंगी ने खट्टे पानी से भरा गोलगप्पा भी लगा दिया।
कुच्ची ने चैंक कर आंखें खोल दी।
-कहां गये?
-कौन? बूढ़ी ने उसके होंठ के दोनों तरफ बहे पानी को अपने आंचल से पोछते हुए पूछा।
कुच्ची को मुंह का स्वाद खट्टा खट्टा सा लग रहा था।
दायें बायें नजर घुमाते हुए वह उठने की कोशिश करने लगी। बूढ़ी ने मना किया- लेटी रह। आराम मिल जाने दे। मैं तेरे लिए दाल का पानी तैयार करती हूं।
बूढ़ी ने चूल्हा जला कर अदहन चढ़ाया। अदहन गनगनाने लगा तो बटलोई में अरहर की दाल, नमक और खटाई एक साथ डाला; ईंधन तेज किया फिर आटा गूंथने लगी।
कटोरे में दाल का पानी निकालने के बाद आटे की छोटी छोटी टिकरियां बना कर बटलोई में डाला और ऊपर से पानी भरे लोटे का ढक्कन लगा दिया। बूढ़ी के मायके में इन्हें ‘दलफरा’ या ‘दाल का दुलहा’ कहते हैं। तुरंता भोजन। झटपट तैयार! खटाई की महक से सुवासित ऐसी टिकरियों का स्वाद ही अलग होता है। उदास निराश मन इनके स्वाद से उछाहिल हो जाता है।
कुच्ची का दर्द तो गोलगप्पे खाने के बाद ही शांत हो गया था। आराम करने और दाल का नमकीन पानी पीने के बाद चैतन्य हुई तो घर में रुका नहीं गया। वह धीरे धीरे चल कर धरमराज वकील के दरवाजे पहुंची। उसने कल धरमराज से भी पंचायत में आने को कहा था लेकिन वह टाल गया।
कुच्ची ने कल शाम धरमराज वकील के घर जाकर पचांयत में आने के लिए कहा था। तब उसने कचेहरी जाना जरूरी बता कर टाल दिया था। अभी घंटे भर की मोहलत मेें वह फिर उसके घर गयी।
दरअसल रिश्ते में भाई लगने वाले बनवारी के खिलाफ बोलने वे वह बचना चाहता था। धरमराज अपने घर के बाहर ही मिल गया। कुच्ची को देख कर झेंप गया। बिना पूछे ही सफाई देने लगा कि एक जमानत के सिलसिले में कचहरी जाना जरूरी होने के कारण...
-कोई बात नहीं देवर अब तो चलोगे?
-बिलकुल। और अकेले नहीं। उधर देखिये... उसने सामने काला कोट पहन कर कुर्सी पर बैठी तीन महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा- आपकी ओर से बहस करने के लिए शहर से तीन तीन वकील ले आया हूं।
कुच्ची ने हाथ जोड़ कर तीनों को नमस्कार किया। धरमराज ने परिचय कराया-यही हैं हमारी कुच्ची भौजी और भौजी ये हैं मनोरमा जी, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा। साथ में दो और पदाधिकारी। औरतों के खिलाफ कहीं भी होने वाले जोर जुल्म के खिलाफ ये हमेशा जान लड़ाने को तैयार रहती है। वकील तो हैं ही।
कुच्ची ने एक बार फिर सिर झुकाया।
धरमराज से इस विचित्र पंचायत की बात सुन कर यह सभी कुच्ची से मिलने के लिए आतुर थीं। जरूरत पड़े तो कुच्ची के पक्ष में बोलने का का मन बना कर आयी हैं। किसी से बीज लेकर बच्चा पैदा कर लेने की कल्पना से ही वे सब रोमांचित हैं। कोई औरत इसके अधिकार की मांग कर सकती है, यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कभी। और यह मांग एक ऐसे गांव की सातवी पास औरत भरी पंचायत में कर रही है जहां न सड़क है न स्कूल है। जहां के लोग आज भी कंुए या हैंडपम्प का पानी पीते हैं और लालटेन या ढिबरी के प्रकाश में जीते हैं। जहां चैबीस घंटे में चार छः घंटे बिजली का लगातार रह जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
उनके संगठन की अधिसंख्य महिलायें परिवारदार हैं। बेटी बेटा व्याह चुकी हैं या व्याहने वाली हैं। जब तक कोई औरत शरण सुरक्षा और रोटी के लिए किसी पुरूष पर निर्भर है, वह ऐसी मांग कैसे कर सकती है? ऐसी मांग का समर्थन करते हुए अखबार में फोटो छप गया तो घर से निकाल दी जायेगी। उनका संकोच देख कर धरमराज कहता है- आप सब की मौजूदगी ही बहुत कुछ बोलेगी। चलिए।
कुच्ची की पुकार सुनकर बिसुन परधान का ड्रायवर बाहर आते हुए ऊंची आवाज में बताता है- परधान जी तो ब्लाक से ही ससुराल चले गये। मैं खाली बुलेरो लेकर लौटा हूं। फिर पास पहुंचने पर धीरे से कहता है- भीतर हल्के के सिपाही के साथ चाह पकौड़ी काट रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। आवास घोटाले की जांच में एफआईआर दर्ज हो गयी है। जमानत का इंतजाम होने तक छुपे-छुपे दिन काटना है।
इस बीच मिठुआ ने दो गैस बत्ती जला कर महुए की डाल से लटका दिया है। पास से जा रहे बिजली के खंभे में कटिया लगा कर उसमें सौ वाट का बल्ब लटका दिया है। रात बारह बजे बिजली आ जायेगी।
दोपहर से शुरु हुयी इस पंचायत के सवाल जवाब की शोहरत दूर तक फैल गयी है। पड़ोस की बाजार में आँगनबाड़ी की कार्यकतिृयों, ग्राम सेविकाओं, स्वास्थ्य-केन्द्र की दाइयों, बैंक और ब्लाक की महिला कर्मचारियों और अध्यापिकाओं की एक बड़ी संख्या किराये पर कमरा लेकर रहती है। उनके लिए यह बड़ा रोमांचक है कि गाॅव की एक विधवा औरत अवैध गर्भ सेते हुए चैधरियों की घेरेबन्दी से अकेले दम मोर्चा ले रही है। ऐसी औरत को देखने सुनने की लालसा उन्हें भी पंचायत में खींच लायी है। वे झुंड बनाकर बीच की खाली जगह में बैठती हैं।
धरमराज वकील खुद महुए की जड़ पर बैठ गये हैं। महिला वकीलों के लिए कुर्सी का इन्तजाम है। दूसरे पंचों की बराबरी में काला कोट पहन कर बैठी तीन तीन औरत वकील और बाजार से आयी औरतों का झुंड पंचों को कुछ असहज कर रहा है। क्या कुच्ची के बुलावे पर आयी है यह सभी?
लेकिन लछिमन चैधरी सांस खींचकर अपने को मजबूत करते हैं और दो टूक कहते हैं- तो तू बच्चे के बाप का नाम बताने को तैयार नहीं है?
-बच्चे के बाप का नाम जानने की न तो पंचायत को जरूरत है न हक।
-हक क्यों नहीं है?
-बताइये कैसे है हक? यह भी बताइये कि पंचायत को सिर्फ सवाल पूछने का हक ही है या जवाब देने की जिम्मेदारी भी?
-दोनों?
-तो मेरे पहले सवाल का जवाब अभी तक क्यों नहीं मिला? तंडो बाबा मेरे सवाल का जवाब पी गये। जब मेरे हाथ, पैर, आंख, कान पर मेरा हक है, इन पर मेरी मरजी चलती है तो कोख पर किस का होगा, उस पर किसकी मरजी चलेगी, इसे जानने के लिए कौन सा कानून पढ़ने की जरूरत है?
अभी-अभी लौटे हैं बलई बाबा। ठीक से बैठ भी नहीं पाये कि इस लड़की ने सीधे उनपर उंगली तान दी। वे आग्नेय नेत्रों से कुच्ची की ओर देख कर कहते हैं- फिर कानून बीच में लायी? मैं देख रहा हूं कि बहसा-बहसी करने में तू गार्गी से भी पांच हाथ आगे बढ़ी जा रही है। करतूत अहिल्या की और तेवर गार्गी के। अहिल्या जैसी औरतों को हजार साल तक पत्थर की जिंदगी जीने की सजा मिलती है, यह मालूम है कि नहीं?
-नहीं मालूम महराज, लेकिन यह मालूम है कि आप हमें धमका रहे हैं। यहां इंसाफ करने के लिए बुलवाया है कि धमकी देने के लिए?
-धमकी नहीं दे रहा, हकीकत बता रहा हूं। अहिल्या के किस्से से सबक सीखा होता तो आज यह पंचायत बुलाने की जरूरत ही न पड़ती।
-ऐसा नहीं है महराज। सुधरा बोल पड़ती हैं- कुच्ची ने न सही लेकिन हजारों साल से इस देश में पैदा हो रही औरतों ने जरूर सबक सीखा है। उसी सीख से उनका कलेजा पत्थर का हो गया है। उसी का डर दिखाकर वे आज भी भेंड़ के झुंड की तरह हांकी जा रही हैं। लेकिन यह बताइये कि गौतम मुनि ने अपनी सारी मर्दानगी अपनी औरत पर ही क्यों दिखायी? सूने घर में घुसकर जिसने छल से अकेली औरत की इज्जत लूटी उसका तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाये। वह मूंछ ऐंठता मुस्कराता सामने से निकल गया। उल्टे खिसियाहट मिटाने के लिये अपनी ही छली गयी पत्नी को पत्थर बना दिया। यह कैसा इंसाफ है? इसमें औरत के सीखने के लिये क्या है?
-बिल्कुल सही। बाजार से आयी औरतों के झुंड से आवाज आती है - हम सब अहिल्या हैं। आज भी अहिल्या हैं। आज भी पत्थर हैं। आज भी छली जा रही हैं।
-सन्नाटा!
इन औरतों का शामिल होना बलई बाबा और लछिमन चैधरी के अंदर सिहरन पैदा कर रहा है। सुघरा से उलझने में भी बुद्धिमानी नहीं समझते बलई। एक तो औरत, दूसरे बेवा, तीसरे इसी गांव की ठकुराईन। कौन इसकी जीभ पकड़ सकता है। वह जो बोलेंगे उसी का सिरा पकड़ कर यह उन्हें पटकनी दे सकती है।
सन्नाटे को कुच्ची ही भंग करती है।
-बाबा उन औरतों का मामला वे जाने या आप जैसे पोथी पत्रा बाचने वाले जाने। यहां हमें बुलवाया है तो हमारी हर्ज-गर्ज पर बिचार करिये। बात से कायल कर दीजिए या कायल हो जाइये। मेरी कोख पर मेरा हक है कि नहीं?
-क्या कहें, कुछ सूझ नहीं रहा। यह भी कैसे कह सकते हैं कि उसकी कोख पर उसका हक नहीं है। उसका नहीं तो किसका है?
लछिमन चैधरी को भी बेज्जत होने का डर सता रहा है। लगता है सारी औरतें कुच्ची के पक्ष में खड़ी हो गयी हैं। सही कहा है, औरत जात को मुंह नहीं लगाना चाहिए। रमेशर को कटघरे में खड़ा किया गया होता तो अब तक सजा जुर्माना करके फुरसत मिल गयी होती।
बनवारी को लग रहा है कि पंच इस औरत का रोंवा भी नहीं उखाड़ पायेंगे। झुट्ठै तुर्रम खां बने फिरते हैं।
बड़ी देर तक चुप्पी छाई रहती है। फिर इंजन की सीटी सुनाई पड़ती है। एक गैस बत्ती के भुकभुकाने की आवाज आती है। मिठुआ उसे उतार कर उसमें हवा भरने लगता है।
-मेरे सवाल का जवाब आप सबके मन में है। आप देना नहीं चाहते। अब मैं दूसरा सवाल पेश करती हूं। मेरे इस सवाल के पेट से ही चैधरी बाबा के सवाल का जवाब निकलेगा। मेरा सवाल है कि फसल पर पहला हक किसका है? खेत का कि बीज का? अगर पंच फैसला करते हैं कि फसल पर खेत का हक है तो पंच मुझसे बच्चे के बाप का नाम पूछने के हकदार नहीं बनते। अगर फैसला बीज के हक में होता है तो मैं बच्चे के बाप को पेश कर दूंगी।
फसल पर पहला हक खेत का कि बीज का?
छोटे-छोटे समूह में तर्क वितर्क शुरू हो जाता है।
-यह कोई नया सवाल थोड़े है। बलई बाबा तिरस्कार से कहते हैं। -जितनी पुरानी दुनिया उतना पुराना सवाल। इस सवाल के जवाब से तो सारे वेद पुरान कलमा कुरान भरे पड़े हैं।
-हमे भी बता दीजिये बाबा। हम तो वेद पुराण पढ़े नहीं है।
-तो तेरे लिये वही गीत फिर फिर से गाना पड़ेगा? दसईपुर की बेड़िन समझ लिया कि बीबी फिर फिर से।
दसईपुर का किस्सा कौन नही जानता इस ईलाके में। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ जाती है।
-च्च! च्च! यह हम कैसे कह सकते है बाबा? आप बड़े हैं। अपने मुंह से बेड़िन बने चाहे पतुरिया।
-बाप रे! कितना तेज झपट्टा मारती है यह औरत। लछिमन चैधरी बलई बाबा के बचाव में आ जाते है। कहते है वेद पुरान तो हम भी नहीं पढ़े लेकिन जो ‘परतच्छ’ है उससे हटकर वेद पुरान में क्या होगा? मेरे विचार से तो बीज ही परधान है। खेत किसी का हो, जो बोया जायेगा वही पैदा होगा। आम के बीज से आम। बबूल के बीज से बबूल। बोया बीज बबूल का, आम कहां से होय?
-सवाल यह नहीं है कि क्या बोने से क्या पैदा होगा। इसे तो पीछे बैठ कर हंस रहा वह बग्गड़ भी जानता है। सुघरा बोलती हैं- सवाल यह है कि फसल पर हक किसका होगा? एक आदमी अपने खेत में गेहूं बो रहा है। उसके बीज के कुछ दाने बगल के जौ के खेत में छिटक कर चले गये। फसल तैयार होने पर साफ पता चल रहा है कि गेहूं के पौधे बगल वाले के बीज से पैदा हुए हैं। तो क्या गेहूं के खेत वाला जौ के खेत में उगे गेहूं के उन पौधों पर अपना हक जता सकता है?
बिल्कुल नहीं। कई आवाजें आती हैं- जिसके खेत में पैदा होता है वही काटता है।
-क्या आज तक एक भी मामला सुना गया कि छिटके बीज के मालिक ने बगल के खेत में घुस कर उन पौधों को काटा हो?
-कभी नहीं। इस नीयत से उस खेत में पैर भी रख देगा तो लाठी चल जायेगी।
-जैसे खेत से खुराक लेकर वह बीज पौधा बनता है, वैसे ही बूंद को आदमी बनाने के लिए मां को नौ महीने अपना खून पिलाना पड़ता हैं। बूंद सिर्फ बूंद होती है। आदमी का बच्च्चा नहीं होती।
-बिल्कुल सही।
- अब पंच तय करें कि बड़ी बात क्या है? बूंद डालना या उस बूंद को पोस कर आदमी बनाना।
धन्नू बाबा कहते हैं - ऐसे छिटके बीज से पैदा पौधों को ‘लमेर’ कहा जाता है। धान की फसल में तो ए अक्सर ही उगे मिलते हैं। ‘लमेर’ मूल फसल के पौधों से ज्यादा तंदुरूस्त, ज्यादा जीवट वाले होते हैं। वे मूल फसल से बित्ता भर ऊंचे होते हैं। उनकी बाल ज्यादा लम्बी और दाने ज्यादा पोढे़ पुष्ट होते हैं। उन पर रोग व्याधि का असर कम होता है। इसी तरह आदमियों की फसल पर नजर डालिए तो हर गांव में एक दो ऐसे लमेर मिल जायेंगे जिनके चेहरे-मोहरे, हँसने मुस्कुराने और बोली बानी के ढंग से आप जान जायेंगे कि यह किसके बीज का लमेर है। आदमी के लमेर भी अपने मूल से ज्यादा लम्बे चैड़े जीवट वाले और तेज होते है। ध्यान दीजिए तो अपने इसी गांव में दो लमेर पहचान में आ जायेंगे। लेकिन क्या किसी लमेर के बीज ने आज तक उन पर अपना दावा ठोंका? कभी कहीं सुना गया कि किसी लमेर का असली बाप उसे लेने आया हो। तो कुच्ची के बच्चे पर उसे बीज दान देने वाले का हक कैसे मानेंगे जो, हक की बात तो दरकिनार, अपना नाम तक जाहिर नहीं करना चाहता।
पंचायत में फिर खुसर पुसर होने लगी है। यह सही है कि लमेर की हकीकत से सारा गांव वाकिफ है। आज से नहीं जमाने से। लेकिन इस पर इस तरह पंचायत में खुलेआम कभी चर्चा हुई हो, किसी को याद नहीं पड़ता। आंख में गड़ने वाली ऐसी हकीकत हजारांे साल से अचर्चित चली आयी, यह भी अजूबा है।
लछिमन चैधरी की मां वर्मिन थीं। जब वर्मा (आज का म्यांमार) की लड़ाई छिड़ी तो लछिमन चैधरी मां की गोद में थे। उनके बाप उन लोगों को लेकर कभी किसी सवारी से तो कभी पैदल भागते हुये गांव लौटे। लछिमन चैधरी के बाप लम्बे-चैडे़ और कालों में भी काले थे। तारकोल के रंग के। लछिमन चैधरी को कद काठी बाप की और रंग रूप मां का मिला, इसलिये वे लम्बे, छरहरे और गोरे बल्कि पीले थे। चिकने गोल चेहरे वाले। बचपन में लोग उन्हें चिढ़ाते कि वे अपने बाप के नहीं, किसी बर्मी के बेटे हैं। सुनते-सुनते उनके मन मे शंका समा गई। अपने बाप के काले चेहरे की ओर देखने का उनका मन नहीं करता था। वे अपनी मां से पूछना चाहते थे कि क्या सचमुच उनका बाप कोई और था? लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी।
अच्छा ही है कि जिन दो अन्य लमेरों की ओर धन्नू बाबा ने इशारा किया वे पंचायत में मौजूद नहीं हैं। एक तो बुढ़ापे के चलते महीनों से चारपाई पर पड़े-पड़े अपने आखिरी दिन गिन रहें हैं। दूसरे जो नौजवान है, बहुत पहले बम्बई चले गये।
-और सुनिये, धन्नू बाबा कहते हैं- मेरा वश चले तो मैं ऐसे ‘लमेरों‘ से सारी दुनिया भर दूं। जितने भी अशक्त अपराधी, बौने, बोदे, लाइलाज बीमारियों के रोगी और दिमागी तौर पर कमजोर लोग हैं उनके बच्चा पैदा करने पर रोक लगा दी जाय और जितने विद्धान, बुद्धिमान, पहलवान हैं उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने के काम पर लगा दिया जाय तो देखिये कि पचास साल में कैसी धुरन्धर पीढ़ी तैयार हो जाती है। देश-दुनिया की नश्ल सुधर जाय और जात कुजात का झगड़ा खतम हो जाय।
वाह बाबा वाह! पीछे से कोई बुलंद आवाज में कहता है- ऐसा इंतजाम पचीस साल पहले करवा देते तो बलई बाबा की जिंदगी भी सुफल हो जाती।
हंसी का फव्वारा।
पंचायत ऐसी नाव है जिस पर बैठे हर व्यक्ति के हाथ में पतवार है। कौन किधर खे कर ले जाने लगे, कुछ कह नहीं सकते। बनवारी का धैर्य जवाब दे रहा है।
वह खड़ा होकर कहता है- देश दुनिया की नसल बाद में सुधारिएगा बाबा। आधी रात बीत रही है। मुद्दे पर आइये।
-मुद्दा तो साफ हो गया। ‘लमेर’ पर खेत वाले का हक बनता है।
-पेड़-पौधों की बात दूसरी है महाराज। लछिमन चैधरी कहते हैं- लेकिन कल को अगर वही लमेर बच्चा मां का गला दबाते हुए पूंछे कि मुझे लमेर क्यों पैदा किया? बोल मेरा बाप कौन है तो...?
- उसके पूछने में अभी अठारह-बीस साल की कसर है। धन्नू बाबा कहते है- उसके पूछने तक वक्त एैसे सवालों का जवाब देने लायक हो जायेगा।
-आप भी बाबा कुछ ज्यादा ही लम्बी हांक रहे हैं। वक्त भला ऐस सवालों का जवाब देने आता है?
-आता है चैधरी। जाने कितने सवालों का जवाब वक्त दे चुका है। अब कोई वैसे सवाल नहीं पूछता। और वक्त नहीं देगा तो बच्चे की मां देगी। हमारे आपके पेट में अभी से दर्द क्यो हो?
बनवारी के मन में धन्नू के लिए चिढ़ पैदा हो गई है। साफ लग रहा है कि वे कुच्ची के पक्ष में बह रहे हैं। ऐसे ही थोड़े भगवान ने निरबसिया किया है। निरबसिया महा निशील।
उससे बिना बोले नहीं रहा जाता- अंगूठा छाप हैं तो इतनी वकालत कर रहे हैं। चार अच्छर पढ़ लिये होते तब तो बादर में प्योंदा लगाते।
-चार आदमी के बीच में बोलने का सहूर सीखों बनवारी। मैं अंगूठा छाप नहीं, चहारम पास हूं। और अंगूठा छाप होना कोई गाली नहीं है। लछिमन चैधरी अंगूठा छाप है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे जाहिल हैं। जब तुम मां के पेट से निकले नहीं थे तो इस देश में इमरजेंसी लगी थी। तब बडे़-बड़े पढ़े लिखों के गले में पड़ा फंदा अंगूठा छाप लोगों ने ही काटा था। पढ़े लिखे लोग तो डर के मारे बिल में घुस गये थे।
एक तीर से दो शिकार तो सुना था, धन्नू बाबा ने तीन-तीन कर लिये। धरमराज सिर नीचे करके मुस्करा रहा है।
लछिमन चैधरी को अच्छा लगा।
बलई सोच में पड़ गये हैं। गांव वालो को यह तो पता था कि वह वोट देने पोलिंग सेंटर नहीं पहुंचे लेकिन यह तो सनातन की अम्मा भी नहीं जान पाईं कि घर से निकल कर वे अरहर के खेत में छिप गये थे। तब धन्नू बिल में घुसने की बात कैसे कह रहे है? इमरजेंसी के दौरान जबरिया नशबन्दी के लिए पकड़ लिए जाने का आतंक उनके मन पर इस कदर हावी हो गया था कि उसके खात्मे का ऐलान सुन लेने के बाद भी उनकी पोलिंग सेन्टर पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहीं कोई धोखा न हो जाय...
फिर उन्हें लगता कि वे बेकार संदेह कर रहे हैं। धनई आम शहराती पढे़-लिखों की बात कर रहे होंगे, सेठों की, अफसरों की, यूनिवर्सिटी के मास्टरों की, जो जरा सी धूप लगते ही कुम्हला जाते हैं। भाग कर एसी में घुस जाते हैं।
बलई का लटका मुंह देख कर बनवारी के तन बदन में आग लग जाती है।
लछिमन चैधरी बीड़ी सुलगाने में लगे हैं।
वह कहता है- मुद्दे को दायें-बाये लेकर मत भागिये बाबा। यह बच्चा मेरे खानदान की नाक काटने आ रहा है। मैं अपने खानदान में ऐसा बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा।
-वह तो पैदा हो चुका। मतलब, पेट में आ चुका।
-मैं दुनिया में नहीं आने दूंगा। बनवारी दोनों हाथ उठा कर दहाड़ता है।
धरमराज वकील खड़ा होकर टोकता है- ऐसा अनर्थ मत भाखिए भइया? पूरे गांव के सामने बच्चे को मारने की धमकी। ऐसा करने की सजा जानते हैं? धारा 212 में आजीवन कारावास। किसी दूसरे ने ऐसा कर दिया तो भी तुम्हीं पकडे़ जाओगे। पूरी जिंदगी चक्की पीसने में खप जायेगी।
-मेरे आगे का पैदा तू मुझे ही डराने चला है। मुफ्त में हीरो होंडा मिल गयी इसलिए?
-मुफ्त में नहीं भइया। तीस हजार नगद गिना है।... और डराने की नहीं समझदारी की बात कर रहा हूं। नाक कटा दिया, कान कटा दिया यह पुरानी बात हो गयी। अगर तुम समझते हो कि भाभी के बच्चा हो जाने के चलते उनका घर की बहू वाला हक मर जायेगा तो गलती पर हो। अगर किसी ने तुम्हे ऐसा पाठ पढ़ाया है तो समझो तुम्हें कुंए में ढकेल रहा है। अगर रमेसर काका अपने जीते जी खेत बेच नहीं देते तो काकी के बाद यह कुच्ची भौजी को ही मिलेगा। उनका हक तभी खत्म होगा जब वे दूसरी शादी कर लेंगी। उनके रहते तुम्हे सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं मिलने वाली।
-इसको सब पता है। तभी तो उसे भगाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। धन्नू बाबा कहते हैं- लेकिन आप लोग बताइये, खानदान या गांव की नाक गर्भ के बच्चे को मारने से कटती है, अकेली औरत के घर में बुरी नीयत से घुसने पर कटती है कि अपनी मर्जी से अपना सहारा पैदा करने से? बनवारी ने जो धमकी दी है उसके खतरे से बचने का रास्ता पंचो को निकालना होगा।
-बिलकुल निकालना होगा। सुघरा कहतीं है।.... यह धमकी नयी नहीं है। औरत को यह धमकी सदियों से मिलती आ रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने ही औरत के साथ अन्याय कर दिया। उसकी छाती फुला दी और हौंसला घटा दिया। जिस दिन से लड़की की छाती फूलने लगती है उसका हौसला घटने लगता है। वह फूली हुई छाती पर गुमान करती है और उसी के चलते मारी जाती है। पैदा तो पहले भी होते रहे हैं ऐसे बच्चे लेकिन मां के डर जाने, हौसला छोड़ देने के चलते मारे जाते रहे, फेंके जाते रहे, गिराये जाते रहे।
-ऐ आजी। कुच्ची खड़ी होती है- कुंती माई डर गयीं, अंजनी माई डर गयीं, सीता की माई डर गयीं लेकिन बालकिसन की माई डरने वाली नहीं है। मेरा बाल किसन पैदा होकर रहेगा।
कुच्ची का ऐलान पूरी पंचायत के कान में झन्न से बजता है। पलभर सन्नाटा। फिर बाजार से आयी महिलाओं के झुंड से ताली बजने की जो शुरुआत होती है वह पूरी पंचायत में फैल जाती है। तीनों महिला वकील भी खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाती। ठीक उसी समय सौ वाट के बल्ब की रोशनी में पूरी पंचायत नहा जाती है। बलई बाबा की कनपटी से पसीना चू पड़ता है।
कुछ देर तक सन्नाटा रहता है फिर सुधरा कहती हैं- पंचों, कई साल तक थाना कचेहरी दौड़ने और परधानी करने के बाद यही समझ में आया कि सारे झगड़े की जड़ पापर्टी है। आदमी की नजर में औरत खुद प्रापर्टी है। बनवारी और हनुमान राम लछिमन की तरह रहते थे लेकिन जैसे ही हनुमान मरा, बनवारी उसकी बेवा की मदद करने के बजाय उसे अपनी प्रापर्टी बनाने की तिकड़म में लग गया। इसकी बने या गांव से भागे तो वह रमेसर की प्रापर्टी हड़पे। बनवारी सिर्फ इसी गांव में थोड़े है। हर गांव में बनवारी हैं। मेरा भतीजा भी तो बनवारी है। आदमी की तो छोड़िये, प्रापर्टी के मामले में हमारी सरकारें तक बनवारियों से कम नहीं हैं। उन्होंने भी मर्दों की तरफदारी वाले कानून बना कर रख छोड़े हैं। मान लीजिए अभी लछिमन चैधरी को दारू की लत लग जाय। दारू के लिए वे अपने खेत बेचने पर आमादा हो जायें। चैधराइन को पता चले। वे बाल बच्चों के साथ हाकिम की इजलास पर जाकर गुहार लगायें कि हजूर मेरे आदमी को खेत बेचने से रोका जाय नहीं तो मैं बाल बच्चों के साथ भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊंगी। पूरी नहीं तो आधी जमीन पर ही स्टे दे दिया जाय। क्या इजलास स्टे दे देगी? हरगिज नहीं। वह हाथ खडे़ कर देगी। क्यांे भाई? उसके पास तो अथाह पावर है। अथाह पावर तो है लेकिन लछिमन चैधरी को अपनी जमीन बेचने से रोकने की पावर नहीं है। जो जमीदारी विनाश कानून हमारे यहां सन् 52 में लागू हुआ वह सिर्फ मर्द को पहचानता है। खेत का सारा मालिकाना वह मर्द को देता है। औरत सरकार की नजर में गोबर का छोत है। किसान की जमीन हड़पने का कानून तो सरकारें मिन्टों में पास कर देती है। बाई रोटेशन पास कर देती हैं लेकिन औरत मर्द के बीच मालिकाना हक बांटने का कानून पास करने की फुरसत आज तक किसी सरकार को नहीं मिली। ऐसा हो जाता तो ‘बनवारियों’ की पैदाइस बन्द हो जाती।
बैठे-बैठे मोबाइल में फोटो खींचने के अलावा बहस में शामिल होने का कोई मौका न पाने वाली महिला मोर्चा की सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया है। मनोरमा जी तुरंत कुर्सी से उठते हुए कहती हैं- भाइयों और बहनों। हमारा संगठन इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहा है। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाने वाले हैं कि महिलाओं को पति की खेती बारी में विवाह के दिन से ही आधा मालिकाना हक दिया जाय।
-और कोख वाला मुद्दा दीदी? कुच्ची पूछती है।
मनोरमा जी ऐसे सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हैं। वे पलभर ठिठकती हैं फिर कहती हैं- देखिए, सही बात तो यह है कि यह मुद्दा अभी हमारे संगठन के सामने उठा ही नहीं है। फिर थोड़ा रूककर, अपनी दूसरी सदस्यों की ओर देखते हुए कहती हैं- दरअसल यह बहुत आगे का मुद्दा है लेकिन गांव में रहकर जब तुम्हारी जैसी औरत इसकी जरूरत महसूस कर रही है, इस मुद्दे को उठा रही है तो देर सवेर इसे वक्त की आवाज बनना ही होगा।
-बड़ा मुद्दा तो कोख पर अधिकार का मुद्दा ही है। बाजार से आयी महिलाओं के बीच से एक लड़की खड़ी होती है - औरत का हक़ हिस्सा मारने वाले ऋषि मुनि क कबके मर मरा गये लेकिन उनका बनाया फंदा अभी भी औरतों के गले में फँसा हुआ है। वक्त आ गया है कि मरे हुओं का कानून मरे हुओं के साथ दफन कर दिया जाय। ऐसा कानून बने जिससे हम भी जिंदा लोगों की तरह जिंदा रह सकें। हम सब अपनी इस बहादुर बहन के साथ हैं।
पता चलता है कि यह लड़की अभी अभी एडीओ पंचायत बन कर ब्लाक पर आयी है।
इन औरतों का रूख देखकर लछिमन चैधरी और बलई बाबा को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है। कहीं सब हंगामा न शुरु कर दें। उनको लगता है कि पंचायत पूरी तरह मुद्दे से भटक गयी है।
आखिरी कोशिश के तौर पर लछिमन चैधरी फिर पैतरा बदलते हैं- आप लोग तो कहां की बात लेकर कहां उड़ गई। असली मुद्दे पर रहिये। यहां रमेशर दोनों परानी भी मौजूद हैं। कुच्ची को आखिर रहना तो उन्हीं के घर में है। उनकी मरजी क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। क्या उन्हे ऐसी दागी औरत अपने घर में रखना कबूल है?
जरूर-जरूर। बलई बाबा फौरन बोलते हैं- कहां हैं रमेशर? बैठे-बैठे सो गये क्या?
रमेशर भगत जब से बैठे हैं पेशाब करने के लिए भी नहीं उठे। पैरों में चिंगुरा पकड़ लिया है। वे जमीन पर हाथ की टेक लेकर खडे़ होते हैं।
-अपने मन की बात बेधड़क बोलिए भगत। किसी से दबने डरने की जरूरत नहीं है। बलई उन्हें झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं।
-हमारे बोलने के दिन तो हनुमान के साथ ही उड़ गये पंचों। सुनने के दिन हैं सो सुन रहे हैं।
-फिर भी अपनी इच्छा बताओ? बहू की मनमानी से दुःख संताप तो होता ही होगा?
-दुःख संताप मुझे नहीं, बनवारी को है महराज। इसी के चलते तो ढाई साल से उसके पेट का पानी नहीं पच रहा है। उसी के बुलावे से, उसी की सुनने तो आप लोग आये हैं।
-तुम्हारी भी सुनी जायेगी। लछिमन चैधरी कहते हैं।
-बहुत अच्छा लग रहा है जब इतने दिन बाद पंच हमारा दुःख संताप पूछ रहे हैं।
-तुम्हारी पतोहू ने ऐसा कांड ही कर दिया कि पूछना लाजमी है। उसने जो कुछ कहा, तुमने सुना कि नहीं?
-काहें नहीं सुना महराज। बहू ने जो कुछ कहा वह तो दोनों कानों के बहिर को भी सुनायी पड़ गया होगा। आज पहली बार समझा कि हमारी बहू इतना जानती है, इतना सोचती है, इतना बोलती है। हम तो उसे गूंगी गाय समझते थे।
फिर चुप्पी।
-अच्छा रमेसर बहू तुम बोलो। लछिमन चैधरी चोट करते हैं - क्या तुम लमेर बच्चे के साथ बहू को अपने घर में रखने को तैयार हो?
-चैधरी, कौन मानुष दावे के साथ कह सकता है कि वह लमेर नहीं है। आप कह सकते हैं?
बूढ़ी एक पल रूकती है और इसी एक पल में लछिमन चैधरी को पसीना छूट जाता है। आगे क्या कहने वाली है बूढ़ी?
- यह बात तो केवल माँ जानती है। फरक इतना है कि दूसरे लमेरों के मुँह पर उनके बाप का ढक्कन रहता है, इस बच्चे के मुँह पर ढक्कन नहीं है। रही बात घर में रखने की, तो जिस बहू ने हमारे लिए अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दिया, हमें उसके रास्ते का काँटा हटाना चाहिए कि उस पर और काँटा बिछाना चाहिए? यह मेरी बहू भी है, बेटी भी है। इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है।
लछिमन चैधरी के मुँह पर ताला लग जाता है।
-बस हो गया। धन्नू बाबा खड़े होते हुए दोनो हाथ उठा कर कहते हैं- बुढ़ापे में सहारे की कितनी जरुरत पड़ती है, इसे बलराज भइया या मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? इसलिए अगर कुच्ची अपने लिए सहारा पैदा कर रही है और रमेसर दोनो परानी राजी हैं तो किसी तीसरे को बीच में कूदने का कोई हक नहीं बनता।
वे बलई और लछिमन चैधरी की ओर देखते हैं फिर कहते हैं- ठकुराइन ने औरतों की हकतलफी वाले जिस कानून की ओर इशारा किया है वह भी बहुत जरूरी मुद्दा है। अगर ब्याह कर आते ही कुच्ची को खेती बारी में कानूनी हक हिस्सा मिल जाता तो आज उसके बच्चे के लिए चिन्ता करने की जरुरत ही न रहती। लेकिन उसका भी रास्ता है। उसे वरासत से नहीं मिलेगा तो रमेसर भगत के अँगूठा निशान से मिल जायेगा। असली चिंता तो उसकी जिंदगी की है। हमें उसकी जिंदगी की गारंटी चाहिए। अगर बनवारी उसकी जिंदगी के लिए खतरा बनता है तो इस जुर्म का भागी पूरा गाॅव होगा। इसलिए जरूरी है कि किसी को बाजार भेज कर गोपाल वेंडर के घर से दस रुपये का स्टाम्प पेपर मँगवाया जाय। इस पर इस धमकी का हवाला देते हुए लिखा जाय कि जच्चा बच्चा को कोई खतरा होता है तो इसका जिम्मेदार बनवारी होगा। सारे पंच उस पर दस्तखत करें। वह कागज सुघरा ठकुराइन के पास रखा जाय उसकी फोटोकापी गाॅव भर में बांटी जाये। कभी कोर्ट कचेहरी में जरुरत पड़े तो सारा गाॅव गवाही देने चले।
बनवारी के कान खड़े हो जाते हैं। यह तो उल्टे उसी को फँसाने का फंदा तैयार किया जा रहा है। बलई और और लछिमन चैधरी की बोलती बंद? ‘सलेन्डर’ कर दिए? उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वह खड़ा होकर मुट्ठी बँधा दाहिना हाथ कुहनी से मोड़ कर सामने ऊपर नीचे हिलाते हुए चिल्लाता है-मेरे फलान-चीन्ह पर जायँ ऐसे पंच और ऐसी पंचायत।
और बाहर जाने के लिए भीड़ में राह बनाने लगता है।
पंचों को ठकरा मार जाता है।
तभी धन्नू बाबा की दहाड़ सुनायी पड़ती है-खबरदार जो आगे बढ़ा। तेरी यह मजाल कि पूरे गाँव को फलान-चीन्ह पर मार कर निकल जायेगा? जाता है तो इसकी सजा सुन कर जा। अगर तू पंच की मरजी के बगैर यहां से भागा तो कल यही गांव तेरे लिए काला पानी हो जायेगा। न गांव का कोई आदमी तेरे दरवाजे जायेगा न कोई तुझे अपने दरवाजे पर खड़ा होने देगा। न कोई तुझसे बोलेगा न तेरी हारी गोहारी दौडे़गा। तेरे साथ राह-रीत हराम है। उठन-बैठन हराम है। खान-पान हराम है। दुआ-सलाम हराम है।... अगर किसी को इस फैसले पर एतराज है तो अभी बता दे।
-बहुत सही। हम इसका समर्थन करते हैं। सुघरा कहती हैं।
बलई बाबा बनवारी को डांटते हैं- तूने भांग तो नहीं खा ली। पूरी पंचायत को फलान-चीन्ह पर मार दिया।
मिठुआ बाल्टी लोटा, खाली डलिया और दोनों बुझी गैस बत्तियां लेकर बाप के बगल में आकर खड़ा हो गया है। सुलछनी घास में सोये अपने दोनों बेटों को झकझोर कर जगाने लगी है।
लछिमन चैधरी डाॅटते हैं- तीन बच्चों के बाप हो गये और पंचायत में बोलने का सहूर नहीं आया? मांफी मांगो।
-बिना शर्त मांफी। जैसे हाईकोर्ट में मांगी जाती है। सुघरा कहती हैं।
लेकिन बनवारी मांफी मांगने को तैयार नहीं दिखता। वह प्रश्न चिन्ह की तरह तन कर खड़ा है।
तभी मिठुआ तौलिया लपेट कर जलता हुआ बल्ब होल्डर से निकाल लेता है।
घुप्प अंधियारे के बाद दसमी के चांद के धीरे-धीरे फरियाते उजाले में यह समझ पाना कठिन है कि बनवारी सिर्फ हाथ उठा रहा है या हाथ जोड़ भी रहा है।
हल्की बहती, पुरवा अचानक तेज हो गयी है। सूखे पत्ते उड़ने लगे हैं। आंधी-पानी आयेगा क्या?
जागो रे जागो। भागो रे भागो...।
-लेकिन कल स्टाम्प पेपर जरूर मंगवा लेना पंडित। खटोले से उठते हुये सुघरा कहती हैं।
-:0:-